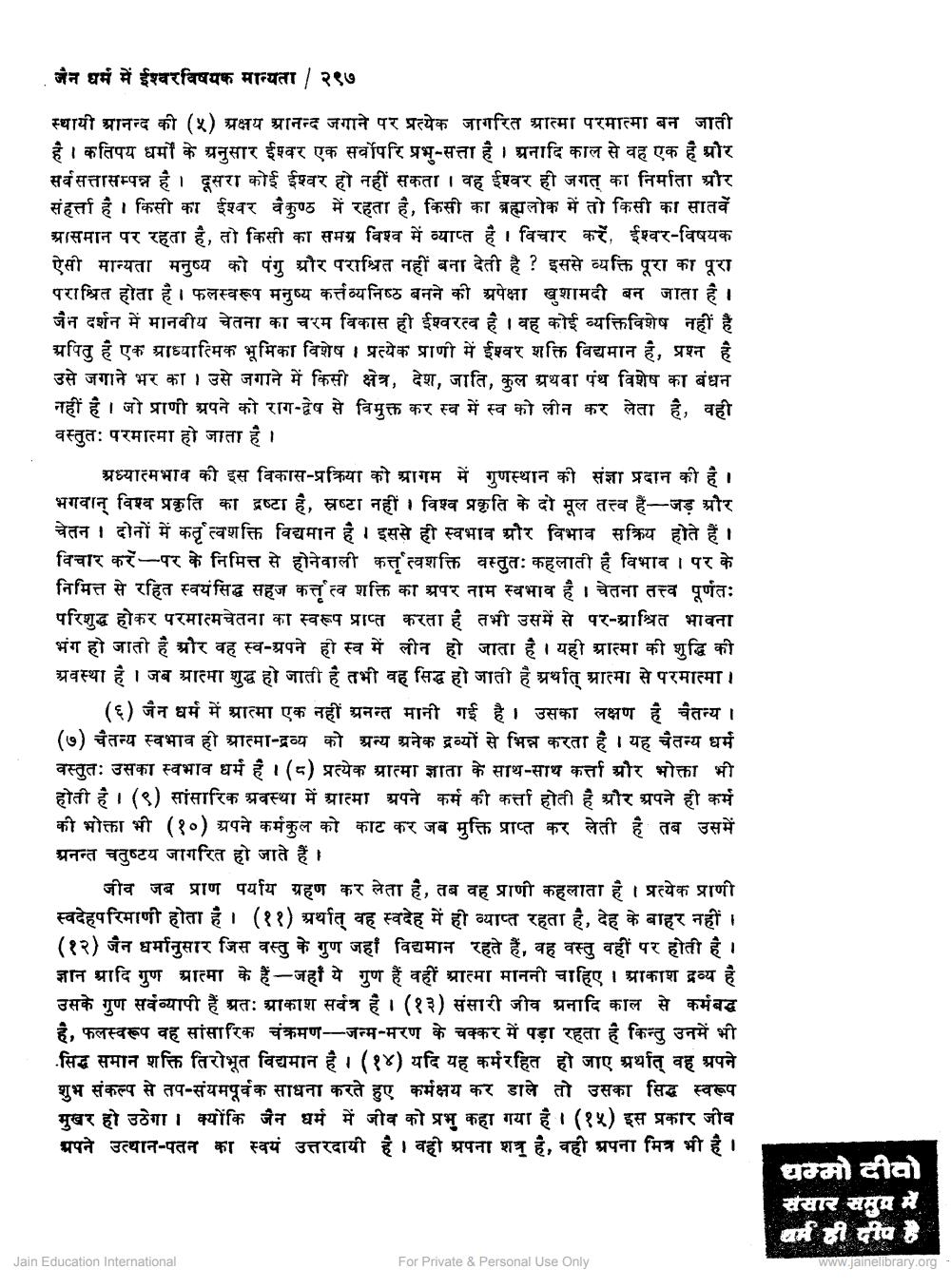________________
जैन धर्म में ईश्वरविषयक मान्यता / २९७
1
स्थायी आनन्द की (५) अक्षय आनन्द जगाने पर प्रत्येक जागरित ग्रात्मा परमात्मा बन जाती है । कतिपय धर्मों के अनुसार ईश्वर एक सर्वोपरि प्रभुसत्ता है। अनादि काल से वह एक है घोर सर्वसत्तासम्पन्न है । दूसरा कोई ईश्वर हो नहीं सकता । वह ईश्वर ही जगत् का निर्माता और संहर्त्ता है । किसी का ईश्वर वैकुण्ठ में रहता है, किसी का ब्रह्मलोक में तो किसी का सातवें प्रासमान पर रहता है, तो किसी का समग्र विश्व में व्याप्त है। विचार करें ईश्वर-विषयक ऐसी मान्यता मनुष्य को पंगु धौर पराधित नहीं बना देती है ? इससे व्यक्ति पूरा का पूरा पराश्रित होता है । फलस्वरूप मनुष्य कर्त्तव्यनिष्ठ बनने की अपेक्षा खुशामदी बन जाता है । जैन दर्शन में मानवीय चेतना का चरम विकास ही ईश्वरत्व है । वह कोई व्यक्तिविशेष नहीं हैं अपितु है एक प्राध्यात्मिक भूमिका विशेष । प्रत्येक प्राणी में ईश्वर शक्ति विद्यमान है, प्रश्न है उसे जगाने भर का उसे जगाने में किसी क्षेत्र, देश, जाति, कुल अथवा पंथ विशेष का बंधन नहीं है। जो प्राणी अपने को राग-द्वेष से विमुक्त कर स्व में स्व को लीन कर लेता है, वही वस्तुतः परमात्मा हो जाता है ।
संज्ञा प्रदान की है ।
।
अध्यात्मभाव की इस विकास प्रक्रिया को श्रागम में गुणस्थान की भगवान् विश्व प्रकृति का द्रष्टा है, स्रष्टा नहीं । विश्व प्रकृति के दो मूल तत्त्व हैं-जड़ और चेतन दोनों में कर्तृत्वशक्ति विद्यमान है। इससे ही स्वभाव और विभाव सक्रिय होते हैं। । विचार करें पर के निमित्त से होनेवाली कसू स्वशक्ति वस्तुतः कहलाती है विभाव पर के निमित्त से रहित स्वयंसिद्ध सहज कर्तृत्व शक्ति का अपर नाम स्वभाव है। चेतना तत्व पूर्णतः परिशुद्ध होकर परमात्मचेतना का स्वरूप प्राप्त करता है तभी उसमें से पर प्राश्रित भावना भंग हो जाती है और वह स्व-अपने ही स्व में लीन हो जाता है । यही श्रात्मा की शुद्धि की अवस्था है । जब ग्रात्मा शुद्ध हो जाती हैं तभी वह सिद्ध हो जाती है अर्थात् आत्मा से परमात्मा ।
(६) जैन धर्म में आत्मा एक नहीं अनन्त मानी गई है। उसका लक्षण है चैतन्य । (७) चैतन्य स्वभाव ही आत्मा द्रव्य को अन्य अनेक द्रव्यों से भिन्न करता है। यह चैतन्य धर्म वस्तुतः उसका स्वभाव धर्म है । (८) प्रत्येक प्रात्मा ज्ञाता के साथ-साथ कर्ता और भोक्ता भी होती है । ( ९ ) सांसारिक अवस्था में ग्रात्मा अपने कर्म की कर्त्ता होती है और अपने ही कर्म की भोक्ता भी (१०) अपने कर्मकुल को काट कर जब मुक्ति प्राप्त कर लेती है तब उसमें अनन्त चतुष्टय जागरित हो जाते हैं ।
जीव जब प्राण पर्याय ग्रहण कर लेता है, तब वह प्राणी कहलाता है । प्रत्येक प्राणी स्वदेहपरिमाणी होता है। (११) अर्थात् वह स्वदेह में ही व्याप्त रहता है, देह के बाहर नहीं । (१२) जैन धर्मानुसार जिस वस्तु के गुण जहाँ विद्यमान रहते हैं, यह वस्तु वहीं पर होती है। ज्ञान श्रादि गुण प्रात्मा के हैं - जहाँ ये गुण हैं वहीं श्रात्मा माननी चाहिए । आकाश द्रव्य है उसके गुण सर्वव्यापी हैं अतः भ्राकाश सर्वत्र है। (१३) संसारी जीव अनादि काल से कर्मबद्ध है, फलस्वरूप वह सांसारिक चंक्रमण – जन्म-मरण के चक्कर में पड़ा रहता है किन्तु उनमें भी
हो जाए अर्थात् वह अपने
सिद्ध समान शक्ति तिरोभूत विद्यमान है। (१४) यदि यह कर्मरहित शुभ संकल्प से तप-संयमपूर्वक साधना करते हुए कर्मक्षय कर डाले तो उसका सिद्ध स्वरूप मुखर हो उठेगा। क्योंकि जैन धर्म में जीव को प्रभु कहा गया है । (१५) इस प्रकार जीव अपने उत्थान-पतन का स्वयं उत्तरदायी है। वही अपना शत्रु है, वही अपना मित्र भी है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
धम्मो दीवो
संसार समुद्र में
धर्म ही दीप है
www.jainelibrary.org