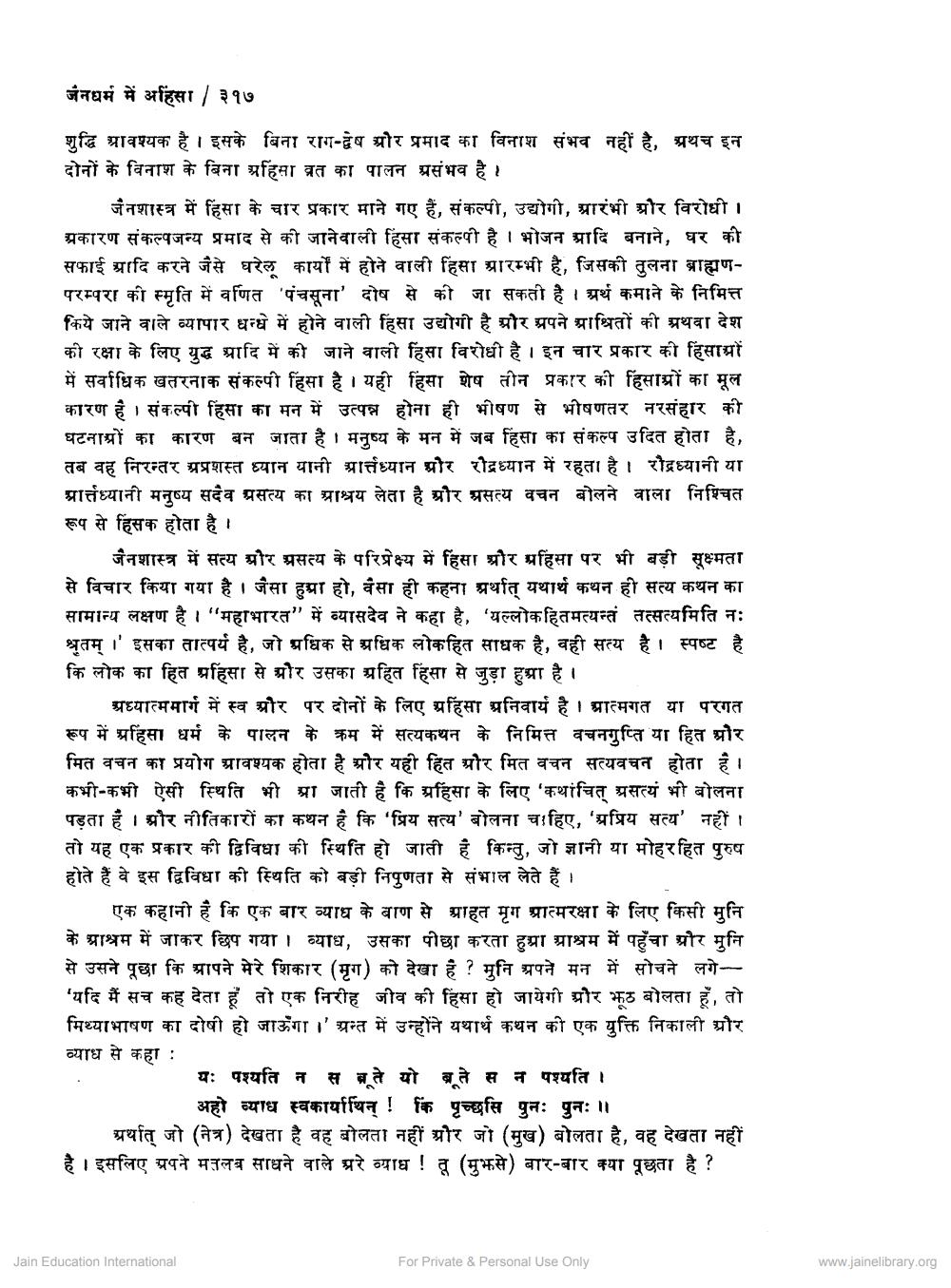________________
जैनधर्म में अहिंसा/३१७
शुद्धि आवश्यक है। इसके बिना राग-द्वेष और प्रमाद का विनाश संभव नहीं है, अथच इन दोनों के विनाश के बिना अहिंसा व्रत का पालन असंभव है।
जैनशास्त्र में हिंसा के चार प्रकार माने गए हैं, संकल्पी, उद्योगी, प्रारंभी और विरोधी। अकारण संकल्पजन्य प्रमाद से की जानेवाली हिंसा संकल्पी है । भोजन आदि बनाने, घर की सफाई आदि करने जैसे घरेल कार्यों में होने वाली हिंसा प्रारम्भी है, जिसकी तुलना ब्राह्मणपरम्परा की स्मृति में वर्णित 'पंचसूना' दोष से की जा सकती है। अर्थ कमाने के निमित्त किये जाने वाले व्यापार धन्धे में होने वाली हिंसा उद्योगी है और अपने आश्रितों की अथवा देश की रक्षा के लिए युद्ध आदि में की जाने वाली हिंसा विरोधी है । इन चार प्रकार की हिंसानों में सर्वाधिक खतरनाक संकल्पी हिंसा है। यही हिंसा शेष तीन प्रकार की हिंसानों का मूल कारण है । संकल्पी हिंसा का मन में उत्पन्न होना ही भीषण से भीषणतर नरसंहार की घटनामों का कारण बन जाता है। मनुष्य के मन में जब हिंसा का संकल्प उदित होता है, तब वह निरन्तर अप्रशस्त ध्यान यानी प्रार्तध्यान और रौद्रध्यान में रहता है। रौद्रध्यानी या प्रार्तध्यानी मनुष्य सदैव असत्य का प्राश्रय लेता है और असत्य वचन बोलने वाला निश्चित रूप से हिंसक होता है।
जैनशास्त्र में सत्य और असत्य के परिप्रेक्ष्य में हिंसा और अहिंसा पर भी बड़ी सूक्ष्मता से विचार किया गया है । जैसा हुअा हो, वैसा ही कहना अर्थात् यथार्थ कथन ही सत्य कथन का सामान्य लक्षण है। "महाभारत" में व्यासदेव ने कहा है, 'यल्लोकहितमत्यन्तं तत्सत्यमिति नः श्रुतम् ।' इसका तात्पर्य है, जो अधिक से अधिक लोकहित साधक है, वही सत्य है। स्पष्ट है कि लोक का हित अहिंसा से और उसका अहित हिंसा से जुड़ा हुआ है।
अध्यात्ममार्ग में स्व और पर दोनों के लिए अहिंसा अनिवार्य है । आत्मगत या परगत रूप में अहिंसा धर्म के पालन के क्रम में सत्यकथन के निमित्त वचनगुप्ति या हित और मित वचन का प्रयोग आवश्यक होता है और यही हित और मित वचन सत्यवचन होता है। कभी-कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि अहिंसा के लिए 'कथांचित् असत्यं भी बोलना पड़ता है । और नीतिकारों का कथन है कि 'प्रिय सत्य' बोलना चाहिए, 'अप्रिय सत्य' नहीं । तो यह एक प्रकार की द्विविधा की स्थिति हो जाती है किन्तु, जो ज्ञानी या मोहरहित पुरुष होते हैं वे इस द्विविधा की स्थिति को बड़ी निपुणता से संभाल लेते हैं।
एक कहानी है कि एक बार व्याध के बाण से पाहत मृग प्रात्मरक्षा के लिए किसी मुनि के आश्रम में जाकर छिप गया। व्याध, उसका पीछा करता हुअा अाश्रम में पहुँचा और मुनि से उसने पूछा कि आपने मेरे शिकार (मृग) को देखा है ? मुनि अपने मन में सोचने लगे'यदि मैं सच कह देता हूँ तो एक निरीह जीव की हिंसा हो जायेगी और झूठ बोलता हूँ, तो मिथ्याभाषण का दोषी हो जाऊंगा।' अन्त में उन्होंने यथार्थ कथन की एक युक्ति निकाली और व्याध से कहा :
यः पश्यति न स ब्रूते यो ब्रूते स न पश्यति ।
अहो व्याध स्वकार्याथिन् ! किं पृच्छसि पुनः पुनः ॥ अर्थात् जो (नेत्र) देखता है वह बोलता नहीं और जो (मुख) बोलता है, वह देखता नहीं है । इसलिए अपने मतलब साधने वाले अरे व्याध ! तू (मुझसे) बार-बार क्या पूछता है ?
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org