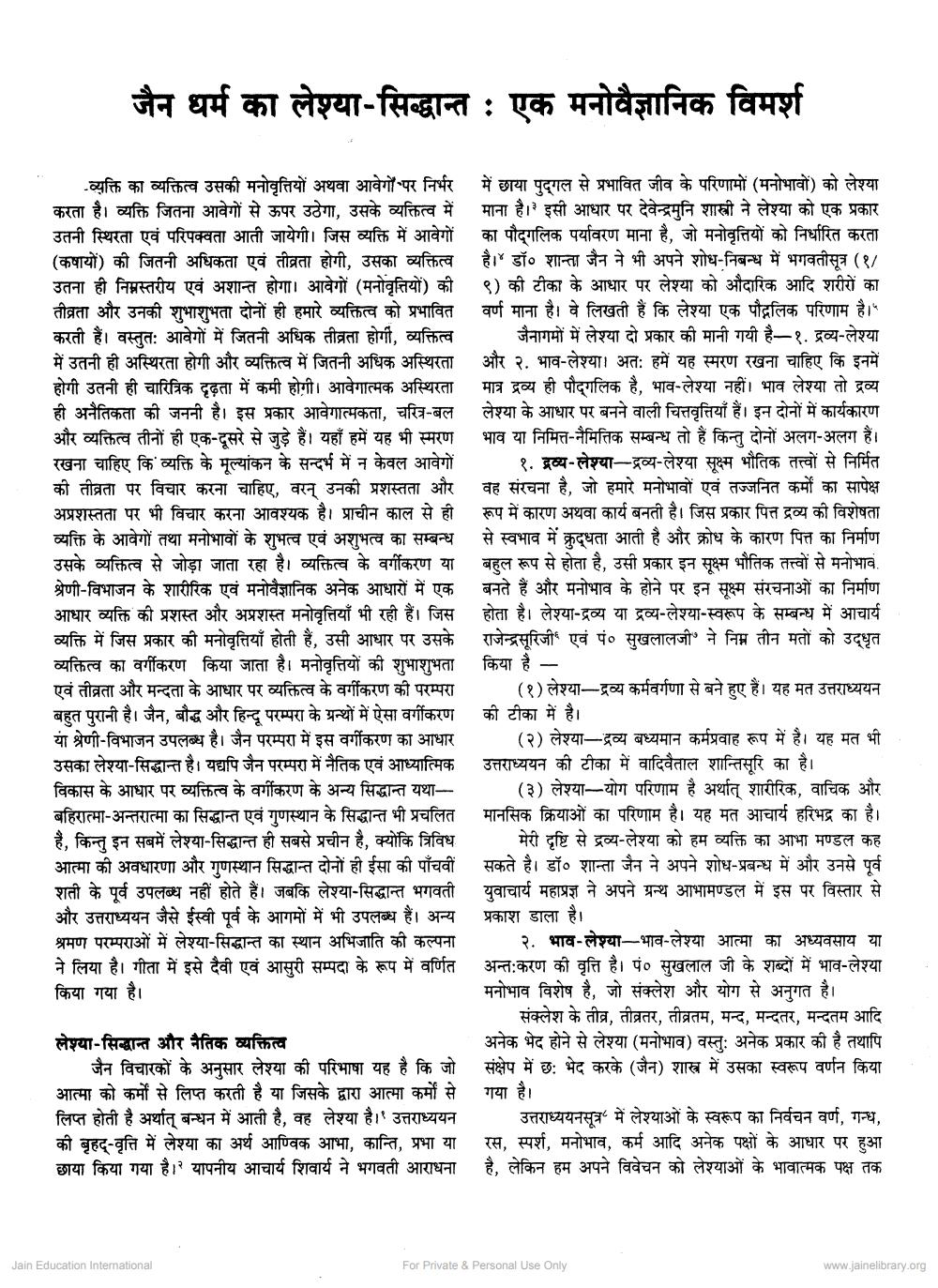________________
जैन धर्म का लेश्या - सिद्धान्त : एक मनोवैज्ञानिक विमर्श
व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी मनोवृत्तियों अथवा आवेगों पर निर्भर करता है। व्यक्ति जितना आवेगों से ऊपर उठेगा, उसके व्यक्तित्व में उतनी स्थिरता एवं परिपक्वता आती जायेगी। जिस व्यक्ति में आवेगों (कषायों) की जितनी अधिकता एवं तीव्रता होगी, उसका व्यक्तित्व उतना ही निम्नस्तरीय एवं अशान्त होगा। आवेगों (मनोवृत्तियों) की तीव्रता और उनकी शुभाशुभता दोनों ही हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। वस्तुतः आवेगों में जितनी अधिक तीव्रता होगी, व्यक्तित्व में उतनी ही अस्थिरता होगी और व्यक्तित्व में जितनी अधिक अस्थिरता होगी उतनी ही चारित्रिक दृढ़ता में कमी होगी। आवेगात्मक अस्थिरता ही अनैतिकता की जननी है। इस प्रकार आवेगात्मकता, चरित्र बल और व्यक्तित्व तीनों ही एक-दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि व्यक्ति के मूल्यांकन के सन्दर्भ में न केवल आवेगों की तीव्रता पर विचार करना चाहिए, वरन् उनकी प्रशस्तता और अप्रशस्तता पर भी विचार करना आवश्यक है। प्राचीन काल से ही व्यक्ति के आवेगों तथा मनोभावों के शुभत्व एवं अशुभत्व का सम्बन्ध उसके व्यक्तित्व से जोड़ा जाता रहा है। व्यक्तित्व के वर्गीकरण या श्रेणी विभाजन के शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक अनेक आधारों में एक आधार व्यक्ति की प्रशस्त और अप्रशस्त मनोवृत्तियाँ भी रही हैं। जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की मनोवृत्तियाँ होती हैं, उसी आधार पर उसके व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है। मनोवृत्तियों की शुभाशुभता एवं तीव्रता और मन्दता के आधार पर व्यक्तित्व के वर्गीकरण की परम्परा बहुत पुरानी है जैन, बौद्ध और हिन्दू परम्परा के ग्रन्थों में ऐसा वर्गीकरण या श्रेणी विभाजन उपलब्ध है। जैन परम्परा में इस वर्गीकरण का आधार उसका लेश्या सिद्धान्त है। यद्यपि जैन परम्परा में नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के आधार पर व्यक्तित्व के वर्गीकरण के अन्य सिद्धान्त यथाबहिरात्मा अन्तरात्मा का सिद्धान्त एवं गुणस्थान के सिद्धान्त भी प्रचलित है, किन्तु इन सबमें लेश्या सिद्धान्त ही सबसे प्रचीन है, क्योंकि त्रिविध आत्मा की अवधारणा और गुणस्थान सिद्धान्त दोनों ही ईसा की पाँचवीं शती के पूर्व उपलब्ध नहीं होते हैं। जबकि लेश्या - सिद्धान्त भगवती और उत्तराध्ययन जैसे ईस्वी पूर्व के आगमों में भी उपलब्ध हैं। अन्य श्रमण परम्पराओं में लेश्या सिद्धान्त का स्थान अभिजाति की कल्पना ने लिया है। गीता में इसे देवी एवं आसुरी सम्पदा के रूप में वर्णित किया गया है।
लेश्या सिद्धान्त और नैतिक व्यक्तित्व
जैन विचारकों के अनुसार लेश्या की परिभाषा यह है कि जो आत्मा को कर्मों से लिप्त करती है या जिसके द्वारा आत्मा कर्मों से लिप्त होती है अर्थात् बन्धन में आती है, वह लेश्या है। उत्तराध्ययन की बृहद् वृत्ति में लेश्या का अर्थ आण्विक आभा, कान्ति, प्रभा या छाया किया गया है' यापनीय आचार्य शिवार्य ने भगवती आराधना
Jain Education International
में छाया पुद्गल से प्रभावित जीव के परिणामों (मनोभावों) को लेश्या माना है। इसी आधार पर देवेन्द्रमुनि शास्त्री ने लेश्या को एक प्रकार का पौद्गलिक पर्यावरण माना है, जो मनोवृत्तियों को निर्धारित करता है । " डॉ० शान्ता जैन ने भी अपने शोध निबन्ध में भगवतीसूत्र (१/ ९) की टीका के आधार पर लेश्या को औदारिक आदि शरीरों का वर्ण माना है। वे लिखती हैं कि लेश्या एक पौगलिक परिणाम है।
जैनागमों में लेश्या दो प्रकार की मानी गयी है- १. द्रव्य लेश्या और २. भाव-लेश्या । अतः हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि इनमें मात्र द्रव्य ही पौद्गलिक है, भाव-लेश्या नहीं भाव लेश्या तो द्रव्य लेश्या के आधार पर बनने वाली चित्तवृत्तियाँ हैं। इन दोनों में कार्यकारण भाव या निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध तो हैं किन्तु दोनों अलग-अलग हैं।
१. द्रव्य लेश्या द्रव्य लेश्या सूक्ष्म भौतिक तत्वों से निर्मित वह संरचना है, जो हमारे मनोभावों एवं तज्जनित कर्मों का सापेक्ष रूप में कारण अथवा कार्य बनती है। जिस प्रकार पित्त द्रव्य की विशेषता से स्वभाव में क्रुद्धता आती है और क्रोध के कारण पित्त का निर्माण बहुल रूप से होता है, उसी प्रकार इन सूक्ष्म भौतिक तत्त्वों से मनोभाव बनते हैं और मनोभाव के होने पर इन सूक्ष्म संरचनाओं का निर्माण होता है। लेश्या द्रव्य या द्रव्य लेश्या स्वरूप के सम्बन्ध में आचार्य राजेन्द्रसूरिजी एवं पं० सुखलालजी ने निम्न तीन मतों को उद्धृत किया है
(१) लेश्या - द्रव्य कर्मवर्गणा से बने हुए हैं। यह मत उत्तराध्ययन की टीका में है।
(२) लेश्या - द्रव्य बध्यमान कर्मप्रवाह रूप में है । यह मत भी उत्तराध्ययन की टीका में वादिवैताल शान्तिसूरि का है।
(३) लेश्या - योग परिणाम है अर्थात् शारीरिक, वाचिक और मानसिक क्रियाओं का परिणाम है। यह मत आचार्य हरिभद्र का है।
मेरी दृष्टि से द्रव्य - लेश्या को हम व्यक्ति का आभा मण्डल कह सकते है । डॉ० शान्ता जैन ने अपने शोध-प्रबन्ध में और उनसे पूर्व युवाचार्य महाप्रज्ञ ने अपने ग्रन्थ आभामण्डल में इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है।
२. भाव - लेश्या – भाव-लेश्या आत्मा का अध्यवसाय या अन्तःकरण की वृत्ति है। पं० सुखलाल जी के शब्दों में भाव - लेश्या मनोभाव विशेष है, जो संक्लेश और योग से अनुगत है।
संक्लेश के तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मन्द, मन्दतर, मन्दतम आदि अनेक भेद होने से लेश्या (मनोभाव) वस्तु अनेक प्रकार की है तथापि संक्षेप में छः भेद करके (जैन) शास्त्र में उसका स्वरूप वर्णन किया गया है।
उत्तराध्ययनसूत्र में लेश्याओं के स्वरूप का निर्वाचन वर्ग, गन्ध, रस, स्पर्श, मनोभाव, कर्म आदि अनेक पक्षों के आधार पर हुआ है, लेकिन हम अपने विवेचन को लेश्याओं के भावात्मक पक्ष तक
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org.