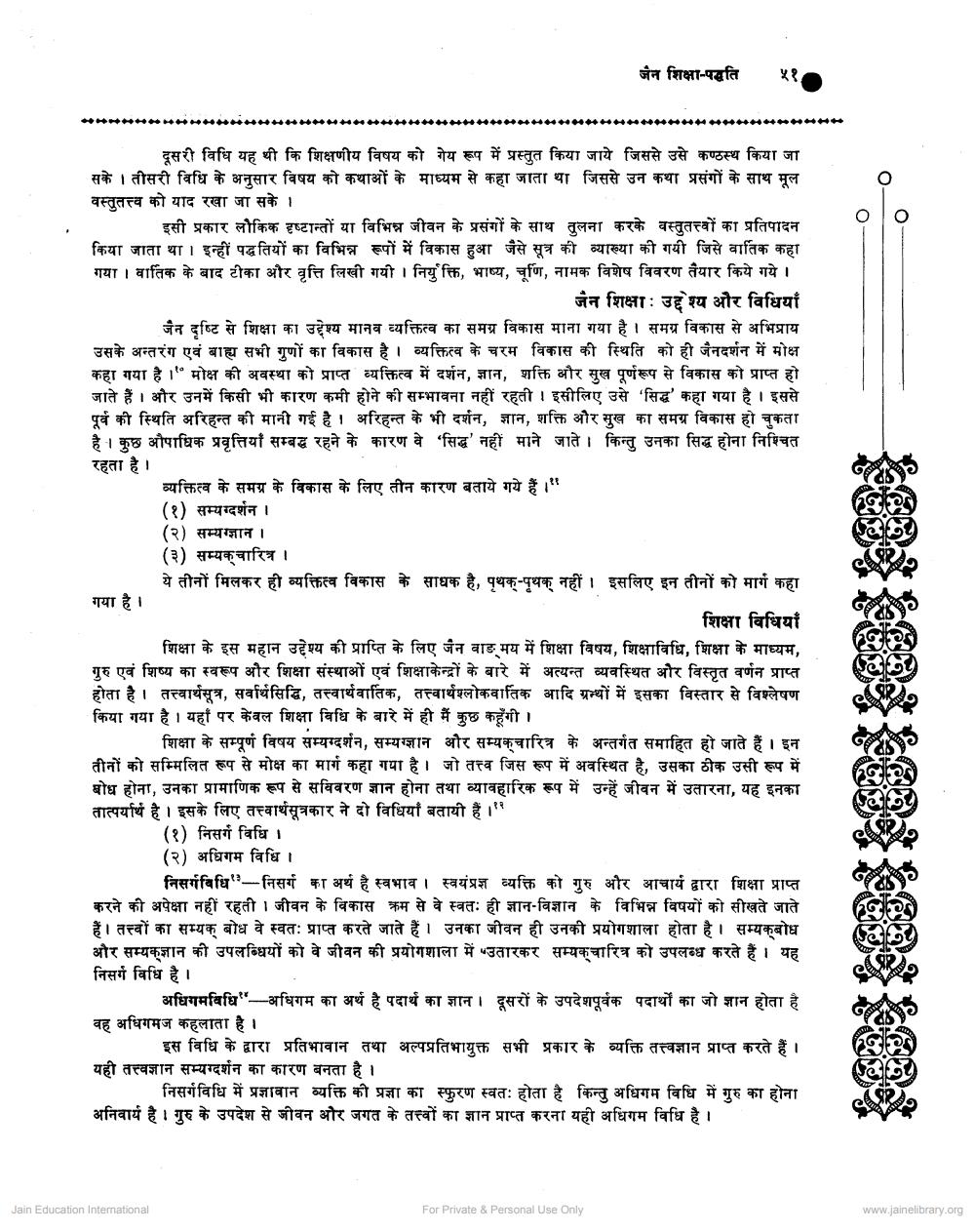________________
जैन शिक्षा-पद्धति
५१.
००
दूसरी विधि यह थी कि शिक्षणीय विषय को गेय रूप में प्रस्तुत किया जाये जिससे उसे कण्ठस्थ किया जा सके । तीसरी विधि के अनुसार विषय को कथाओं के माध्यम से कहा जाता था जिससे उन कथा प्रसंगों के साथ मूल वस्तुतत्त्व को याद रखा जा सके ।
इसी प्रकार लौकिक दृष्टान्तों या विभिन्न जीवन के प्रसंगों के साथ तुलना करके वस्तुतत्त्वों का प्रतिपादन किया जाता था। इन्हीं पद्धतियों का विभिन्न रूपों में विकास हुआ जैसे सूत्र की व्याख्या की गयी जिसे वार्तिक कहा गया। वार्तिक के बाद टीका और वृत्ति लिखी गयी । नियुक्ति, भाष्य, चूणि, नामक विशेष विवरण तैयार किये गये ।
जैन शिक्षाः उद्देश्य और विधियाँ जैन दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का समग्र विकास माना गया है। समग्र विकास से अभिप्राय उसके अन्तरंग एवं बाह्य सभी गुणों का विकास है। व्यक्तित्व के चरम विकास की स्थिति को ही जैनदर्शन में मोक्ष कहा गया है। मोक्ष की अवस्था को प्राप्त व्यक्तित्व में दर्शन, ज्ञान, शक्ति और सुख पूर्णरूप से विकास को प्राप्त हो जाते हैं। और उनमें किसी भी कारण कमी होने की सम्भावना नहीं रहती। इसीलिए उसे 'सिद्ध' कहा गया है। इससे पूर्व की स्थिति अरिहन्त की मानी गई है। अरिहन्त के भी दर्शन, ज्ञान, शक्ति और सुख का समग्र विकास हो चुकता है । कुछ औपाधिक प्रवृत्तियाँ सम्बद्ध रहने के कारण वे 'सिद्ध' नहीं माने जाते। किन्तु उनका सिद्ध होना निश्चित रहता है।
व्यक्तित्व के समग्र के विकास के लिए तीन कारण बताये गये हैं।" (१) सम्यग्दर्शन । (२) सम्यग्ज्ञान। (३) सम्यक्चारित्र ।
ये तीनों मिलकर ही व्यक्तित्व विकास के साधक है, पृथक्-पृथक् नहीं। इसलिए इन तीनों को मार्ग कहा गया है।
शिक्षा विधियाँ शिक्षा के इस महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जैन वाङमय में शिक्षा विषय, शिक्षाविधि, शिक्षा के माध्यम, गुरु एवं शिष्य का स्वरूप और शिक्षा संस्थाओं एवं शिक्षाकेन्द्रों के बारे में अत्यन्त व्यवस्थित और विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। तत्त्वार्थसूत्र, सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वार्थवार्तिक, तत्त्वार्थश्लोकवातिक आदि ग्रन्थों में इसका विस्तार से विश्लेषण किया गया है। यहाँ पर केवल शिक्षा विधि के बारे में ही मैं कुछ कहूँगी।
शिक्षा के सम्पूर्ण विषय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र के अन्तर्गत समाहित हो जाते हैं । इन तीनों को सम्मिलित रूप से मोक्ष का मार्ग कहा गया है। जो तत्त्व जिस रूप में अवस्थित है, उसका ठीक उसी रूप में बोध होना, उनका प्रामाणिक रूप से सविवरण ज्ञान होना तथा व्यावहारिक रूप में उन्हें जीवन में उतारना, यह इनका तात्पर्यार्थ है । इसके लिए तत्त्वार्थसूत्रकार ने दो विधियां बतायी हैं । १२
(१) निसर्ग विधि। (२) अधिगम विधि।
निसर्गविधि-निसर्ग का अर्थ है स्वभाव । स्वयंप्रज्ञ व्यक्ति को गुरु और आचार्य द्वारा शिक्षा प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं रहती। जीवन के विकास क्रम से वे स्वतः ही ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न विषयों को सीखते जाते हैं। तत्त्वों का सम्यक् बोध वे स्वतः प्राप्त करते जाते हैं। उनका जीवन ही उनकी प्रयोगशाला होता है। सम्यक्बोध
और सम्यक्ज्ञान की उपलब्धियों को वे जीवन की प्रयोगशाला में "उतारकर सम्यक्चारित्र को उपलब्ध करते हैं। यह निसर्ग विधि है।
अधिगमविधि"-अधिगम का अर्थ है पदार्थ का ज्ञान। दूसरों के उपदेशपूर्वक पदार्थों का जो ज्ञान होता है वह अधिगमज कहलाता है।
इस विधि के द्वारा प्रतिभावान तथा अल्पप्रतिभायुक्त सभी प्रकार के व्यक्ति तत्त्वज्ञान प्राप्त करते हैं। यही तत्त्वज्ञान सम्यग्दर्शन का कारण बनता है।
निसर्गविधि में प्रज्ञावान व्यक्ति की प्रज्ञा का स्फुरण स्वतः होता है किन्तु अधिगम विधि में गुरु का होना अनिवार्य है। गुरु के उपदेश से जीवन और जगत के तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त करना यही अधिगम विधि है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org