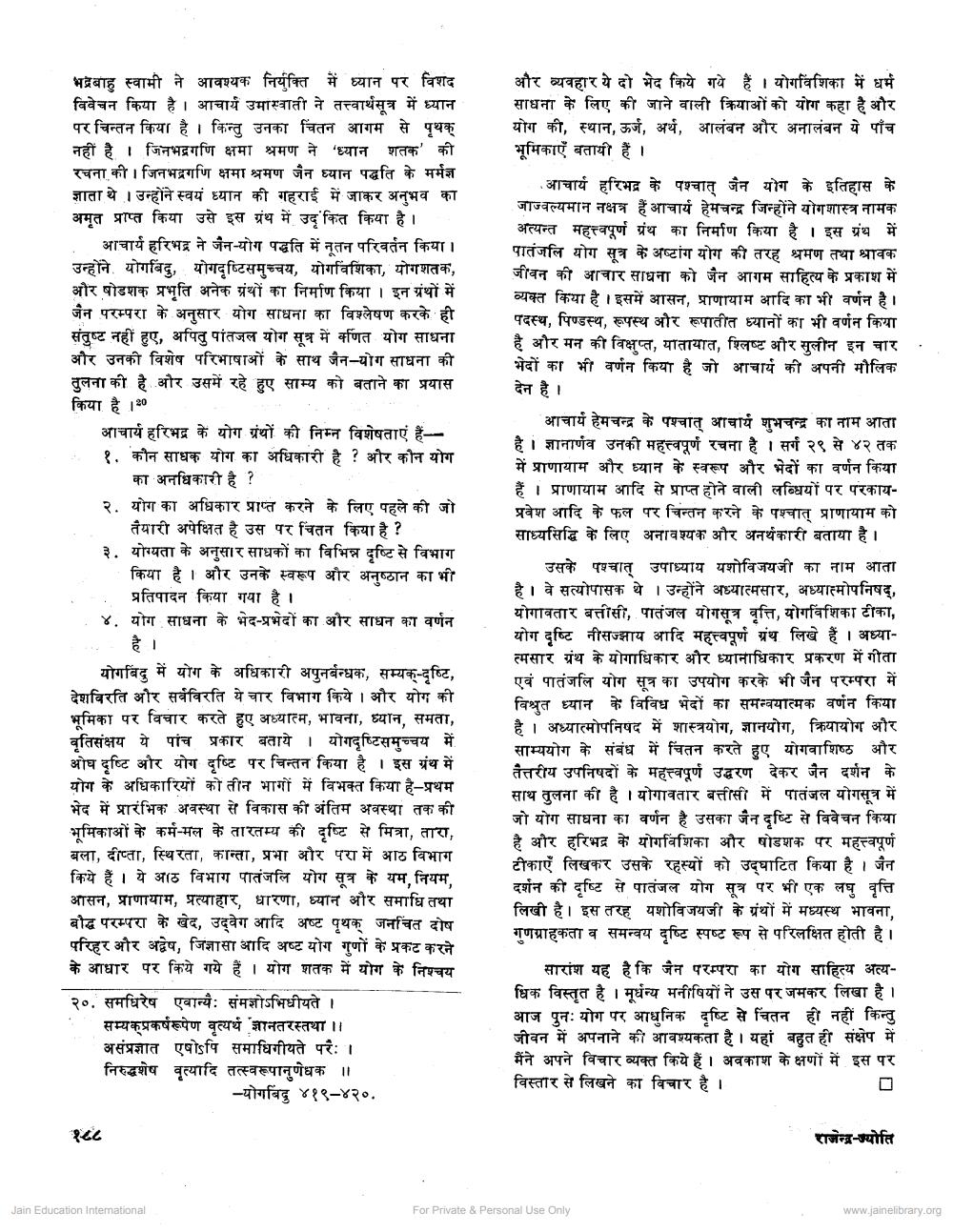________________ भद्रबाहु स्वामी ने आवश्यक नियुक्ति में ध्यान पर विशद विवेचन किया है। आचार्य उमास्वाती ने तत्त्वार्थसूत्र में ध्यान पर चिन्तन किया है। किन्तु उनका चिंतन आगम से पृथक् नहीं है / जिनभद्रगणि क्षमा श्रमण ने 'ध्यान शतक' की रचना की / जिनभद्रगणि क्षमा श्रमण जैन ध्यान पद्धति के मर्मज्ञ ज्ञाता थे / उन्होंने स्वयं ध्यान की गहराई में जाकर अनुभव का अमृत प्राप्त किया उसे इस ग्रंथ में उदृ'कित किया है। . आचार्य हरिभद्र ने जैन-योग पद्धति में नूतन परिवर्तन किया। उन्होंने योगबिंदु, योगदृष्टिसमुच्चय, योगविशिका, योगशतक, और षोडशक प्रभृति अनेक ग्रंथों का निर्माण किया / इन ग्रंथों में जैन परम्परा के अनुसार योग साधना का विश्लेषण करके ही संतुष्ट नहीं हुए, अपितु पांतजल योग सूत्र में कणित योग साधना और उनकी विशेष परिभाषाओं के साथ जैन-योग साधना की तुलना की है और उसमें रहे हुए साम्य को बताने का प्रयास किया है / आचार्य हरिभद्र के योग ग्रंथों की निम्न विशेषताएं हैं१. कौन साधक योग का अधिकारी है ? और कौन योग का अनधिकारी है ? 2. योग का अधिकार प्राप्त करने के लिए पहले की जो तैयारी अपेक्षित है उस पर चितन किया है ? 3. योग्यता के अनुसार साधकों का विभिन्न दृष्टि से विभाग किया है / और उनके स्वरूप और अनुष्ठान का भी प्रतिपादन किया गया है। . 4. योग साधना के भेद-प्रभेदों का और साधन का वर्णन और व्यवहार ये दो भेद किये गये हैं / योगविंशिका में धर्म साधना के लिए की जाने वाली क्रियाओं को योग कहा है और योग की, स्थान, ऊर्ज, अर्थ, आलंबन और अनालंबन ये पाँच भूमिकाएँ बतायी हैं। आचार्य हरिभद्र के पश्चात् जैन योग के इतिहास के जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं आचार्य हेमचन्द्र जिन्होंने योगशास्त्र नामक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रंथ का निर्माण किया है / इस ग्रंथ में पातंजलि योग सूत्र के अष्टांग योग की तरह श्रमण तथा श्रावक जीवन की आचार साधना को जैन आगम साहित्य के प्रकाश में व्यक्त किया है / इसमें आसन, प्राणायाम आदि का भी वर्णन है। पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यानों का भी वर्णन किया है और मन की विक्षुप्त, यातायात, श्लिष्ट और सुलीन इन चार भेदों का भी वर्णन किया है जो आचार्य की अपनी मौलिक देन है। आचार्य हेमचन्द्र के पश्चात् आचार्य शुभचन्द्र का नाम आता है। ज्ञानार्णव उनकी महत्त्वपूर्ण रचना है / सर्ग 29 से 42 तक में प्राणायाम और ध्यान के स्वरूप और भेदों का वर्णन किया हैं / प्राणायाम आदि से प्राप्त होने वाली लब्धियों पर परकायप्रवेश आदि के फल पर चिन्तन करने के पश्चात् प्राणायाम को साध्यसिद्धि के लिए अनावश्यक और अनर्थकारी बताया है। उसके पश्चात् उपाध्याय यशोविजयजी का नाम आता है। वे सत्योपासक थे / उन्होंने अध्यात्मसार, अध्यात्मोपनिषद्, योगावतार बत्तीसी, पातंजल योगसूत्र वृत्ति, योगविंशिका टीका, योग दृष्टि नीसज्झाय आदि महत्त्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं / अध्यात्मसार ग्रंथ के योगाधिकार और ध्यानाधिकार प्रकरण में गीता एवं पातंजलि योग सूत्र का उपयोग करके भी जैन परम्परा में विश्रुत ध्यान के विविध भेदों का समन्वयात्मक वर्णन किया है। अध्यात्मोपनिषद में शास्त्रयोग, ज्ञानयोग, क्रियायोग और साम्ययोग के संबंध में चिंतन करते हुए योगवाशिष्ठ और तैत्तरीय उपनिषदों के महत्त्वपूर्ण उद्धरण देकर जैन दर्शन के साथ तुलना की है / योगावतार बत्तीसी में पातंजल योगसूत्र में जो योग साधना का वर्णन है उसका जैन दृष्टि से विवेचन किया है और हरिभद्र के योगविशिका और षोडशक पर महत्त्वपूर्ण टीकाएँ लिखकर उसके रहस्यों को उद्घाटित किया है / जैन दर्शन की दृष्टि से पातंजल योग सूत्र पर भी एक लघु वृत्ति लिखी है। इस तरह यशोविजयजी के ग्रंथों में मध्यस्थ भावना, गुणग्राहकता व समन्वय दृष्टि स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। सारांश यह है कि जैन परम्परा का योग साहित्य अत्यधिक विस्तृत है / मूर्धन्य मनीषियों ने उस पर जमकर लिखा है। आज पुनः योग पर आधुनिक दृष्टि से चिंतन ही नहीं किन्तु जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। यहां बहुत ही संक्षेप में मैंने अपने विचार व्यक्त किये हैं। अवकाश के क्षणों में इस पर विस्तार से लिखने का विचार है / योगबिंदु में योग के अधिकारी अपुनर्बन्धक, सम्यक्-दृष्टि, देशविरति और सर्वविरति ये चार विभाग किये / और योग की भूमिका पर विचार करते हुए अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता, वृतिसंक्षय ये पांच प्रकार बताये / योगदृष्टिसमुच्चय में ओघ दृष्टि और योग दृष्टि पर चिन्तन किया है / इस ग्रंथ में योग के अधिकारियों को तीन भागों में विभक्त किया है-प्रथम भेद में प्रारंभिक अवस्था से विकास की अंतिम अवस्था तक की भूमिकाओं के कर्म-मल के तारतम्य की दृष्टि से मित्रा, तारा, बला, दीप्ता, स्थिरता, कान्ता, प्रभा और परा में आठ विभाग किये हैं / ये आठ विभाग पातंजलि योग सूत्र के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तथा बौद्ध परम्परा के खेद, उद्वेग आदि अष्ट पृथक् जनचित दोष परिहर और अद्वेष, जिज्ञासा आदि अष्ट योग गुणों के प्रकट करने के आधार पर किये गये हैं / योग शतक में योग के निश्चय 20. समधिरेष एवान्यैः संमज्ञोऽभिधीयते / सम्यक्प्रकर्षरूपेण वृत्यर्थ ज्ञानतरस्तथा / / असंप्रज्ञात एषोऽपि समाधिगीयते परैः / निरुद्धशेष वृत्यादि तत्स्वरूपानुणेधक // -योगबिंदु 419-420. 188 राजेन्द्र-ज्योति Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org