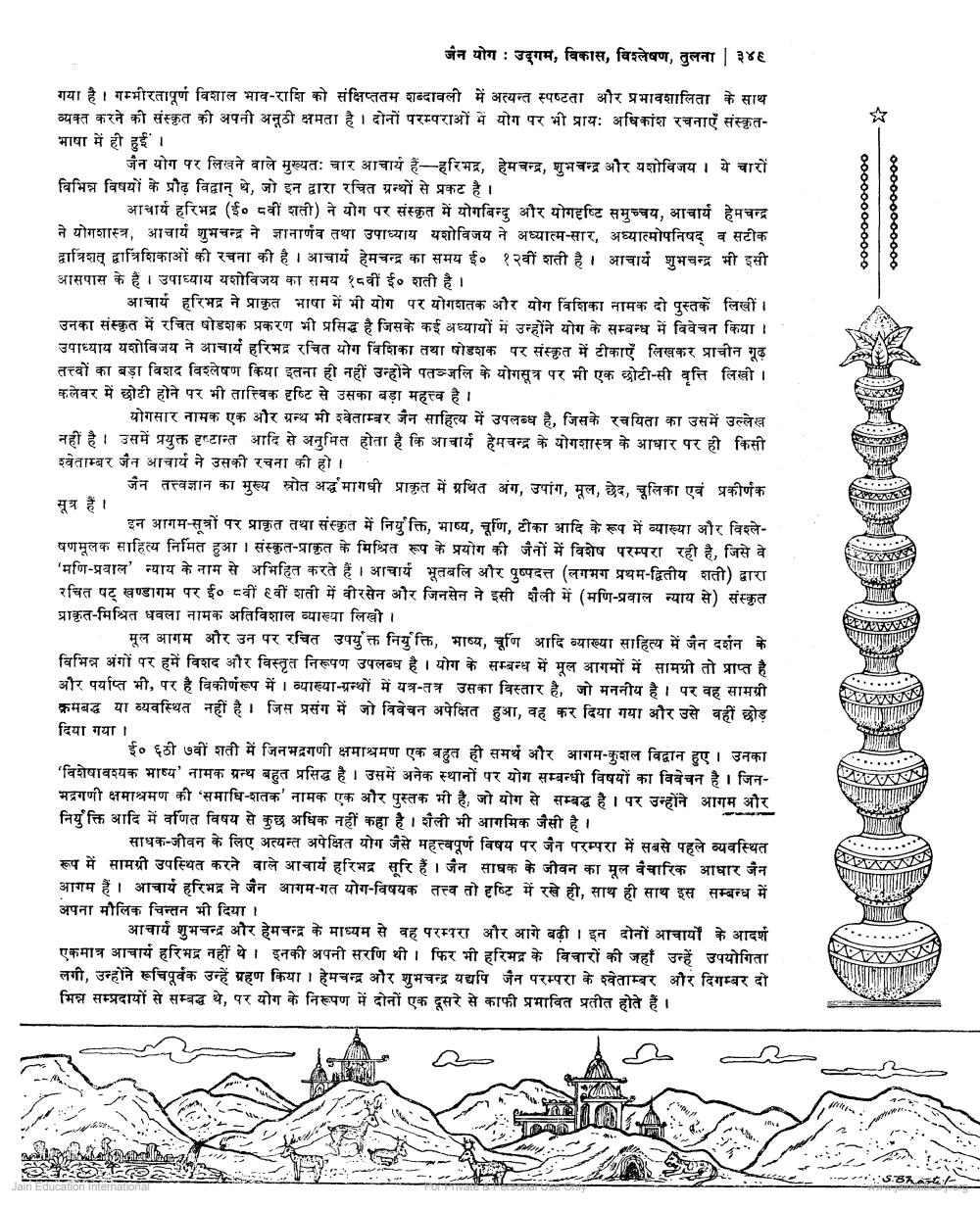________________
जंग योग उद्गम, विकास, विश्लेषण, तुलना | १४६
गया है । गम्भीरतापूर्ण विशाल भाव राशि को संक्षिप्ततम शब्दावली में अत्यन्त स्पष्टता और प्रभावशालिता के साथ व्यक्त करने की संस्कृत की अपनी अनूठी क्षमता है। दोनों परम्पराओं में योग पर भी प्रायः अधिकांश रचनाएँ संस्कृतभाषा में ही हुई ।
जैन योग पर लिखने वाले मुख्यतः चार आचार्य हैं - हरिभद्र, हेमचन्द्र, शुभचन्द्र और यशोविजय । ये चारों विभिन्न विषयों के प्रौढ़ विद्वान् थे, जो इन द्वारा रचित ग्रन्थों से प्रकट है ।
आचार्य हरिभद्र ( ई० ८वीं शती) ने योग पर संस्कृत में योगबिन्दु और योगदृष्टि समुच्चय, आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र, आचार्य शुभचन्द्र ने ज्ञानार्णव तथा उपाध्याय यशोविजय ने अध्यात्म-सार, अध्यात्मोपनिषद् व सटीक द्वात्रिंशत् द्वात्रिंशिकाओं की रचना की है। आचार्य हेमचन्द्र का समय ई० १२वीं शती है। आचार्य शुभचन्द्र भी इसी आसपास के हैं । उपाध्याय यशोविजय का समय १८वीं ई० शती है ।
आचार्य हरिभद्र ने प्राकृत भाषा में भी योग पर योगशतक और योग विशिका नामक दो पुस्तकें लिखीं। उनका संस्कृत में रचित षोडशक प्रकरण भी प्रसिद्ध है जिसके कई अध्यायों में उन्होंने योग के सम्बन्ध में विवेचन किया । उपाध्याय यशोविजय ने आचार्य हरिभद्र रचित योग विंशिका तथा षोडशक पर संस्कृत में टीकाएँ लिखकर प्राचीन गूढ़ तत्त्वों का बड़ा विशद विश्लेषण किया इतना ही नहीं उन्होंने पतञ्जलि के योगसूत्र पर मी एक छोटी-सी वृत्ति लिखी । कलेवर में छोटी होने पर भी तात्त्विक दृष्टि से उसका बड़ा महत्त्व है ।
योगसार नामक एक और ग्रन्थ मी श्वेताम्बर जैन साहित्य में उपलब्ध है, जिसके रचयिता का उसमें उल्लेख नहीं है । उसमें प्रयुक्त दृष्टान्त आदि से अनुमित होता है कि आचार्य हेमचन्द्र के योगशास्त्र के आधार पर ही किसी श्वेताम्बर जैन आचार्य ने उसकी रचना की हो।
जैन तत्त्वज्ञान का मुख्य स्रोत अर्द्धमागधी प्राकृत में ग्रथित अंग, उपांग, मूल, छेद, चूलिका एवं प्रकीर्णक
सूत्र है।
इन आगम-सूत्रों पर प्राकृत तथा संस्कृत में नियुक्ति, भाष्य, चूणि, टीका आदि के रूप में व्याख्या और विश्लेषणमूलक साहित्य निर्मित हुआ । संस्कृत प्राकृत के मिश्रित रूप के प्रयोग की जैनों में विशेष परम्परा रही है, जिसे वे 'मणि प्रवाल' न्याय के नाम से अभिहित करते हैं। आचार्य भूतबलि और पुष्पदत्त (लगभग प्रथम द्वितीय शती) द्वारा रचित षट् खण्डागम पर ई० ८वीं ध्वीं शती में वीरसेन और जिनसेन ने इसी शैली में (मणि - प्रवाल न्याय से ) संस्कृत प्राकृत- मिश्रित धवला नामक अतिविशाल व्याख्या लिखी ।
मूल आगम और उन पर रचित उपर्युक्त नियुक्ति, भाष्य, चूर्णि आदि व्याख्या साहित्य में जैन दर्शन के विभिन्न अंगों पर हमें विशद और विस्तृत निरूपण उपलब्ध है। योग के सम्बन्ध में मूल आगमों में सामग्री तो प्राप्त है और पर्याप्त भी, पर है विकीर्णरूप में । व्याख्या-ग्रन्थों में यत्र-तत्र उसका विस्तार है, जो मननीय है । पर वह सामग्री क्रमबद्ध या व्यवस्थित नहीं है। जिस प्रसंग में जो विवेचन अपेक्षित हुआ, वह कर दिया गया और उसे वहीं छोड़ दिया गया ।
ई० ६ठी ७वीं शती में जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण एक बहुत ही समर्थ और आगम-कुशल विद्वान हुए। उनका 'विशेषावश्यक भाष्य' नामक ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध है। उसमें अनेक स्थानों पर योग सम्बन्धी विषयों का विवेचन है । जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण की 'समाधि-शतक' नामक एक और पुस्तक भी है, जो योग से सम्बद्ध है । पर उन्होंने आगम और नियुक्ति आदि में वर्णित विषय से कुछ अधिक नहीं कहा है। शैली भी आगमिक जैसी है ।
साधक - जीवन के लिए अत्यन्त अपेक्षित योग जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर जैन परम्परा में सबसे पहले व्यवस्थित रूप में सामग्री उपस्थित करने वाले आचार्य हरिभद्र सूरि हैं। जैन साधक के जीवन का मूल वैचारिक आधार जैन आगम हैं । आचार्य हरिभद्र ने जैन आगम-गत योग-विषयक तत्त्व तो दृष्टि में रखे ही, साथ ही साथ इस अपना मौलिक चिन्तन भी दिया ।
सम्बन्ध में
विचारों की जहाँ उन्हें उपयोगिता
आचार्य शुभचन्द्र और हेमचन्द्र के माध्यम से वह परम्परा और आगे बढ़ी। इन दोनों आचार्यों के आदर्श एकमात्र आचार्य हरिभद्र नहीं थे। इनकी अपनी सरणि थी। फिर भी हरिभद्र के लगी, उन्होंने रूचिपूर्वक उन्हें ग्रहण किया। हेमचन्द्र और शुभचन्द्र यद्यपि जैन परम्परा के श्वेताम्बर और दिगम्बर दो भिन्न सम्प्रदायों से सम्बद्ध थे, पर योग के निरूपण में दोनों एक दूसरे से काफी प्रभावित प्रतीत होते हैं।
Jain Education International
pu
K
23
سے
ooooooooo000 000000000000
*CODECFEES
5.8haste/