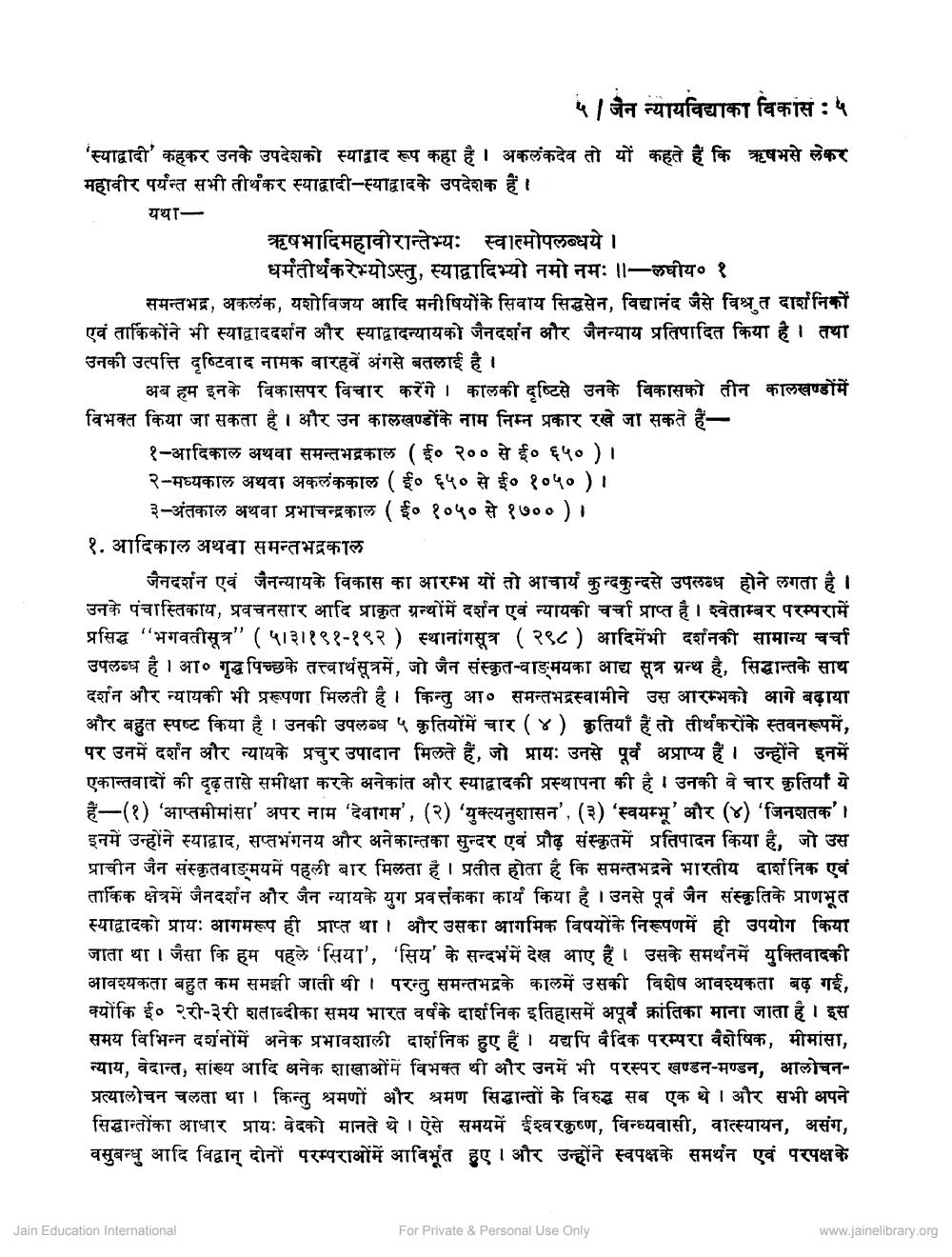________________
५ / जैन न्यायविद्याका विकास : ५
'स्याद्वादी' कहकर उनके उपदेशको स्याद्वाद रूप कहा है। अकलंकदेव तो यों कहते हैं कि ऋषभसे लेकर महावीर पर्यन्त सभी तीर्थंकर स्याद्वादी-स्याद्वादके उपदेशक हैं। यथा
ऋषभादिमहावीरान्तेभ्यः स्वात्मोपलब्धये ।
धर्मतीर्थकरेभ्योऽस्तु, स्याद्वादिभ्यो नमो नमः ।।-लघीय० १ समन्तभद्र, अकलंक, यशोविजय आदि मनीषियोंके सिवाय सिद्धसेन, विद्यानंद जैसे विश्रुत दार्शनिकों एवं ताकिकोंने भी स्याद्वाददर्शन और स्याद्वादन्यायको जैनदर्शन और जैनन्याय प्रतिपादित किया है। तथा उनकी उत्पत्ति दृष्टिवाद नामक बारहवें अंगसे बतलाई है।
अब हम इनके विकासपर विचार करेंगे। कालकी दष्टिसे उनके विकासको तीन कालखण्डोंमें विभक्त किया जा सकता है। और उन कालखण्डोंके नाम निम्न प्रकार रखे जा सकते हैं
१-आदिकाल अथवा समन्तभद्रकाल (ई० २०० से ई० ६५० )। २-मध्यकाल अथवा अकलंककाल (ई०६५० से ई० १०५०)।
३-अंतकाल अथवा प्रभाचन्द्रकाल (ई०१०५० से १७००)। १. आदिकाल अथवा समन्तभद्रकाल
जैनदर्शन एवं जैनन्यायके विकास का आरम्भ यों तो आचार्य कुन्दकुन्दसे उपलब्ध होने लगता है। उनके पंचास्तिकाय, प्रवचनसार आदि प्राकृत ग्रन्थोंमें दर्शन एवं न्यायकी चर्चा प्राप्त है । श्वेताम्बर परम्परामें प्रसिद्ध "भगवतीसूत्र" ( ५।३।१९१-१९२) स्थानांगसूत्र ( २९८) आदिमेंभी दर्शनकी सामान्य चर्चा उपलब्ध है । आ० गृद्ध पिच्छके तत्त्वार्थसूत्रमें, जो जैन संस्कृत-वाङ्मयका आद्य सूत्र ग्रन्थ है, सिद्धान्तके साथ दर्शन और न्यायकी भी प्ररूपणा मिलती है। किन्तु आ० समन्तभद्रस्वामीने उस आरम्भको आगे बढ़ाया और बहुत स्पष्ट किया है । उनकी उपलब्ध ५ कृतियोंमें चार (४) कृतियाँ हैं तो तीर्थंकरोंके स्तवनरूपमें, पर उनमें दर्शन और न्यायके प्रचुर उपादान मिलते हैं, जो प्रायः उनसे पूर्व अप्राप्य हैं। उन्होंने इनमें एकान्तवादों की दृढ़तासे समीक्षा करके अनेकांत और स्याद्वादकी प्रस्थापना की है। उनकी वे चार कृतियाँ ये हैं-(१) 'आप्तमीमांसा' अपर नाम 'देवागम', (२) 'युक्त्यनुशासन', (३) 'स्वयम्भू' और (४) 'जिनशतक'। इनमें उन्होंने स्याद्वाद, सप्तभंगनय और अनेकान्तका सुन्दर एवं प्रौढ़ संस्कृतमें प्रतिपादन किया है, जो उस प्राचीन जैन संस्कृतवाङ्मयमें पहली बार मिलता है । प्रतीत होता है कि समन्तभद्रने भारतीय दार्शनिक एवं तार्किक क्षेत्रमें जैनदर्शन और जैन न्यायके युग प्रवर्तकका कार्य किया है । उनसे पूर्व जैन संस्कृतिके प्राणभूत स्याद्वादको प्रायः आगमरूप ही प्राप्त था। और उसका आगमिक विषयों के निरूपणमें ही उपयोग किया जाता था । जैसा कि हम पहले 'सिया', 'सिय' के सन्दर्भ में देख आए हैं। उसके समर्थनमें युक्तिवादकी आवश्यकता बहुत कम समझी जाती थी। परन्तु समन्तभद्रके कालमें उसकी विशेष आवश्यकता बढ़ गई, क्योंकि ई० २री-३री शताब्दीका समय भारत वर्षके दार्शनिक इतिहासमें अपूर्व क्रांतिका माना जाता है। इस समय विभिन्न दर्शनोंमें अनेक प्रभावशाली दार्शनिक हए हैं। यद्यपि वैदिक परम्परा वैशेषिक, मीमांसा, न्याय, वेदान्त, सांख्य आदि अनेक शाखाओं में विभक्त थी और उनमें भी परस्पर खण्डन-मण्डन, आलोचनप्रत्यालोचन चलता था। किन्तु श्रमणों और श्रमण सिद्धान्तों के विरुद्ध सब एक थे । और सभी अपने सिद्धान्तोंका आधार प्रायः वेदको मानते थे । ऐसे समयमें ईश्वरकृष्ण, विन्ध्यवासी, वात्स्यायन, असंग, वसुबन्धु आदि विद्वान दोनों परम्पराओंमें आविर्भूत हुए । और उन्होंने स्वपक्षके समर्थन एवं परपक्षके
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org