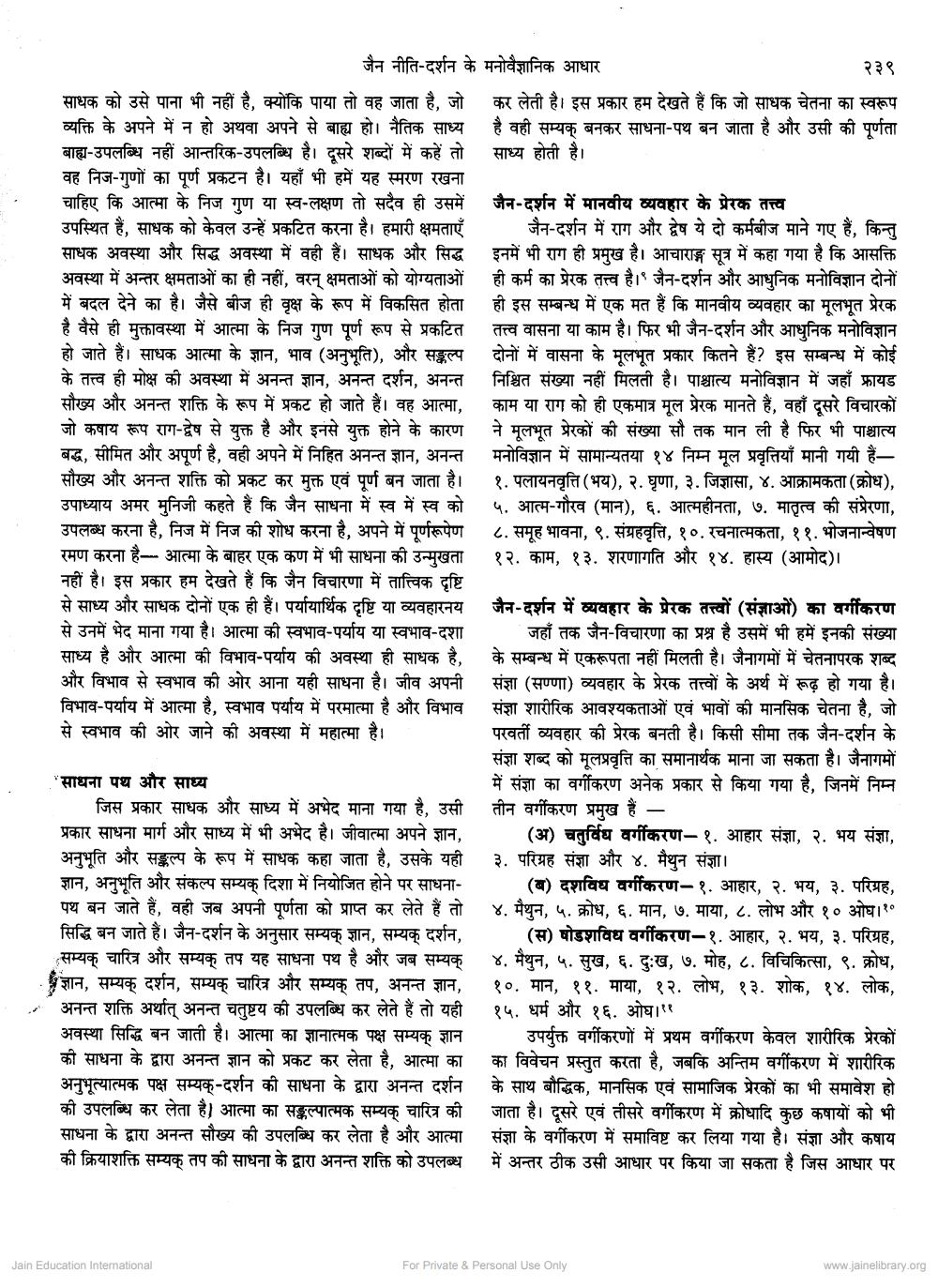________________
जैन नीति दर्शन के साधक को उसे पाना भी नहीं है, क्योंकि पाया तो वह जाता है, जो व्यक्ति के अपने में न हो अथवा अपने से बाह्य हो नैतिक साध्य बाह्य-उपलब्धि नहीं आन्तरिक उपलब्धि है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह निज-गुणों का पूर्ण प्रकटन है। यहाँ भी हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा के निज गुण या स्व-लक्षण तो सदैव ही उसमें उपस्थित हैं, साधक को केवल उन्हें प्रकटित करना है । हमारी क्षमताएँ साधक अवस्था और सिद्ध अवस्था में वही हैं। साधक और सिद्ध अवस्था में अन्तर क्षमताओं का ही नहीं, वरन् क्षमताओं को योग्यताओं में बदल देने का है। जैसे बीज ही वृक्ष के रूप में विकसित होता है वैसे ही मुक्तावस्था में आत्मा के निज गुण पूर्ण रूप से प्रकटित हो जाते हैं। साधक आत्मा के ज्ञान, भाव (अनुभूति), और सङ्कल्प के तत्त्व ही मोक्ष की अवस्था में अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सौख्य और अनन्त शक्ति के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वह आत्मा, जो कषाय रूप राग-द्वेष से युक्त है और इनसे युक्त होने के कारण बद्ध, सीमित और अपूर्ण है, वही अपने में निहित अनन्त ज्ञान, अनन्त सौख्य और अनन्त शक्ति को प्रकट कर मुक्त एवं पूर्ण बन जाता है। उपाध्याय अमर मुनिजी कहते हैं कि जैन साधना में स्व में स्व को उपलब्ध करना है, निज में निज की शोध करना है, अपने में पूर्णरूपेण रमण करना है --- आत्मा के बाहर एक कण में भी साधना की उन्मुखता नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन विचारणा में तात्त्विक दृष्टि से साध्य और साधक दोनों एक ही हैं। पर्यायार्थिक दृष्टि या व्यवहारनय से उनमें भेद माना गया है। आत्मा की स्वभाव-पर्याय या स्वभाव- दशा साध्य है और आत्मा की विभाव पर्याय की अवस्था ही साधक है, और विभाव से स्वभाव की ओर आना यही साधना है जीव अपनी विभाव- पर्याय में आत्मा है स्वभाव पर्याय में परमात्मा है और विभाव से स्वभाव की ओर जाने की अवस्था में महात्मा है।
* साधना पथ और साध्य
जिस प्रकार साधक और साध्य में अभेद माना गया है, उसी प्रकार साधना मार्ग और साध्य में भी अभेद है। जीवात्मा अपने ज्ञान, अनुभूति और सङ्कल्प के रूप में साधक कहा जाता है, उसके यही ज्ञान, अनुभूति और संकल्प सम्यक् दिशा में नियोजित होने पर साधनापथ बन जाते हैं, वही जब अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं तो सिद्धि बन जाते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन, सम्यक् चारित्र और सम्यक् तप यह साधना पथ है और जब सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन, सम्यक् चारित्र और सम्यक् तप, अनन्त ज्ञान, अनन्त शक्ति अर्थात् अनन्त चतुष्टय की उपलब्धि कर लेते हैं तो यही अवस्था सिद्धि बन जाती है। आत्मा का ज्ञानात्मक पक्ष सम्यक् ज्ञान की साधना के द्वारा अनन्त ज्ञान को प्रकट कर लेता है, आत्मा का अनुभूत्यात्मक पक्ष सम्यक् दर्शन की साधना के द्वारा अनन्त दर्शन की उपलब्धि कर लेता है। आत्मा का सङ्कल्पात्मक सम्यक चारित्र की साधना के द्वारा अनन्त सौख्य की उपलब्धि कर लेता है और आत्मा की क्रियाशक्ति सम्यक् तप की साधना के द्वारा अनन्त शक्ति को उपलब्ध
Jain Education International
मनोवैज्ञानिक आधार
२३९ कर लेती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो साधक चेतना का स्वरूप है वही सम्यक् बनकर साधना पथ बन जाता है और उसी की पूर्णता साध्य होती है।
जैन दर्शन में मानवीय व्यवहार के प्रेरक तत्त्व
जैन दर्शन में राग और द्वेष ये दो कर्मबीज माने गए हैं, किन्तु इनमें भी राग ही प्रमुख है। आचाराङ्ग सूत्र में कहा गया है कि आसक्ति ही कर्म का प्रेरक तत्व है।" जैन दर्शन और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों ही इस सम्बन्ध में एक मत हैं कि मानवीय व्यवहार का मूलभूत प्रेरक तत्त्व वासना या काम है फिर भी जैन दर्शन और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों में वासना के मूलभूत प्रकार कितने हैं? इस सम्बन्ध में कोई निश्चित संख्या नहीं मिलती है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में जहाँ फ्रायड काम या राग को ही एकमात्र मूल प्रेरक मानते हैं, वहाँ दूसरे विचारकों ने मूलभूत प्रेरकों की संख्या सौ तक मान ली है फिर भी पाश्चात्य मनोविज्ञान में सामान्यतया १४ निम्न मूल प्रवृत्तियाँ मानी गयी हैं१. पलायनवृत्ति (भय), २. घृणा, ३. जिज्ञासा, ४. आक्रामकता (क्रोध), ५. आत्म- गौरव (मान), ६. आत्महीनता, ७. मातृत्व की संप्रेरणा, ८. समूह भावना, ९ संग्रहवृत्ति, १० रचनात्मकता, ११. भोजनान्वेषण १२. काम १३. शरणागति और १४ हास्य (आमोद)।
·
जैन दर्शन में व्यवहार के प्रेरक तत्त्वों (संज्ञाओं) का वर्गीकरण जहाँ तक जैन- विचारणा का प्रश्न है उसमें भी हमें इनकी संख्या के सम्बन्ध में एकरूपता नहीं मिलती है। जैनागमों में चेतनापरक शब्द संज्ञा ( सण्णा) व्यवहार के प्रेरक तत्त्वों के अर्थ में रूढ़ हो गया है। संज्ञा शारीरिक आवश्यकताओं एवं भावों की मानसिक चेतना है, जो परवर्ती व्यवहार की प्रेरक बनती है किसी सीमा तक जैन दर्शन के संज्ञा शब्द को मूलप्रवृत्ति का समानार्थक माना जा सकता है। जैनागमों में संज्ञा का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है, जिनमें निम्न तीन वर्गीकरण प्रमुख हैं
-
—
(अ) चतुर्विध वर्गीकरण १. आहार संज्ञा, २. भय संज्ञा, ३. परिग्रह संज्ञा और ४ मैथुन संज्ञा
(ब) दशविध वर्गीकरण- १. आहार, २. भय, ३. परिग्रह, ४. मैथुन, ५. क्रोध, ६. मान, ७ माया, ८. लोभ और १० ओघ । १०
(स) षोडशविध वर्गीकरण- १. आहार, २. भय, ३ परिग्रह, ४. मैथुन, ५. सुख, ६. दुःख, ७. मोह, ८. विचिकित्सा, ९. क्रोध, १०. मान, ११. माया, १२. लोभ, १३. शोक, १४. लोक, १५. धर्म और १६. ओघ । १९
उपर्युक्त वर्गीकरणों में प्रथम वर्गीकरण केवल शारीरिक प्रेरकों का विवेचन प्रस्तुत करता है, जबकि अन्तिम वर्गीकरण में शारीरिक के साथ बौद्धिक, मानसिक एवं सामाजिक प्रेरकों का भी समावेश हो जाता है। दूसरे एवं तीसरे वर्गीकरण में क्रोधादि कुछ कषायों को भी संज्ञा के वर्गीकरण में समाविष्ट कर लिया गया है। संज्ञा और कषाय में अन्तर ठीक उसी आधार पर किया जा सकता है जिस आधार पर
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org.