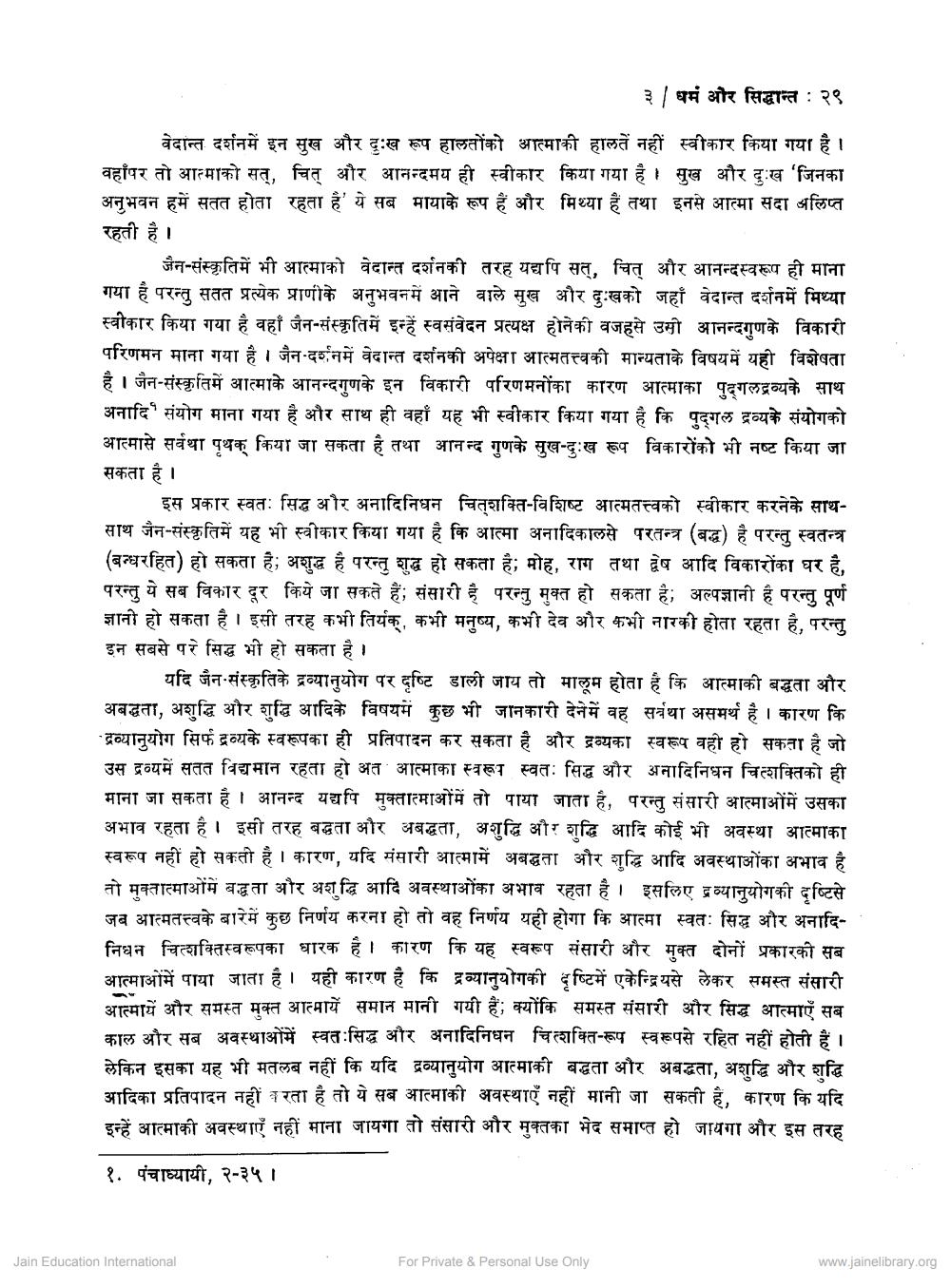________________
३ / धर्म और सिद्धान्त २९
वेदान्त दर्शनमें इन सुख और दुःख रूप हालतोंको आत्माकी हालतें नहीं स्वीकार किया गया है । वहाँपर तो आत्माको सत्, चित् और आनन्दमय ही स्वीकार किया गया है। सुख और दुःख 'जिनका अनुभवन हमें सतत होता रहता है ये सब मायाके रूप हैं और मिथ्या है तथा इनसे आत्मा सदा अलिप्त रहती है।
जैन-संस्कृतिमें भी आत्माको वेदान्त दर्शनकी तरह यद्यपि सत्, चित् और आनन्दस्वरूप ही माना गया है परन्तु सतत प्रत्येक प्राणी के अनुभवनमें आने वाले सुख और दुःखको जहाँ वेदान्त दर्शन में मिथ्या स्वीकार किया गया है वहाँ जैन-संस्कृतिमें इन्हें स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होने की वजहसे उमी आनन्दगुणके विकारी परिणमन माना गया है । जैन दर्शन में वेदान्त दर्शनकी अपेक्षा आत्मतत्त्वकी मान्यता के विषय में यही विशेषता है। जैन संस्कृतिमें आत्माके आनन्दगुणके इन विकारी परिणमनोंका कारण आत्माका पुद्गलद्रव्यके साथ अनादि संयोग माना गया है और साथ ही वहाँ यह भी स्वीकार किया गया है कि पुद्गल द्रव्यके संयोगको आत्मासे सर्वथा पृथक किया जा सकता है तथा आनन्द गुणके सुख-दुःख रूप विकारोंको भी नष्ट किया जा सकता है ।
इस प्रकार स्वतः सिद्ध और अनादिनिधन चितृशक्ति विशिष्ट आत्मतत्त्वको स्वीकार करनेके साथसाथ जैन - संस्कृति में यह भी स्वीकार किया गया है कि आत्मा अनादिकाल से परतन्त्र (बद्ध ) है परन्तु स्वतन्त्र (बन्धरहित) हो सकता है; अशुद्ध है परन्तु शुद्ध हो सकता है, मोह, राग तथा द्वेष आदि विकारोंका घर है, परन्तु ये सब विकार दूर किये जा सकते हैं; संसारी है परन्तु मुक्त हो सकता है; अल्पज्ञानी है परन्तु पूर्ण ज्ञानी हो सकता है। इसी तरह कभी तिर्यक्, कभी मनुष्य, कभी देव और कभी नारकी होता रहता है, परन्तु इन सबसे परे सिद्ध भी हो सकता है ।
यदि जैन संस्कृतिके द्रव्यानुयोग पर दृष्टि डाली जाय तो मालूम होता है कि आत्माकी बढता और सर्वथा असमर्थ है। कारण कि
स्वरूप वही हो सकता है जो अनादिनिधन चिलाक्तिको ही परन्तु संसारी आत्माओं में उसका
अवद्धता, अशुद्धि और बुद्धि आदिके विषय में कुछ भी जानकारी देने में वह - द्रव्यानुयोग सिर्फ द्रव्यके स्वरूपका ही प्रतिपादन कर सकता है और द्रव्यका उस द्रव्य में सतत विद्यमान रहता हो अत आत्माका स्वरूप स्वतः सिद्ध और माना जा सकता है | आनन्द यद्यपि मुक्तात्माओं में तो पाया जाता है, अभाव रहता है। इसी तरह बढता और अबद्धता, अशुद्धि और शुद्धि आदि कोई भी अवस्था आत्माका स्वरूप नहीं हो सकती है। कारण, यदि संसारी आत्मामें अवद्धता और शुद्धि आदि अवस्थाओंका अभाव है तो मुक्तात्माओं में बढ़ता और अशुद्धि आदि अवस्थाओंका अभाव रहता है। इसलिए व्यानुयोगकी दृष्टिसे जब आत्मतत्त्वके बारेमें कुछ निर्णय करना हो तो वह निर्णय यही होगा कि आत्मा स्वतः सिद्ध और अनादिनिधन चित्याक्तिस्वरूपका धारक है। कारण कि यह स्वरूप संसारी और मुक्त दोनों प्रकारको सब आत्माओं में पाया जाता है। यही कारण है कि म्यानुयोगकी दृष्टिमें एकेन्द्रियसे लेकर समस्त संसारी आत्मायें और समस्त मुक्त आत्मायें समान मानी गयी हैं; क्योंकि समस्त संसारी और सिद्ध आत्माएँ सब काल और सब अवस्थाओं में स्वतः सिद्ध और अनादिनिधन चित्वावित रूप स्वरूपसे रहित नहीं होती है। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि यदि द्रव्यानुयोग आत्माकी बद्धता और अबद्धता, अशुद्धि और शुद्धि आदिका प्रतिपादन नहीं करता है तो ये सब आत्माको अवस्थाएँ नहीं मानी जा सकती है, कारण कि यदि इन्हें आत्माकी अवस्थाएँ नहीं माना जायगा तो संसारी और मुक्तका भेद समाप्त हो जायगा और इस तरह
१. पंचाध्यायी, २-३५ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org