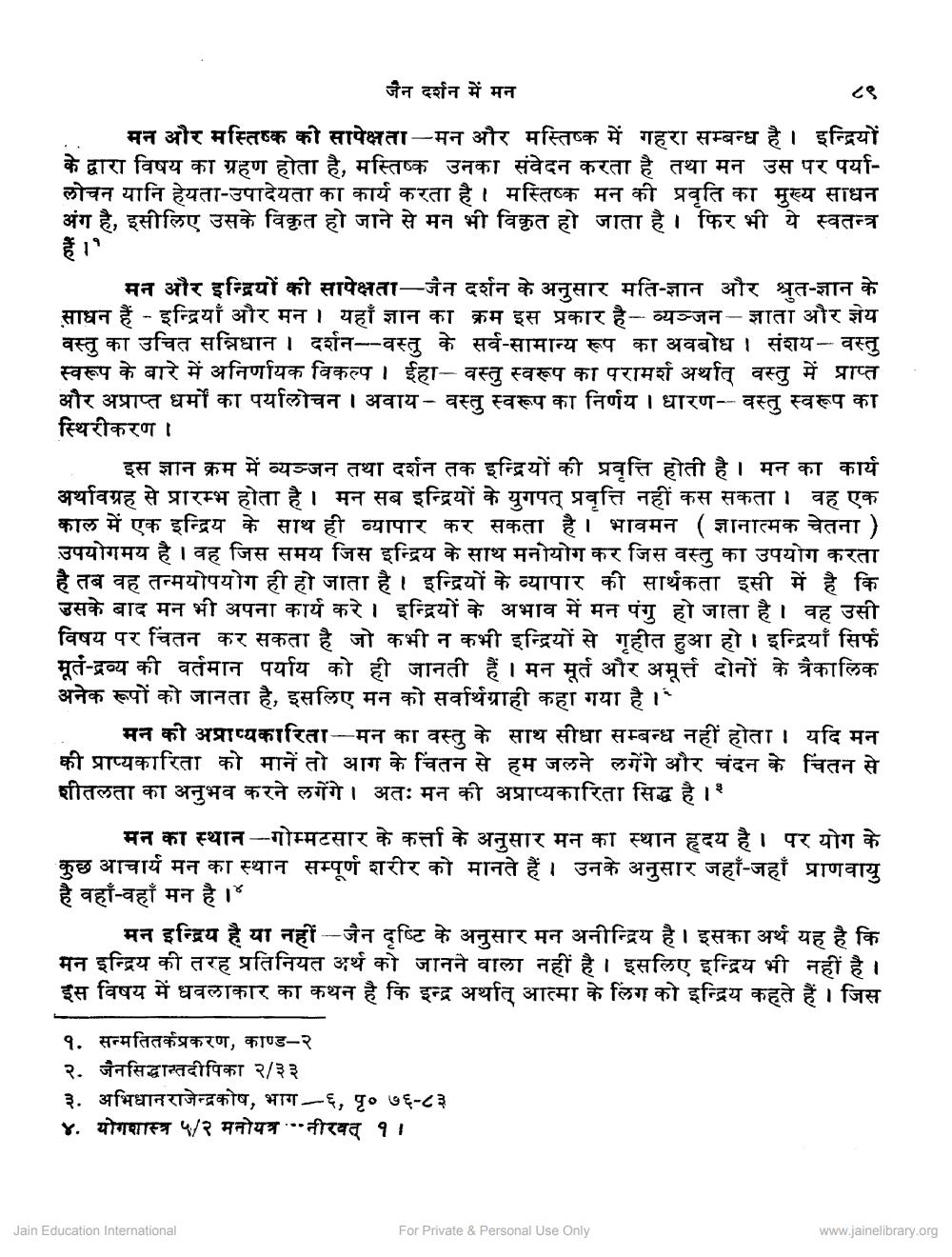________________
जैन दर्शन में मन
मन और मस्तिष्क की सापेक्षता-मन और मस्तिष्क में गहरा सम्बन्ध है। इन्द्रियों के द्वारा विषय का ग्रहण होता है, मस्तिष्क उनका संवेदन करता है तथा मन उस पर पर्यालोचन यानि हेयता-उपादेयता का कार्य करता है। मस्तिष्क मन की प्रवृति का मुख्य साधन अंग है, इसीलिए उसके विकृत हो जाने से मन भी विकृत हो जाता है। फिर भी ये स्वतन्त्र
मन और इन्द्रियों की सापेक्षता-जैन दर्शन के अनुसार मति-ज्ञान और श्रुत-ज्ञान के साधन हैं - इन्द्रियाँ और मन । यहाँ ज्ञान का क्रम इस प्रकार है- व्यञ्जन- ज्ञाता और ज्ञेय वस्तु का उचित सन्निधान । दर्शन--वस्तु के सर्व-सामान्य रूप का अवबोध । संशय- वस्तु स्वरूप के बारे में अनिर्णायक विकल्प । ईहा-वस्त स्वरूप का परामर्श अर्थात वस्तू में प्राप्त और अप्राप्त धर्मों का पर्यालोचन । अवाय- वस्तु स्वरूप का निर्णय । धारण--- वस्तु स्वरूप का स्थिरीकरण ।
इस ज्ञान क्रम में व्यञ्जन तथा दर्शन तक इन्द्रियों की प्रवृत्ति होती है। मन का कार्य अर्थावग्रह से प्रारम्भ होता है। मन सब इन्द्रियों के युगपत् प्रवृत्ति नहीं कस सकता। वह एक काल में एक इन्द्रिय के साथ ही व्यापार कर सकता है। भावमन (ज्ञानात्मक चेतना) उपयोगमय है । वह जिस समय जिस इन्द्रिय के साथ मनोयोग कर जिस वस्तु का उपयोग करता है तब वह तन्मयोपयोग ही हो जाता है। इन्द्रियों के व्यापार की सार्थकता इसी में है कि उसके बाद मन भी अपना कार्य करे। इन्द्रियों के अभाव में मन पंगु हो जाता है। वह उसी विषय पर चिंतन कर सकता है जो कभी न कभी इन्द्रियों से गृहीत हुआ हो। इन्द्रियाँ सिर्फ मूर्त-द्रव्य की वर्तमान पर्याय को ही जानती हैं । मन मूर्त और अमूर्त दोनों के कालिक अनेक रूपों को जानता है, इसलिए मन को सर्वार्थग्राही कहा गया है।
मन की अप्राप्यकारिता-मन का वस्तु के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं होता। यदि मन की प्राप्यकारिता को मानें तो आग के चिंतन से हम जलने लगेंगे और चंदन के चिंतन से शीतलता का अनुभव करने लगेंगे। अतः मन की अप्राप्यकारिता सिद्ध है।
मन का स्थान -गोम्मटसार के कर्ता के अनुसार मन का स्थान हृदय है। पर योग के कुछ आचार्य मन का स्थान सम्पूर्ण शरीर को मानते हैं। उनके अनुसार जहाँ-जहाँ प्राणवायु है वहाँ-वहाँ मन है।
मन इन्द्रिय है या नहीं-जैन दृष्टि के अनुसार मन अनीन्द्रिय है। इसका अर्थ यह है कि मन इन्द्रिय की तरह प्रतिनियत अर्थ को जानने वाला नहीं है। इसलिए इन्द्रिय भी नहीं है। इस विषय में धवलाकार का कथन है कि इन्द्र अर्थात् आत्मा के लिंग को इन्द्रिय कहते हैं। जिस
१. सन्मतितर्कप्रकरण, काण्ड-२ २. जैनसिद्धान्तदीपिका २/३३ ३. अभिधानराजेन्द्रकोष, भाग -६, पृ० ७६-८३ ४. योगशास्त्र ५/२ मनोयत्र "नीरवत् १।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org