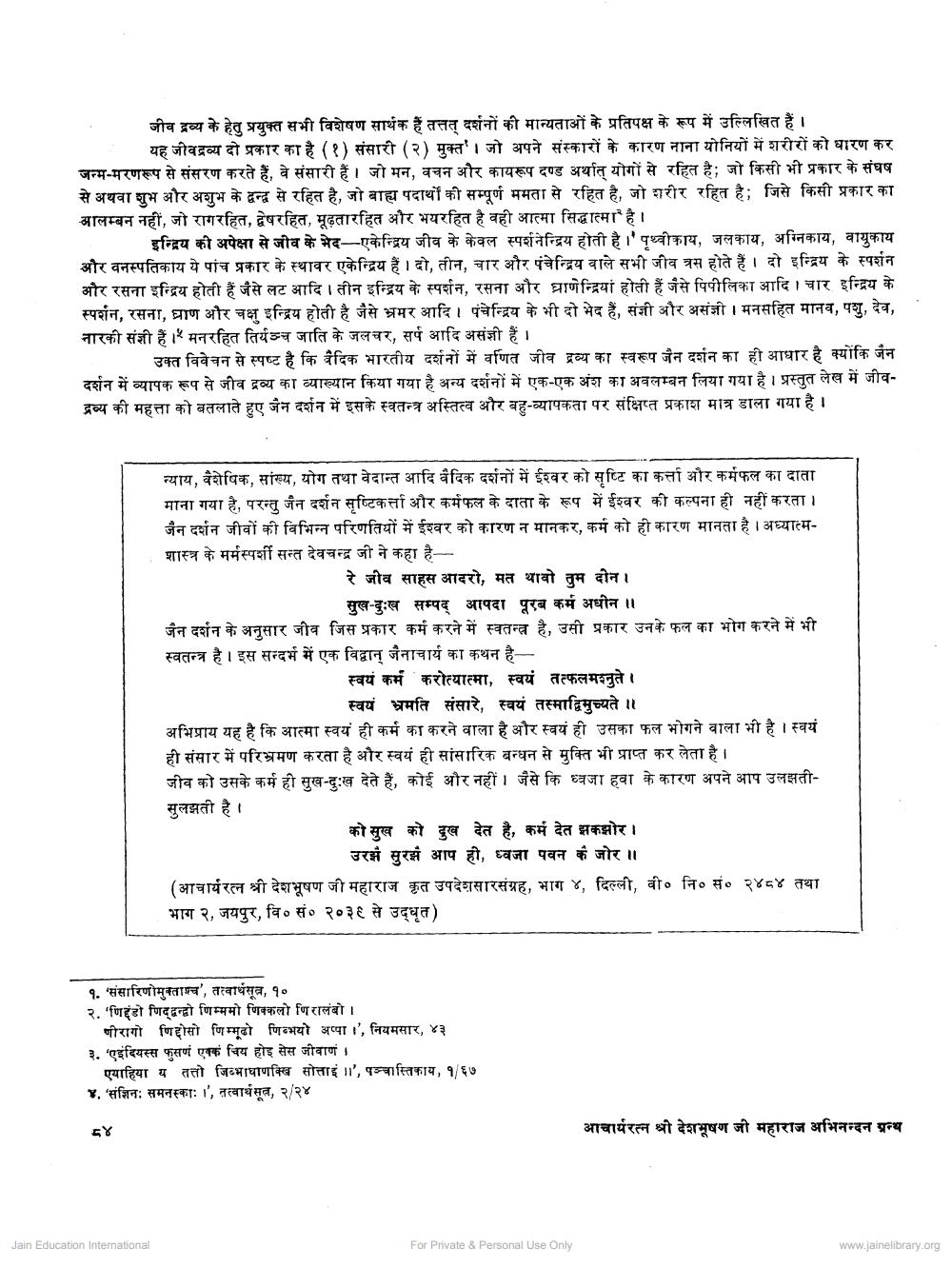________________ जीव द्रव्य के हेतु प्रयुक्त सभी विशेषण सार्थक हैं तत्तत् दर्शनों की मान्यताओं के प्रतिपक्ष के रूप में उल्लिखित हैं। यह जीवद्रव्य दो प्रकार का है (1) संसारी (2) मुक्त। जो अपने संस्कारों के कारण नाना योनियों में शरीरों को धारण कर जन्म-मरणरूप से संसरण करते हैं, वे संसारी हैं। जो मन, वचन और कायरूप दण्ड अर्थात् योगों से रहित है; जो किसी भी प्रकार के संघष से अथवा शुभ और अशुभ के द्वन्द्व से रहित है, जो बाह्य पदार्थों की सम्पूर्ण ममता से रहित है, जो शरीर रहित है; जिसे किसी प्रकार का आलम्बन नहीं, जो रागरहित, द्वेषरहित, मूढ़तारहित और भयरहित है वही आत्मा सिद्धात्मा है। इन्द्रिय की अपेक्षा से जीव के भेद-एकेन्द्रिय जीव के केवल स्पर्शनेन्द्रिय होती है।' पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय ये पांच प्रकार के स्थावर एकेन्द्रिय हैं। दो, तीन, चार और पंचेन्द्रिय वाले सभी जीव वस होते हैं। दो इन्द्रिय के स्पर्शन और रसना इन्द्रिय होती हैं जैसे लट आदि / तीन इन्द्रिय के स्पर्शन, रसना और घ्राणेन्द्रियां होती हैं जैसे पिपीलिका आदि / चार इन्द्रिय के स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इन्द्रिय होती है जैसे भ्रमर आदि। पंचेन्द्रिय के भी दो भेद हैं, संज्ञी और असंज्ञी / मनसहित मानव, पशु, देव, नारकी संज्ञी हैं। मनरहित तिर्यञ्च जाति के जलचर, सर्प आदि असंज्ञी हैं / उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वैदिक भारतीय दर्शनों में वणित जीव द्रव्य का स्वरूप जैन दर्शन का ही आधार है क्योंकि जैन दर्शन में व्यापक रूप से जीव द्रव्य का व्याख्यान किया गया है अन्य दर्शनों में एक-एक अंश का अवलम्बन लिया गया है। प्रस्तुत लेख में जीवद्रव्य की महत्ता को बतलाते हुए जैन दर्शन में इसके स्वतन्त्र अस्तित्व और बहु-व्यापकता पर संक्षिप्त प्रकाश मात्र डाला गया है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग तथा वेदान्त आदि वैदिक दर्शनों में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता और कर्मफल का दाता माना गया है, परन्तु जैन दर्शन सृष्टिकर्ता और कर्मफल के दाता के रूप में ईश्वर की कल्पना ही नहीं करता। जैन दर्शन जीवों की विभिन्न परिणतियों में ईश्वर को कारण न मानकर, कर्म को ही कारण मानता है / अध्यात्मशास्त्र के मर्मस्पर्शी सन्त देवचन्द्र जी ने कहा है रे जीव साहस आदरो, मत थावो तुम दोन। ___ सुख-दुःख सम्पद् आपदा पूरब कर्म अधीन / / जैन दर्शन के अनुसार जीव जिस प्रकार कर्म करने में स्वतन्त्र है, उसी प्रकार उनके फल का भोग करने में भी स्वतन्त्र है। इस सन्दर्भ में एक विद्वान् जैनाचार्य का कथन है स्वयं कर्म करोत्यात्मा, स्वयं तत्फलमश्नुते / स्वयं भ्रमति संसारे, स्वयं तस्माद्विमुच्यते // अभिप्राय यह है कि आत्मा स्वयं ही कर्म का करने वाला है और स्वयं ही उसका फल भोगने वाला भी है / स्वयं ही संसार में परिभ्रमण करता है और स्वयं ही सांसारिक बन्धन से मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। जीव को उसके कर्म ही सुख-दुःख देते हैं, कोई और नहीं। जैसे कि ध्वजा हवा के कारण अपने आप उलझतीसुलझती है। को सुख को दुख देत है, कर्म देत झकझोर / उरझै सुरझै आप हो, ध्वजा पवन के जोर // (आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज कृत उपदेशसारसंग्रह, भाग 4, दिल्ली, वी० नि० सं० 2484 तथा भाग 2, जयपुर, वि० सं० 2036 से उद्धृत) 1. 'संसारिणोमुक्ताश्च', तत्वार्थसूत्र, 10 2. 'णिइंडो णिद्वन्द्वो णिम्ममो णिक्कलो णिरालंबो। णीरागो णिद्दोसो णि म्मूढो णिभयो अप्पा।', नियमसार, 43 3. 'एइंदियस्स फुसणं एक्कं चिय होइ सेस जीवाणं / एयाहिया य तत्तो जिब्भाघाणक्खि सोत्ताई // ', पञ्चास्तिकाय, 1/67 4. 'संज्ञिनः समनस्काः / ', तत्वार्थसूत्र, 2/24 84 आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन अन्य Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org