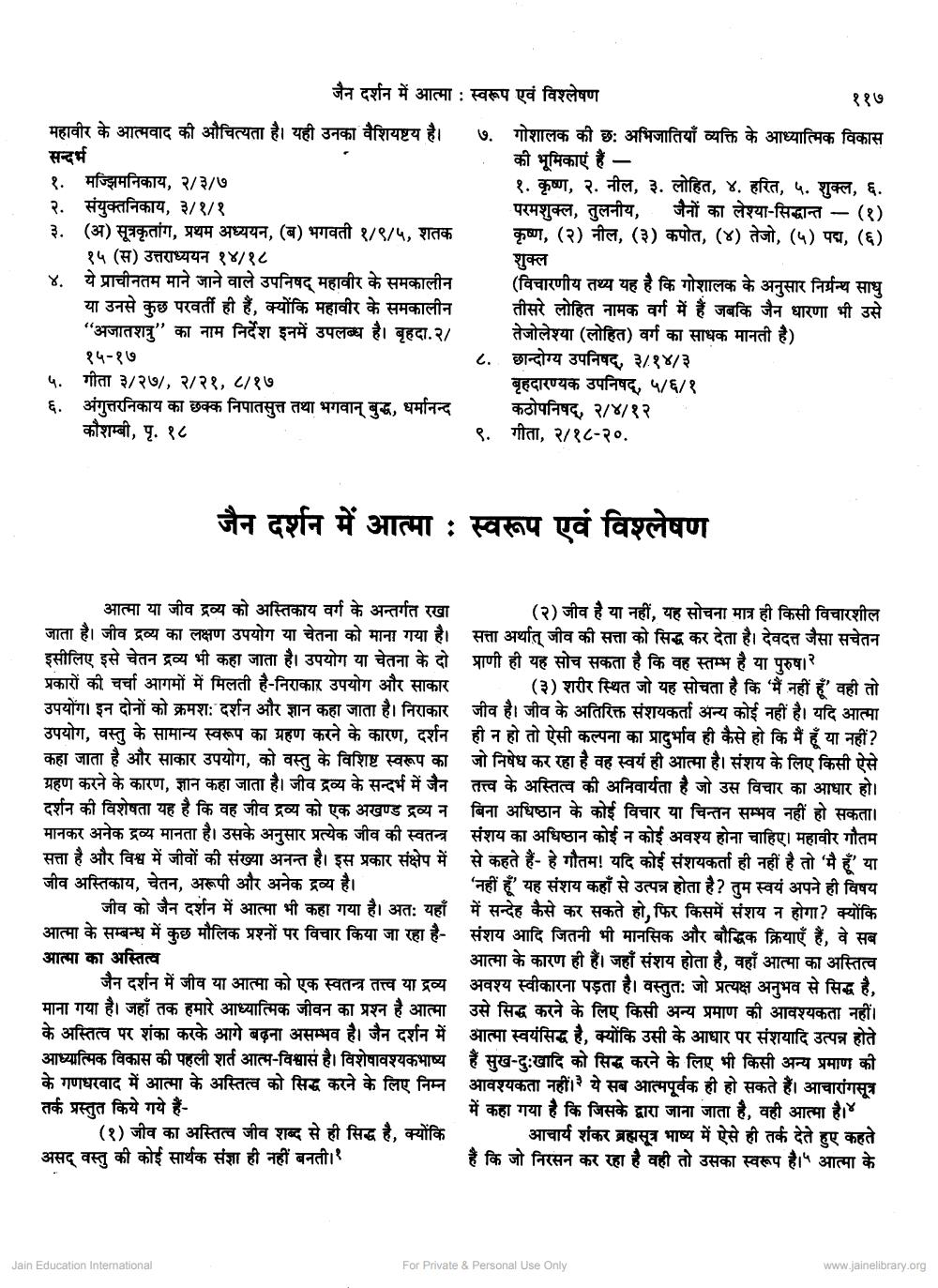________________
जैन दर्शन में आत्मा
महावीर के आत्मवाद की औचित्यता है। यही उनका वैशिष्टय है। सन्दर्भ
१. मज्झिमनिकाय, २/३/७
२. संयुक्तनिकाय, ३/१/१
३. (अ) सूत्रकृतांग, प्रथम अध्ययन, (ब) भगवती १/९/५, शतक १५ (स) उत्तराध्ययन १४ / १८
४. ये प्राचीनतम माने जाने वाले उपनिषद् महावीर के समकालीन या उनसे कुछ परवर्ती ही हैं, क्योंकि महावीर के समकालीन "अजातशत्रु " का नाम निर्देश इनमें उपलब्ध है। बृहदा. २/
१५-१७
८.
गीता ३/२७/ २ /२१, ८/१७
अंगुत्तरनिकाय का छक्क निपातसुत्त तथा भगवान् बुद्ध, धर्मानन्द कौशम्बी, पृ. १८
५.
६.
जैन दर्शन
आत्मा या जीव द्रव्य को अस्तिकाय वर्ग के अन्तर्गत रखा जाता है। जीव द्रव्य का लक्षण उपयोग या चेतना को माना गया है। इसीलिए इसे चेतन द्रव्य भी कहा जाता है। उपयोग या चेतना के दो प्रकारों की चर्चा आगमों में मिलती है-निराकार उपयोग और साकार उपयोग। इन दोनों को क्रमशः दर्शन और ज्ञान कहा जाता है। निराकार उपयोग, वस्तु के सामान्य स्वरूप का ग्रहण करने के कारण, दर्शन कहा जाता है और साकार उपयोग, को वस्तु के विशिष्ट स्वरूप का ग्रहण करने के कारण, ज्ञान कहा जाता है। जीव द्रव्य के सन्दर्भ में जैन दर्शन की विशेषता यह है कि वह जीव द्रव्य को एक अखण्ड द्रव्य न मानकर अनेक द्रव्य मानता है। उसके अनुसार प्रत्येक जीव की स्वतन्त्र सत्ता है और विश्व में जीवों की संख्या अनन्त है। इस प्रकार संक्षेप में जीव अस्तिकाय, चेतन, अरूपी और अनेक द्रव्य है।
जीव को जैन दर्शन में आत्मा भी कहा गया है अतः यहाँ आत्मा के सम्बन्ध में कुछ मौलिक प्रश्नों पर विचार किया जा रहा हैआत्मा का अस्तित्व
जैन दर्शन में जीव या आत्मा को एक स्वतन्त्र तत्त्व या द्रव्य माना गया है। जहाँ तक हमारे आध्यात्मिक जीवन का प्रश्न है आत्मा के अस्तित्व पर शंका करके आगे बढ़ना असम्भव है। जैन दर्शन में आध्यात्मिक विकास की पहली शर्त आत्म-विश्वास है। विशेषावश्यकभाष्य के गणधरवाद में आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए निम्न तर्क प्रस्तुत किये गये हैं
स्वरूप एवं विश्लेषण
११७
७. गोशालक की छः अभिजातियाँ व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास की भूमिकाएं है
2
(१)
१. कृष्ण, २. नील, ३. लोहित, ४. हरित ५ शुक्ल, ६. परमशुक्ल, तुलनीय, जैनों का लेश्या - सिद्धान्त कृष्ण, (२) नील, (३) कपोत, (४) तेजो, (५) पद्म, (६) शुक्ल
(१) जीव का अस्तित्व जीव शब्द से ही सिद्ध है, क्योंकि असद् वस्तु की कोई सार्थक संज्ञा ही नहीं बनती।
Jain Education International
-
(विचारणीय तथ्य यह है कि गोशालक के अनुसार निर्मन्थ साधु तीसरे लोहित नामक वर्ग में हैं जबकि जैन धारणा भी उसे तेजोलेश्या (लोहित) वर्ग का साधक मानती है)
छान्दोग्य उपनिषद्, ३ / १४ / ३ बृहदारण्यक उपनिषद्, ५ / ६ / १ कठोपनिषद् २/४/१२
९. गीता २/१८-२०.
आत्मा : स्वरूप एवं विश्लेषण
-
(२) जीव है या नहीं, यह सोचना मात्र ही किसी विचारशील सत्ता अर्थात् जीव की सत्ता को सिद्ध कर देता है । देवदत्त जैसा सचेतन प्राणी ही यह सोच सकता है कि वह स्तम्भ है या पुरुष
For Private & Personal Use Only
(३) शरीर स्थित जो यह सोचता है कि 'मैं नहीं हूँ' वही तो जीव है। जीव के अतिरिक्त संशयकर्ता अन्य कोई नहीं है। यदि आत्मा ही न हो तो ऐसी कल्पना का प्रादुर्भाव ही कैसे हो कि मैं हूँ या नहीं? जो निषेध कर रहा है वह स्वयं ही आत्मा है। संशय के लिए किसी ऐसे तत्व के अस्तित्व की अनिवार्यता है जो उस विचार का आधार हो । बिना अधिष्ठान के कोई विचार या चिन्तन सम्भव नहीं हो सकता। संशय का अधिष्ठान कोई न कोई अवश्य होना चाहिए। महावीर गौतम से कहते हैं- हे गौतम! यदि कोई संशयकर्ता ही नहीं है तो 'मैं हूँ' या 'नहीं हूँ' यह संशय कहाँ से उत्पन्न होता है? तुम स्वयं अपने ही विषय में सन्देह कैसे कर सकते हो, फिर किसमें संशय न होगा ? क्योंकि संशय आदि जितनी भी मानसिक और बौद्धिक क्रियाएँ हैं, वे सब आत्मा के कारण ही हैं। जहाँ संशय होता है, वहाँ आत्मा का अस्तित्व अवश्य स्वीकारना पड़ता है। वस्तुतः जो प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध है, उसे सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं । आत्मा स्वयंसिद्ध है, क्योंकि उसी के आधार पर संशयादि उत्पन्न होते हैं सुख-दुःखादि को सिद्ध करने के लिए भी किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये सब आत्मपूर्वक ही हो सकते हैं। आचारांगसूत्र में कहा गया है कि जिसके द्वारा जाना जाता है, वही आत्मा है । ४
आचार्य शंकर ब्रह्मसूत्र भाष्य में ऐसे ही तर्क देते हुए कहते हैं कि जो निरसन कर रहा है वही तो उसका स्वरूप है। 4 आत्मा के
www.jainelibrary.org.