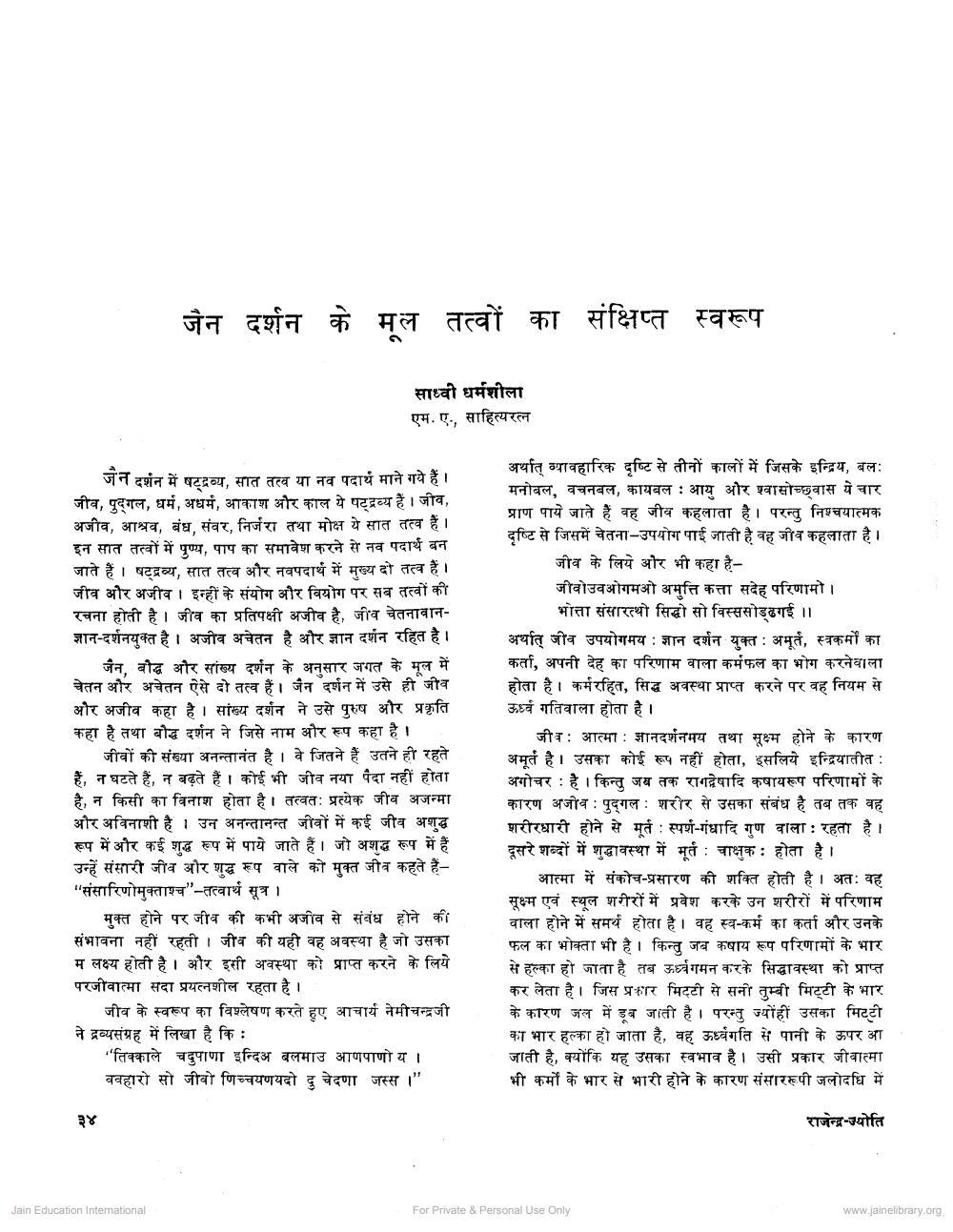________________
जैन दर्शन के
मूल
३४
जैन दर्शन में षट्द्रव्य, सात तत्व या नव पदार्थं माने गये हैं । जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये पद्रव्य हैं । जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा तथा मोक्ष ये सात तत्व हैं। इन सात तत्वों में पुण्य, पाप का समावेश करने से नव पदार्थ बन जाते हैं । षद्रव्य, सात तत्व और नवपदार्थ में मुख्य दो तत्व हैं । जीव और अजीव । इन्हीं के संयोग और वियोग पर सब तत्वों की रचना होती है । जीव का प्रतिपक्षी अजीव है, जीव चेतनावानज्ञान-दर्शनयुक्त है । अजीव अचेतन है और ज्ञान दर्शन रहित है। जैन, बौद्ध और सांख्य दर्शन के अनुसार जगत के मूल में चेतन और अचेतन ऐसे दो तत्व हैं। जैन दर्शन में उसे ही जीव और अजीव कहा है। सांख्य दर्शन ने उसे पुरुष और प्रकृति कहा है तथा बौद्ध दर्शन ने जिसे नाम और रूप कहा है।
जीवों की संख्या अनन्तानंत है । वे जितने हैं उतने ही रहते हैं, न घटते हैं, न बढ़ते हैं। कोई भी जीव नया पैदा नहीं होता है, न किसी का विनाश होता है । तत्वतः प्रत्येक जीव अजन्मा और अविनाशी है । उन अनन्तानन्त जीवों में कई जीव अशुद्ध रूप में और कई शुद्ध रूप में पाये जाते हैं। जो अशुद्ध रूप में हैं उन्हें संसारी जीव और शुद्ध रूप वाले को मुक्त जीव कहते हैं"संसारिणमुक्ताश्च" तत्वार्थ सूत्र
तत्वों का
मुक्त होने पर जीव की कभी अजीव से संबंध होने की संभावना नहीं रहती । जीव की यही वह अवस्था है जो उसका म लक्ष्य होती है । और इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिये परजीवात्मा सदा प्रयत्नशील रहता है ।
Jain Education International
साध्वी धर्मशीला एम. ए. साहित्यरत्न
जीव के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए आचार्य नेमीचन्द्रजी ने द्रव्यसंग्रह में लिखा है कि :
" तिक्काले चदुपाणा इन्दिअ बलमाउ आणपाणो य । बहारी सो जीवो णिच्चरणयो दु चेदणा जस्स ।"
का संक्षिप्त स्वरूप
अर्थात् व्यावहारिक दृष्टि से तीनों कालों में जिसके इन्द्रिय, बलः मनोबल, वचनबल, कायबल : आयु और श्वासोच्छ्वास ये चार प्राण पाये जाते हैं वह जीव कहलाता है । परन्तु निश्चयात्मक दृष्टि से जिसमें चेतना - उपयोग पाई जाती है वह जीव कहलाता है।
जीव के लिये और भी कहा है
जीवोओगमओ अमृति कता सदेह परिणामो भोता संसार सिद्धो सो विसोहगई ॥
अर्थात् जीव उपयोगमय ज्ञान दर्शन युक्त अमूर्त स्वकर्मों का कर्ता, अपनी देह का परिणाम वाला कर्मफल का भोग करनेवाला होता है । कर्मरहित, सिद्ध अवस्था प्राप्त करने पर वह नियम से ऊर्ध्व गतिवाला होता है ।
जीव आत्मा ज्ञानदर्शनमय तथा सूक्ष्म होने के कारण अमूर्त है। उसका कोई रूप नहीं होता, इसलिये इन्द्रियातीत: अगोचर: है । किन्तु जब तक रागद्वेषादि कषायरूप परिणामों के कारण अजीव : पुद्गल शरीर से उसका संबंध है तब तक वह शरीरधारी होने से मूर्त स्पर्श-गंधादि गुण वाला रहता है। दूसरे शब्दों में शुद्धावस्था में मूर्त चाक होता है।
आत्मा में संकोच - प्रसारण की शक्ति होती है। अतः वह सूक्ष्म एवं स्थूल शरीरों में प्रवेश करके उन शरीरों में परिणाम वाला होने में समर्थ होता है। वह स्व-कर्म का कर्ता और उनके फल का भोक्ता भी है। किन्तु जब कषाय रूप परिणामों के भार से हल्का हो जाता है तब ऊर्ध्वगमन करके सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है । जिस प्रकार मिट्टी से सनी तुम्बी मिट्टी के भार के कारण जल में डूब जाती है । परन्तु ज्योंहीं उसका मिट्टी का भार हल्का हो जाता है, वह ऊर्ध्वगति से पानी के ऊपर आ जाती है, क्योंकि यह उसका स्वभाव है । उसी प्रकार जीवात्मा भी कर्मों के भार से भारी होने के कारण संसाररूपी जलोदधि में
राजेन्द्र- ज्योति
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org,