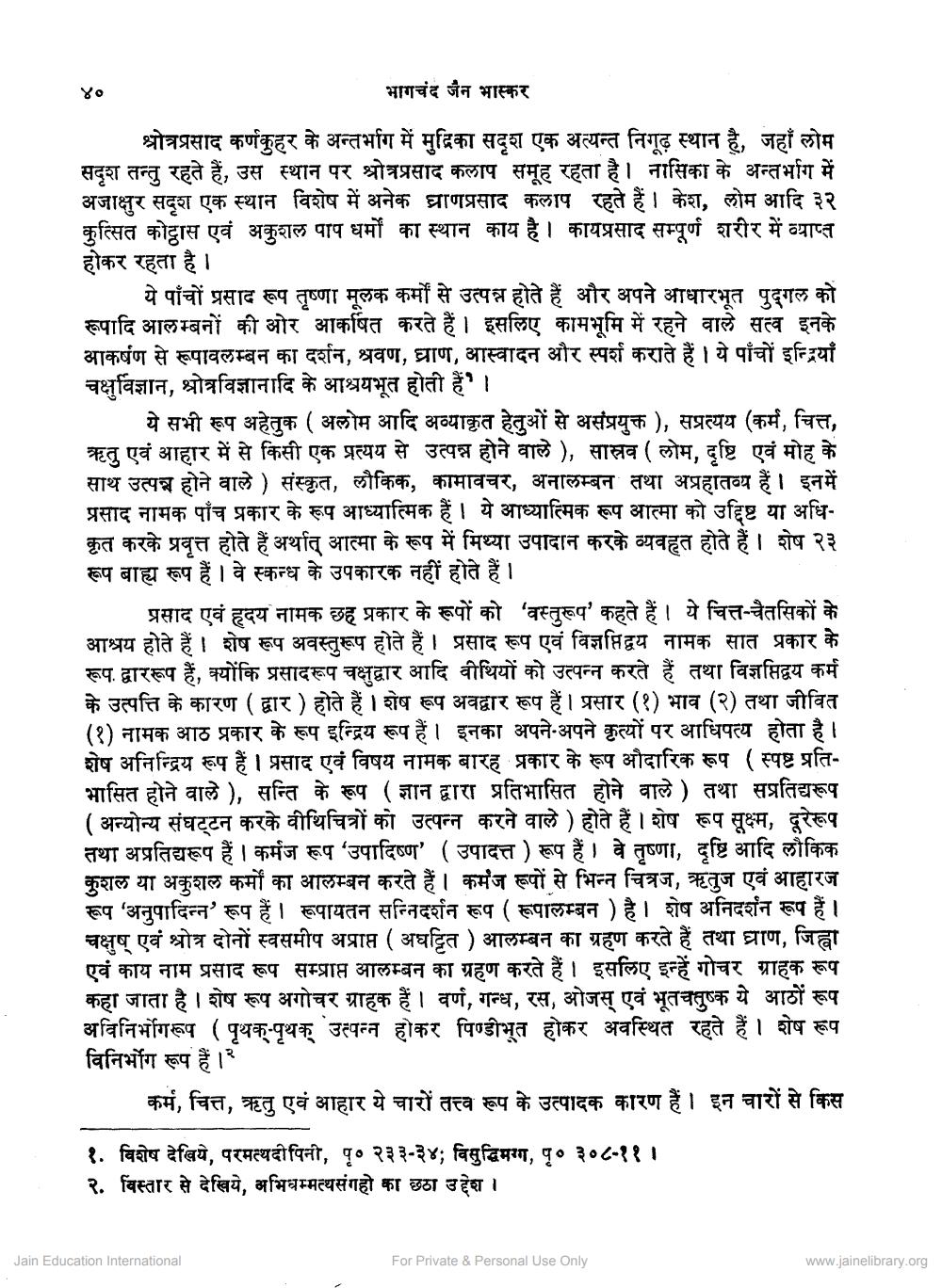________________
भागचंद जैन भास्कर
श्रोत्रप्रसाद कर्णकुहर के अन्तर्भाग में मुद्रिका सदृश एक अत्यन्त निगूढ़ स्थान है, जहाँ लोम सदृश तन्तु रहते हैं, उस स्थान पर श्रोत्रप्रसाद कलाप समूह रहता है । नासिका के अन्तर्भाग में अजाक्षुर सदृश एक स्थान विशेष में अनेक प्राणप्रसाद कलाप रहते हैं । केश, लोम आदि ३२ कुत्सित कोट्ठास एवं अकुशल पाप धर्मों का स्थान काय है । कायप्रसाद सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होकर रहता है ।
४०
ये पाँचों प्रसाद रूप तृष्णा मूलक कर्मों से उत्पन्न होते हैं और अपने आधारभूत पुद्गल को रूपादि आलम्बनों की ओर आकर्षित करते हैं । इसलिए कामभूमि में रहने वाले सत्व इनके आकर्षण से रूपावलम्बन का दर्शन, श्रवण, घ्राण, आस्वादन और स्पर्श कराते हैं । ये पाँचों इन्द्रियाँ चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञानादि के आश्रयभूत होती हैं' ।
ये सभी रूप अहेतुक ( अलोम आदि अव्याकृत हेतुओं से असंप्रयुक्त), सप्रत्यय ( कर्म, चित्त, ऋतु एवं आहार में से किसी एक प्रत्यय से उत्पन्न होने वाले), सास्रव ( लोम, दृष्टि एवं मोह के साथ उत्पन्न होने वाले ) संस्कृत, लौकिक, कामावचर, अनालम्बन तथा अप्रहातव्य हैं । इनमें प्रसाद नामक पाँच प्रकार के रूप आध्यात्मिक हैं । ये आध्यात्मिक रूप आत्मा को उद्दिष्ट या अधिकृत करके प्रवृत्त होते हैं अर्थात् आत्मा के रूप में मिथ्या उपादान करके व्यवहृत होते हैं । शेष २३ रूप बाह्य रूप हैं । वे स्कन्ध के उपकारक नहीं होते हैं ।
प्रसाद एवं हृदय नामक छह प्रकार के रूपों को 'वस्तुरूप' कहते हैं । ये चित्त- चैतसिकों के आश्रय होते हैं । शेष रूप अवस्तुरूप होते हैं । प्रसाद रूप एवं विज्ञप्तिद्वय नामक सात प्रकार के रूप. द्वाररूप हैं, क्योंकि प्रसादरूप चक्षुद्वार आदि वीथियों को उत्पन्न करते हैं तथा विज्ञप्तिद्वय कर्म के उत्पत्ति के कारण ( द्वार ) होते हैं । शेष रूप अवद्वार रूप हैं । प्रसार (१) भाव (२) तथा जीवित (१) नामक आठ प्रकार के रूप इन्द्रिय रूप हैं । इनका अपने-अपने कृत्यों पर आधिपत्य होता है । शेष अनिन्द्रिय रूप हैं । प्रसाद एवं विषय नामक बारह प्रकार के रूप औदारिक रूप ( स्पष्ट प्रतिभासित होने वाले ), सन्ति के रूप ( ज्ञान द्वारा प्रतिभासित होने वाले ) तथा सप्रतिद्यरूप ( अन्योन्य संघट्टन करके वीथिचित्रों को उत्पन्न करने वाले ) होते हैं । शेष रूप सूक्ष्म, दूरेरूप तथा अप्रतिरूप हैं । कर्मज रूप 'उपादिष्ण' ( उपादत्त ) रूप हैं। वे तृष्णा, दृष्टि आदि लौकिक कुशल या अकुशल कर्मों का आलम्बन करते हैं । कर्मज रूपों से भिन्न चित्रज, ऋतुज एवं आहारज रूप 'अनुपादिन्न' रूप हैं । रूपायतन सन्निदर्शन रूप ( रूपालम्बन ) है । शेष अनिदर्शन रूप हैं । चक्षुष् एवं श्रोत्र दोनों स्वसमीप अप्राप्त ( अघट्टित ) आलम्बन का ग्रहण करते हैं तथा घ्राण, जिह्वा एवं काय नाम प्रसाद रूप सम्प्राप्त आलम्बन का ग्रहण करते हैं । इसलिए इन्हें गोचर ग्राहक रूप कहा जाता है । शेष रूप अगोचर ग्राहक हैं । वर्ण, गन्ध, रस, ओजस् एवं भूतचतुष्क ये आठों रूप अविनिर्भोगरूप ( पृथक्-पृथक् उत्पन्न होकर पिण्डीभूत होकर अवस्थित रहते हैं । शेष रूप विनिर्भोग रूप हैं ।
कर्म, चित्त, ऋतु एवं आहार ये चारों तत्त्व रूप के उत्पादक कारण हैं । इन चारों से किस
१. विशेष देखिये, परमत्थदीपिनी, पृ० २३३-३४; विसुद्धिमग्ग, पृ० ३०८-११ । २. विस्तार से देखिये, अभिवम्मत्थसंगहो का छठा उद्देश ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org