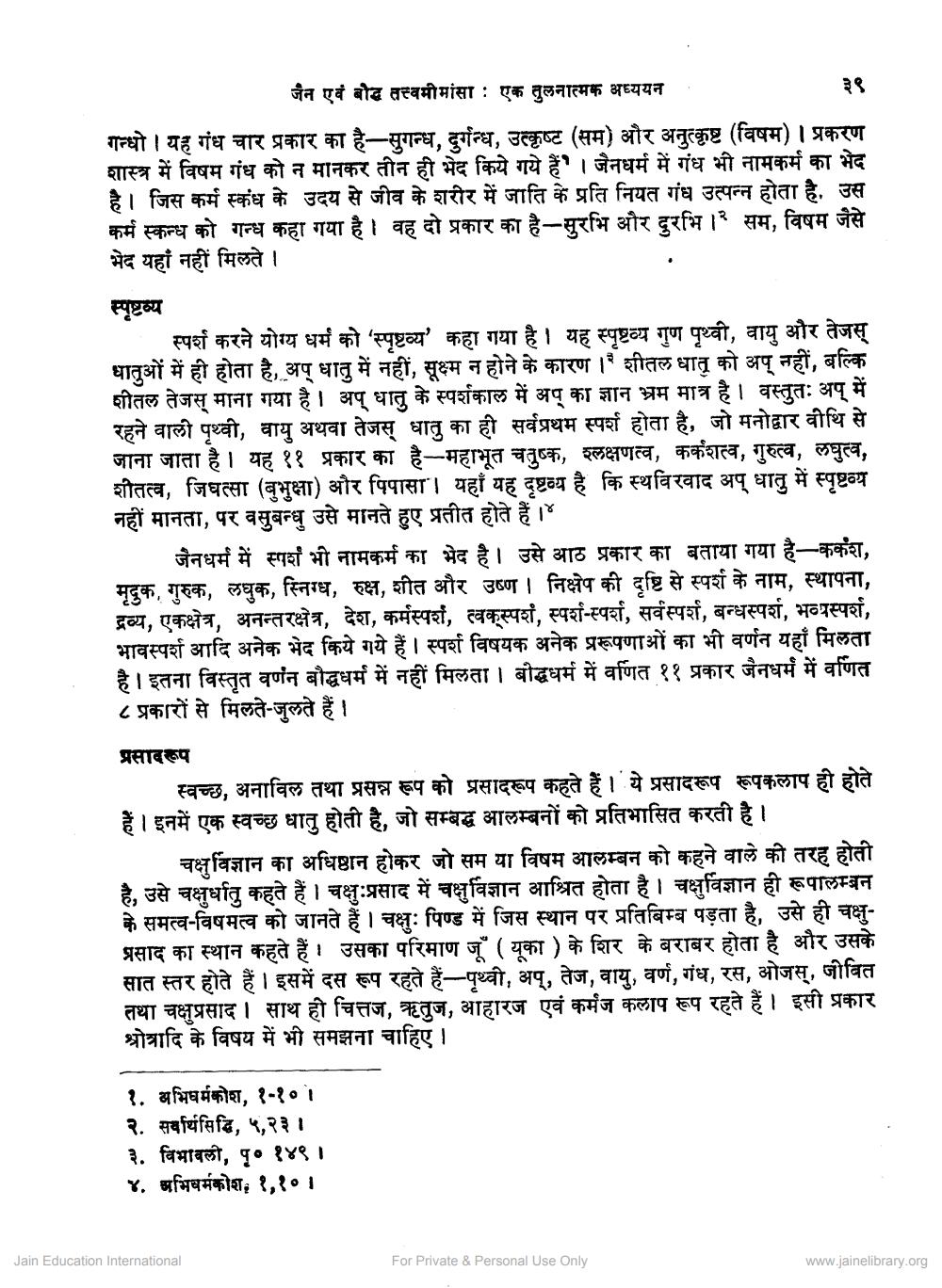________________
जैन एवं बौद्ध तत्त्वमीमांसा : एक तुलनात्मक अध्ययन
३९ गन्धो । यह गंध चार प्रकार का है-सुगन्ध, दुर्गन्ध, उत्कृष्ट (सम) और अनुत्कृष्ट (विषम)। प्रकरण शास्त्र में विषम गंध को न मानकर तीन ही भेद किये गये हैं । जैनधर्म में गंध भी नामकर्म का भेद है। जिस कर्म स्कंध के उदय से जीव के शरीर में जाति के प्रति नियत गंध उत्पन्न होता है, उस कर्म स्कन्ध को गन्ध कहा गया है। वह दो प्रकार का है-सुरभि और दुरभि । सम, विषम जैसे भेद यहां नहीं मिलते।
स्पृष्टव्य
स्पर्श करने योग्य धर्म को 'स्पृष्टव्य' कहा गया है। यह स्पृष्टव्य गुण पृथ्वी, वायु और तेजस् धातुओं में ही होता है, अप् धातु में नहीं, सूक्ष्म न होने के कारण । शीतल धातु को अप् नहीं, बल्कि शीतल तेजस् माना गया है। अप् धातु के स्पर्शकाल में अप का ज्ञान भ्रम मात्र है। वस्तुतः अप् में रहने वाली पृथ्वी, वायु अथवा तेजस् धातु का ही सर्वप्रथम स्पर्श होता है, जो मनोद्वार वीथि से जाना जाता है। यह ११ प्रकार का है-महाभूत चतुष्क, श्लक्षणत्व, कर्कशत्व, गुरुत्व, लघुत्व, शीतत्व, जिघत्सा (बुभुक्षा) और पिपासा। यहाँ यह दृष्टव्य है कि स्थविरवाद अप् धातु में स्पृष्टव्य नहीं मानता, पर वसुबन्धु उसे मानते हुए प्रतीत होते हैं ।
जैनधर्म में स्पर्श भी नामकर्म का भेद है। उसे आठ प्रकार का बताया गया है-कर्कश, मृदुक, गुरुक, लघुक, स्निग्ध, रुक्ष, शीत और उष्ण । निक्षेप की दृष्टि से स्पर्श के नाम, स्थापना, द्रव्य, एकक्षेत्र, अनन्तरक्षेत्र, देश, कर्मस्पर्श, त्वक्स्पर्श, स्पर्श-स्पर्श, सर्वस्पर्श, बन्धस्पर्श, भव्यस्पर्श, भावस्पर्श आदि अनेक भेद किये गये हैं। स्पर्श विषयक अनेक प्ररूपणाओं का भी वर्णन यहाँ मिलता है। इतना विस्तृत वर्णन बौद्धधर्म में नहीं मिलता। बौद्धधर्म में वर्णित ११ प्रकार जैनधर्म में वर्णित ८ प्रकारों से मिलते-जुलते हैं।।
प्रसादरूप
स्वच्छ, अनाविल तथा प्रसन्न रूप को प्रसादरूप कहते हैं। ये प्रसादरूप रूपकलाप ही होते हैं। इनमें एक स्वच्छ धातु होती है, जो सम्बद्ध आलम्बनों को प्रतिभासित करती है।
__ चक्षुर्विज्ञान का अधिष्ठान होकर जो सम या विषम आलम्बन को कहने वाले की तरह होती है, उसे चक्षुर्धातु कहते हैं । चक्षुःप्रसाद में चक्षुर्विज्ञान आश्रित होता है। चक्षुर्विज्ञान ही रूपालम्बन के समत्व-विषमत्व को जानते हैं । चक्षुः पिण्ड में जिस स्थान पर प्रतिबिम्ब पड़ता है, उसे ही चक्षुप्रसाद का स्थान कहते हैं। उसका परिमाण जूं (यूका ) के शिर के बराबर होता है और उसके सात स्तर होते हैं। इसमें दस रूप रहते हैं-पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वर्ण, गंध, रस, ओजस्, जीवित तथा चक्षुप्रसाद । साथ ही चित्तज, ऋतुज, आहारज एवं कर्मज कलाप रूप रहते हैं। इसी प्रकार श्रोत्रादि के विषय में भी समझना चाहिए।
१. अभिधर्मकोश, १-१०॥ २. सर्वार्थसिद्धि, ५,२३ । ३. विभावली, पृ. १४९ । ४. अभिधर्मकोश, १,१०।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org