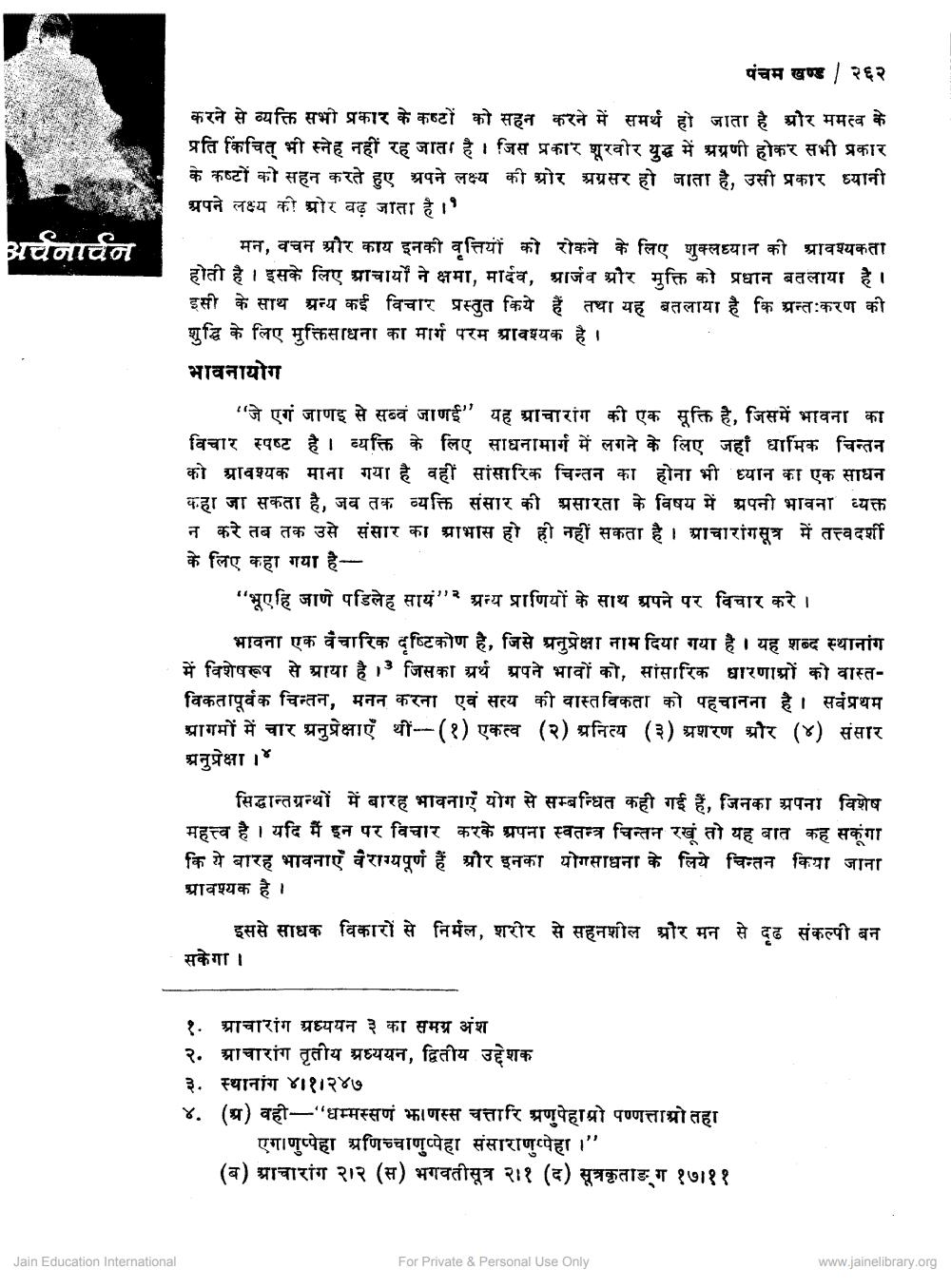________________
अर्चनार्चन
Jain Education International
पंचम खण्ड / २६२
जाता है और ममत्व के अग्रणी होकर सभी प्रकार
करने से व्यक्ति सभी प्रकार के कष्टों को सहन करने में समर्थ हो प्रति किंचित् भी स्नेह नहीं रह जाता है। जिस प्रकार शूरवीर युद्ध में के कष्टों को सहन करते हुए अपने लक्ष्य की घोर अग्रसर हो जाता है, उसी प्रकार ध्यानी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है ।"
'
मन, वचन और काय इनकी वृत्तियों को रोकने के लिए शुक्लध्यान की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्राचायों ने क्षमा, मार्दव, आर्जव और मुक्ति को प्रधान बतलाया है। इसी के साथ अन्य कई विचार प्रस्तुत किये हैं तथा यह बतलाया है कि ग्रन्तःकरण की शुद्धि के लिए मुक्तिसाधना का मार्ग परम प्रावश्यक है। भावनायोग
सूक्ति है, जिसमें भावना का लिए जहाँ धार्मिक चिन्तन
ध्यान का एक साधन
"जे एवं जाणद से सब्वं जागई" यह प्राचारांग की एक विचार स्पष्ट है व्यक्ति के लिए साधनामार्ग में लगने के को आवश्यक माना गया है वहीं सांसारिक चिन्तन का होना भी कहा जा सकता है, जब तक व्यक्ति संसार की असारता के विषय में अपनी भावना व्यक्त न करे तब तक उसे संसार का आभास हो ही नहीं सकता है । आचारांगसूत्र में तत्त्वदर्शी के लिए कहा गया है
२
"भूएहि जाणे पडिलेह सायं ग्रन्य प्राणियों के साथ अपने पर विचार करे ।
भावना एक वैचारिक दृष्टिकोण है, जिसे धनुप्रेक्षा नाम दिया गया है। यह शब्द स्थानांग में विशेषरूप से आया है। जिसका अर्थ अपने भावों को, सांसारिक धारणानों को वास्तकी वास्तविकता को पहचानना है । सर्वप्रथम (२) श्रनित्य ( ३ ) अशरण और (४) संसार
विकतापूर्वक चिन्तन, मनन करना एवं सत्य श्रागमों में चार अनुप्रेक्षाएँ थीं - ( १ ) एकत्व धनुप्रेक्षा ।*
महत्त्व है। यदि मैं इन पर विचार कि ये बारह भावनाएं वैराग्यपूर्ण हैं श्रावश्यक है ।
सिद्धान्तग्रन्थों में बारह भावनाएं योग से सम्बन्धित कही गई हैं, जिनका अपना विशेष करके अपना स्वतस्त्र चिन्तन रखूं तो यह बात कह सकूंगा और इनका योगसाधना के लिये चिन्तन किया जाना
इससे साधक विकारों से निर्मल शरीर से सहनशील और मन से दृढ संकल्पी बन
"
सकेगा ।
१. आचारांग अध्ययन ३ का समग्र अंश
२. प्राचारांग तृतीय अध्ययन, द्वितीय उद्देशक
३. स्थानांग ४।१।२४७
४. (अ) वही "धम्मस्सणं झाणस्स चत्तारि प्रणुपेहाम्रो पण्णत्ताम्रो तहा
एमाणुप्पेहा प्रणिच्चाणुप्पेहा संसाराणुत्हा ।"
(ब) प्राचारांग २२ (स) भगवतीसूत्र २1१ (द) सूत्रकृताङग १७।११
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org