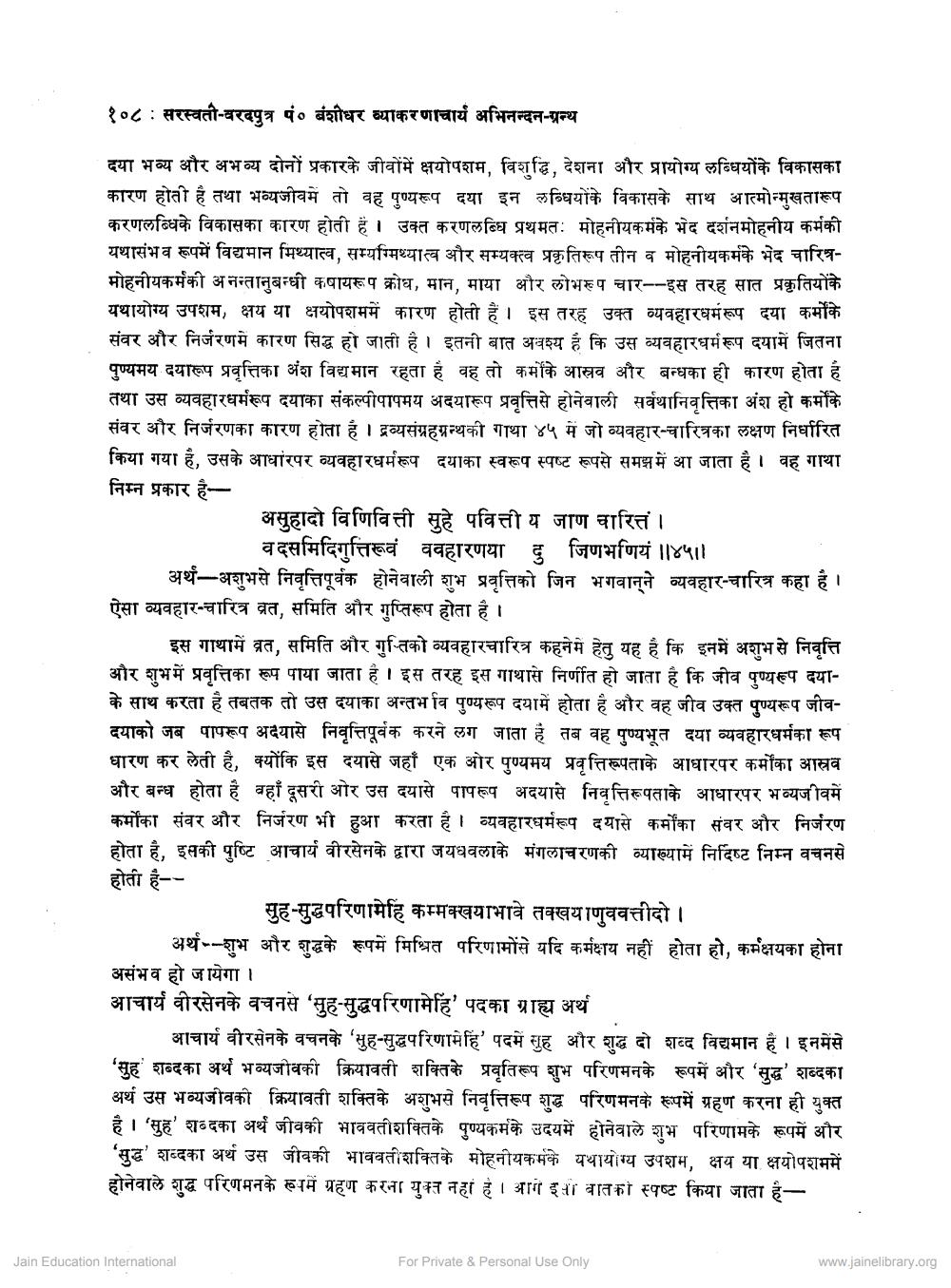________________
१०८ : सरस्वती वरदपुत्र पं० बंशीधर व्याकरणाचार्यं अभिनन्दन ग्रन्थ
दया भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीवों में क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य लब्धियोंके विकासका कारण होती है तथा भव्यजीव में तो वह पुण्यरूप दया इन लब्धियोंके विकासके साथ आत्मोन्मुखतारूप करणलब्धि विकासका कारण होती है । उक्त करणलब्धि प्रथमतः मोहनीयकर्मके भेद दर्शनमोहनीय कर्मकी यथासंभव रूपमें विद्यमान मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृतिरूप तीन व मोहनीयकर्मके भेद चारित्रमोहनीय कर्म की अनन्तानुबन्धी कषायरूप क्रोध, मान, माया और लोभरूप चार -- इस तरह सात प्रकृतियोंके यथायोग्य उपशम, क्षय या क्षयोपशममें कारण होती हैं। इस तरह उक्त व्यवहारधर्मरूप दया कर्मोंके संवर और निर्जरण में कारण सिद्ध हो जाती है। इतनी बात अवश्य है कि उस व्यवहारधर्मरूप दयामें जितना पुण्यमय दयारूप प्रवृत्तिका अंश विद्यमान रहता है वह तो कर्मोंके आस्रव और बन्धका ही कारण होता है तथा उस व्यवहारधर्मरूप दयाका संकल्पीपापमय अदयारूप प्रवृत्ति से होनेवाली सर्वथानिवृत्तिका अंश हो कर्मोंके संवर और निर्जरणका कारण होता है । द्रव्यसंग्रह ग्रन्थकी गाथा ४५ में जो व्यवहार चारित्रका लक्षण निर्धारित किया गया है, उसके आधारपर व्यवहारधर्मरूप दयाका स्वरूप स्पष्ट रूपसे समझ में आ जाता है । वह गाथा निम्न प्रकार है
असुहादो विणिवित्ती सुहे पवित्तीय जाण चारितं । वदसमिदिगुत्तिरूवं ववहारणया दु जिणभणियं ॥ ४५ ॥ |
अर्थ - अशुभसे निवृत्तिपूर्वक होनेवाली शुभ प्रवृत्तिको जिन भगवान्ने व्यवहार चारित्र कहा है । ऐसा व्यवहार चारित्र व्रत, समिति और गुप्तिरूप होता है ।
इस गाथामें व्रत, समिति और गुतिको व्यवहारचारित्र कहने में हेतु यह है कि इनमें अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्तिका रूप पाया जाता है । इस तरह इस गाथासे निर्णीत हो जाता है कि जीव पुण्यरूप दयाके साथ करता है तबतक तो उस दयाका अन्तर्भाव पुण्यरूप दयामें होता है और वह जीव उक्त पुण्यरूप जीवदयाको जब पापरूप अदयासे निवृत्तिपूर्वक करने लग जाता है तब वह पुण्यभूत दया व्यवहारधर्मका रूप धारण कर लेती है, क्योंकि इस दयासे जहाँ एक ओर पुण्यमय प्रवृत्तिरूपताके आधारपर कर्मोंका आस्रव और बन्ध होता है वहाँ दूसरी ओर उस दयासे पापरूप अदयासे निवृत्तिरूपताके आधारपर भव्यजीवमें कर्मोंका संवर और निर्जरण भी हुआ करता है । व्यवहारधर्मरूप दयासे कर्मोंका संवर और निर्जरण होता है, इसकी पुष्टि आचार्य वीरसेनके द्वारा जयधवलाके मंगलाचरणकी व्याख्यामें निर्दिष्ट निम्न वचन से होती है-
सुह-सुद्धपरिणामेहि कम्मक्खयाभावे तक्खयाणुववत्तीदो ।
अर्थ -- शुभ और शुद्धके रूपमें मिश्रित परिणामों से यदि कर्मक्षय नहीं होता हो, कर्मक्षयका होना असंभव हो जायेगा ।
आचार्य वीरसेनके वचनसे 'सुह- सुद्धपरिणामेहि' पदका ग्राह्य अर्थ
शब्द विद्यमान हैं । इनमें से रूपमें और 'सुद्ध' शब्दका
आचार्य वीरसेनके वचनके 'सुह-सुद्धपरिणामेहि' पदमें सुह और शुद्ध दो 'सुह' शब्द का अर्थ भव्यजीवकी क्रियावती शक्तिके प्रवृतिरूप शुभ परिणमनके अर्थ उस भव्यजीवकी क्रियावती शक्तिके अशुभसे निवृत्तिरूप शुद्ध परिणमनके रूपमें ग्रहण करना ही युक्त है । 'सुह' शब्दका अर्थं जीवकी भाववतीशक्तिके पुण्यकर्मके उदयमें होनेवाले शुभ परिणामके रूपमें और 'सुद्ध' शब्दका अर्थ उस जीवकी भाववतीशक्तिके मोहनीयकर्मके यथायोग्य उपशम, क्षय या क्षयोपशममें होनेवाले शुद्ध परिणमनके रूपमें ग्रहण करना युक्त नहीं है। आगे इसी बात को स्पष्ट किया जाता है
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org