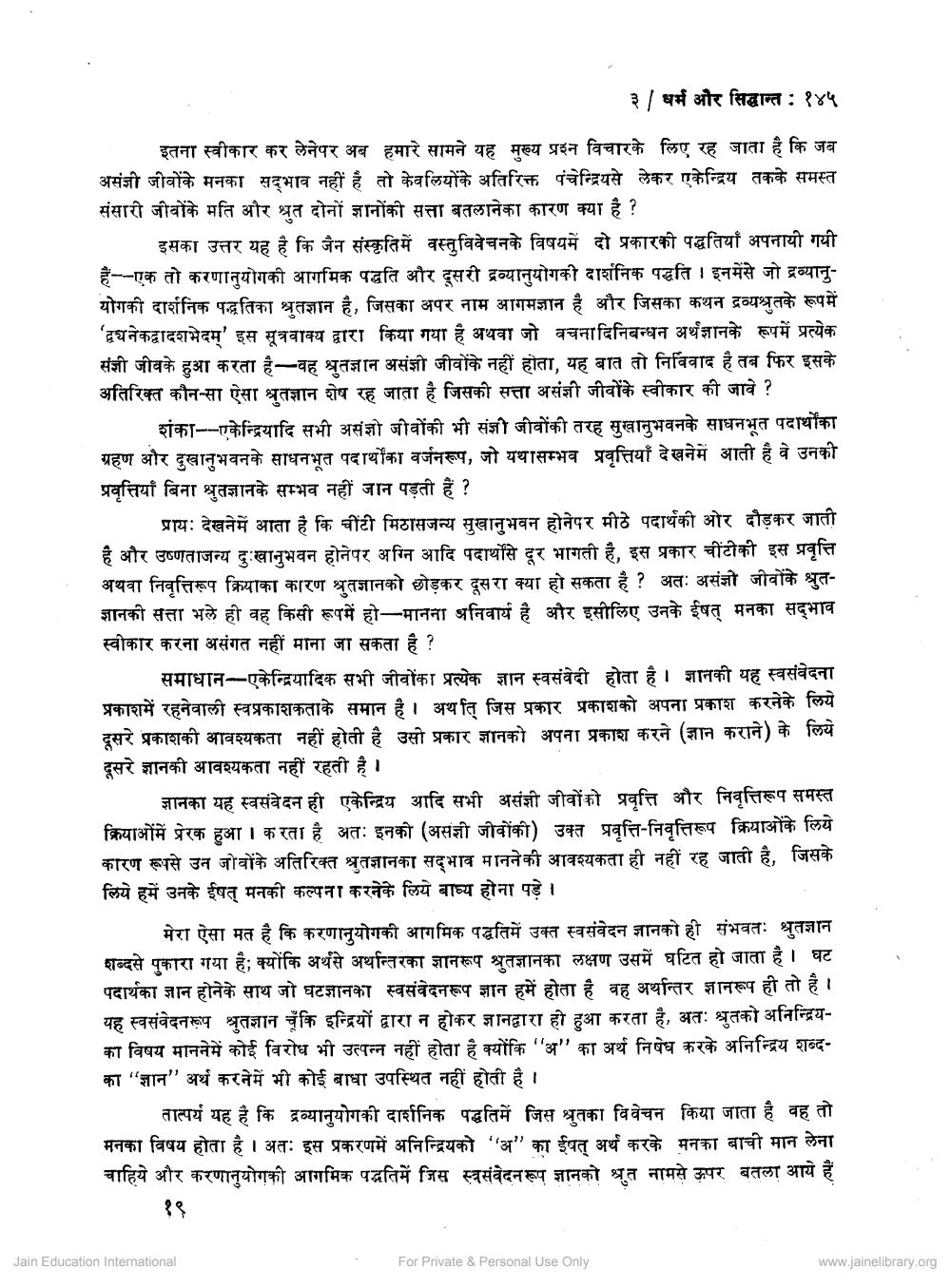________________
३/ धर्म और सिद्धान्त : १४५
इतना स्वीकार कर लेनेपर अब हमारे सामने यह मुख्य प्रश्न विचारके लिए रह जाता है कि जब असंज्ञी जीवोंके मनका सद्भाव नहीं है तो केवलियोंके अतिरिक्त पंचेन्द्रियसे लेकर एकेन्द्रिय तकके समस्त संसारी जीवोंके मति और श्रुत दोनों ज्ञानोंकी सत्ता बतलानेका कारण क्या है ?
____ इसका उत्तर यह है कि जैन संस्कृतिमें वस्तुविवेचनके विषयमें दो प्रकारकी पद्धतियाँ अपनायी गयी हैं--एक तो करणानुयोगकी आगमिक पद्धति और दूसरी द्रव्यानुयोगको दार्शनिक पद्धति । इनमेंसे जो द्रव्यानुयोगकी दार्शनिक पद्धतिका श्रतज्ञान है, जिसका अपर नाम आगमज्ञान है और जिसका कथन द्रव्यश्रुतके रूप में 'द्वधनेकद्वादशभेदम्' इस सूत्रवाक्य द्वारा किया गया है अथवा जो वचनादिनिबन्धन अर्थज्ञानके रूपमें प्रत्येक संज्ञी जीवके हुआ करता है-वह श्रुतज्ञान असंज्ञी जीवोंके नहीं होता, यह बात तो निर्विवाद है तब फिर इसके अतिरिक्त कौन-सा ऐसा श्रतज्ञान शेष रह जाता है जिसकी सत्ता असंज्ञी जीवोंके स्वीकार की जावे ?
__ शंका--एकेन्द्रियादि सभी असंज्ञो जीवोंकी भी संज्ञी जीवोंकी तरह सुखानुभवनके साधनभूत पदार्थोंका ग्रहण और दुखानुभवनके साधनभूत पदार्थोंका वर्जनरूप, जो यथासम्भव प्रवृत्तियाँ देखने में आती है वे उनकी प्रवृत्तियाँ बिना श्रुतज्ञानके सम्भव नहीं जान पड़ती हैं ?
प्रायः देखने में आता है कि चींटी मिठासजन्य सुखानुभवन होनेपर मीठे पदार्थकी ओर दौड़कर जाती है और उष्णताजन्य दुःखानुभवन होनेपर अग्नि आदि पदार्थोसे दूर भागती है, इस प्रकार चींटीकी इस प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिरूप क्रियाका कारण श्रुतज्ञानको छोड़कर दूसरा क्या हो सकता है ? अतः असंज्ञो जीवोंके श्रुतज्ञानकी सत्ता भले ही वह किसी रूपमें हो-मानना अनिवार्य है और इसीलिए उनके ईषत् मनका सद्भाव स्वीकार करना असंगत नहीं माना जा सकता है ?
समाधान-एकेन्द्रियादिक सभी जीवोंका प्रत्येक ज्ञान स्वसंवेदी होता है। ज्ञानकी यह स्वसंवेदना प्रकाशमें रहनेवाली स्वप्रकाशकताके समान है। अर्थात् जिस प्रकार प्रकाशको अपना प्रकाश करनेके लिये दूसरे प्रकाशकी आवश्यकता नहीं होती है उसी प्रकार ज्ञानको अपना प्रकाश करने (ज्ञान कराने) के लिये दूसरे ज्ञानकी आवश्यकता नहीं रहती है।
ज्ञानका यह स्वसंवेदन ही एकेन्द्रिय आदि सभी असंज्ञी जीवोंको प्रवृत्ति और निवृत्तिरूप समस्त क्रियाओंमें प्रेरक हुआ । क रता है अतः इनको (असज्ञी जीवोंकी) उक्त प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप क्रियाओंके लिये कारण रूपसे उन जोवोंके अतिरिक्त श्रुतज्ञानका सद्भाव मानने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है, जिसके लिये हमें उनके ईषत् मनकी कल्पना करनेके लिये बाध्य होना पड़े।
मेरा ऐसा मत है कि करणानुयोगकी आगमिक पद्धतिमें उक्त स्वसंवेदन ज्ञानको ही संभवतः श्रुतज्ञान शब्दसे पुकारा गया है; क्योंकि अर्थसे अर्थान्तरका ज्ञानरूप श्रुतज्ञानका लक्षण उसमें घटित हो जाता है। घट पदार्थका ज्ञान होनेके साथ जो घटज्ञानका स्वसंवेदनरूप ज्ञान हमें होता है वह अर्थान्तर ज्ञानरूप ही तो है। यह स्वसंवेदनरूप श्रुतज्ञान चूँकि इन्द्रियों द्वारा न होकर ज्ञानद्वारा ही हुआ करता है, अतः श्रुतको अनिन्द्रियका विषय मानने में कोई विरोध भी उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि "अ" का अर्थ निषेध करके अनिन्द्रिय शब्दका "ज्ञान" अर्थ करने में भी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है।
तात्पर्य यह है कि द्रव्यानुयोगकी दार्शनिक पद्धतिमें जिस श्रुतका विवेचन किया जाता है वह तो मनका विषय होता है । अतः इस प्रकरणमें अनिन्द्रियको "अ" का ईषत अर्थ करके मनका बाची मान लेना चाहिये और करणानुयोगकी आगमिक पद्धतिमें जिस स्वसंवेदनरूप ज्ञानको श्रुत नामसे ऊपर बतला आये हैं
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org