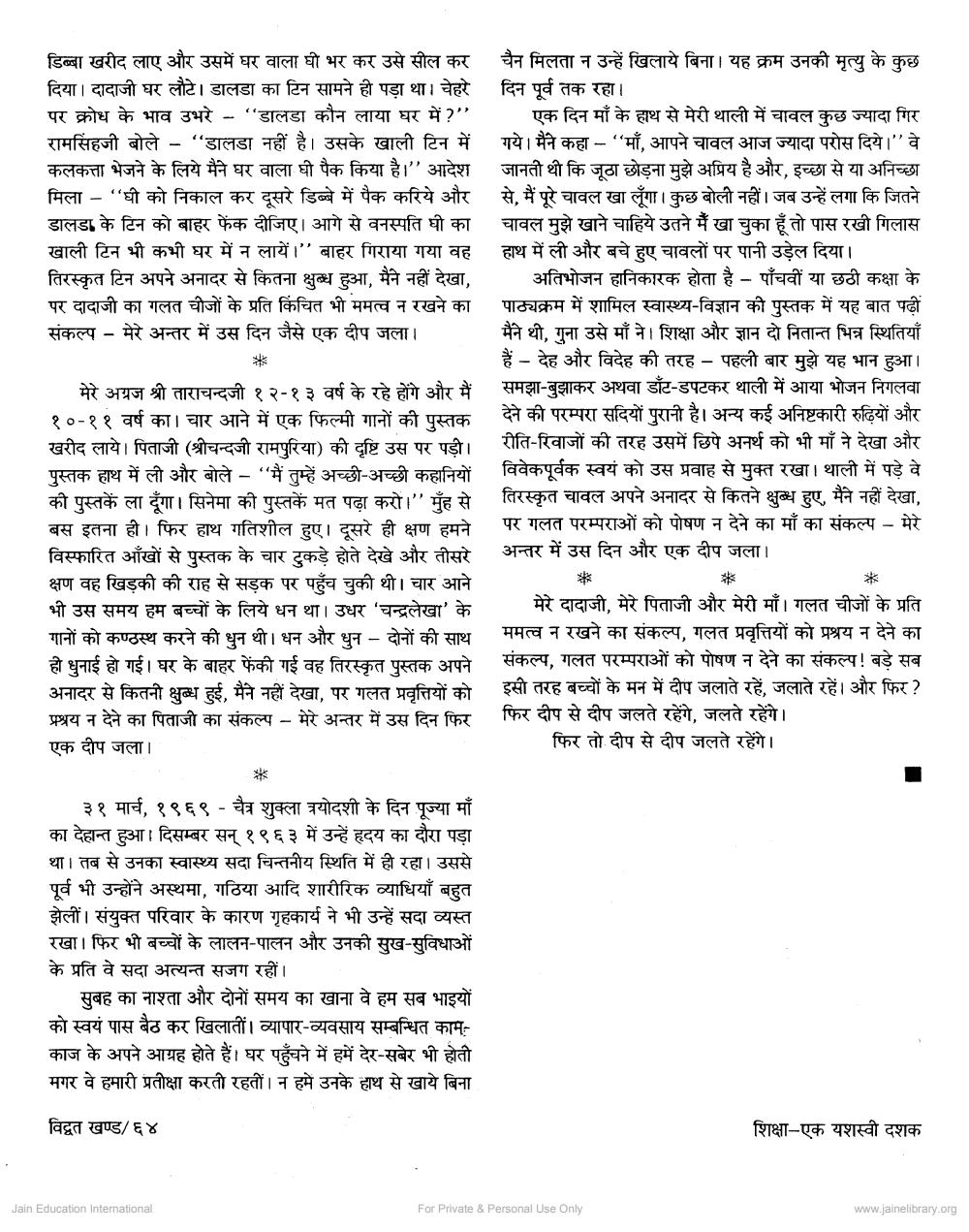________________ डिब्बा खरीद लाए और उसमें घर वाला घी भर कर उसे सील कर चैन मिलता न उन्हें खिलाये बिना। यह क्रम उनकी मृत्यु के कुछ दिया। दादाजी घर लौटे। डालडा का टिन सामने ही पड़ा था। चेहरे दिन पूर्व तक रहा। पर क्रोध के भाव उभरे - "डालडा कौन लाया घर में?" एक दिन माँ के हाथ से मेरी थाली में चावल कुछ ज्यादा गिर रामसिंहजी बोले - "डालडा नहीं है। उसके खाली टिन में गये। मैंने कहा - "माँ, आपने चावल आज ज्यादा परोस दिये। वे कलकत्ता भेजने के लिये मैने घर वाला घी पैक किया है।" आदेश जानती थी कि जूठा छोड़ना मुझे अप्रिय है और, इच्छा से या अनिच्छा मिला - “घी को निकाल कर दूसरे डिब्बे में पैक करिये और से, मैं पूरे चावल खा लूँगा। कुछ बोली नहीं। जब उन्हें लगा कि जितने डालडा के टिन को बाहर फेंक दीजिए। आगे से वनस्पति घी का चावल मुझे खाने चाहिये उतने मैं खा चुका हूँ तो पास रखी गिलास खाली टिन भी कभी घर में न लायें।'' बाहर गिराया गया वह हाथ में ली और बचे हुए चावलों पर पानी उड़ेल दिया। तिरस्कृत टिन अपने अनादर से कितना क्षुब्ध हुआ, मैने नहीं देखा, अतिभोजन हानिकारक होता है - पाँचवीं या छठी कक्षा के पर दादाजी का गलत चीजों के प्रति किंचित भी ममत्व न रखने का पाठ्यक्रम में शामिल स्वास्थ्य-विज्ञान की पुस्तक में यह बात पढ़ी संकल्प - मेरे अन्तर में उस दिन जैसे एक दीप जला। मैने थी, गुना उसे माँ ने। शिक्षा और ज्ञान दो नितान्त भिन्न स्थितियाँ हैं - देह और विदेह की तरह - पहली बार मुझे यह भान हुआ। मेरे अग्रज श्री ताराचन्दजी 12-13 वर्ष के रहे होंगे और मैं समझा-बुझाकर अथवा डाँट-डपटकर थाली में आया भोजन निगलवा 10-11 वर्ष का। चार आने में एक फिल्मी गानों की पुस्तक / देने की परम्परा सदियों पुरानी है। अन्य कई अनिष्टकारी रुढ़ियों और खरीद लाये। पिताजी (श्रीचन्दजी रामपुरिया) की दृष्टि उस पर पड़ी। रीति-रिवाजों की तरह उसमें छिपे अनर्थ को भी माँ ने देखा और पुस्तक हाथ में ली और बोले - “मैं तुम्हें अच्छी-अच्छी कहानियों विवेकपूर्वक स्वयं को उस प्रवाह से मुक्त रखा। थाली में पड़े वे की पुस्तकें ला दूँगा। सिनेमा की पुस्तकें मत पढा करो।" मुँह से तिरस्कृत चावल अपने अनादर से कितने क्षुब्ध हुए, मैने नहीं देखा, बस इतना ही। फिर हाथ गतिशील हए। दूसरे ही क्षण हमने पर गलत परम्पराओं को पोषण न देने का माँ का संकल्प - मेरे विस्फारित आँखों से पुस्तक के चार टकडे होते देखे और तीसरे अन्तर में उस दिन और एक दीप जला। क्षण वह खिड़की की राह से सड़क पर पहुँच चुकी थी। चार आने भी उस समय हम बच्चों के लिये धन था। उधर 'चन्द्रलेखा' के मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मेरी माँ। गलत चीजों के प्रति गानों को कण्ठस्थ करने की धुन थी। धन और धुन - दोनों की साथ। ममत्व न रखने का संकल्प, गलत प्रवृत्तियों को प्रश्रय न देने का अनादर से कितनी क्षुब्ध हई, मैने नहीं देखा, पर गलत प्रवृत्तियों को प्रश्रय न देने का पिताजी का संकल्प - मेरे अन्तर में उस दिन फिर एक दीप जला। इसी तरह बच्चों के मन में दीप जलाते रहें, जलाते रहें। और फिर? फिर दीप से दीप जलते रहेंगे, जलते रहेंगे। फिर तो दीप से दीप जलते रहेंगे। 31 मार्च, 1969 - चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन पूज्या माँ का देहान्त हुआ। दिसम्बर सन् 1963 में उन्हें हृदय का दौरा पड़ा था। तब से उनका स्वास्थ्य सदा चिन्तनीय स्थिति में ही रहा। उससे पूर्व भी उन्होंने अस्थमा, गठिया आदि शारीरिक व्याधियाँ बहुत झेली। संयुक्त परिवार के कारण गृहकार्य ने भी उन्हें सदा व्यस्त रखा। फिर भी बच्चों के लालन-पालन और उनकी सुख-सुविधाओं के प्रति वे सदा अत्यन्त सजग रहीं। सुबह का नाश्ता और दोनों समय का खाना वे हम सब भाइयों को स्वयं पास बैठ कर खिलाती। व्यापार-व्यवसाय सम्बन्धित कामकाज के अपने आग्रह होते हैं। घर पहुँचने में हमें देर-सबेर भी होती मगर वे हमारी प्रतीक्षा करती रहतीं। न हमें उनके हाथ से खाये बिना विद्वत खण्ड/६४ शिक्षा-एक यशस्वी दशक Jain Education International For Private & Personal Use Only www.jainelibrary.org