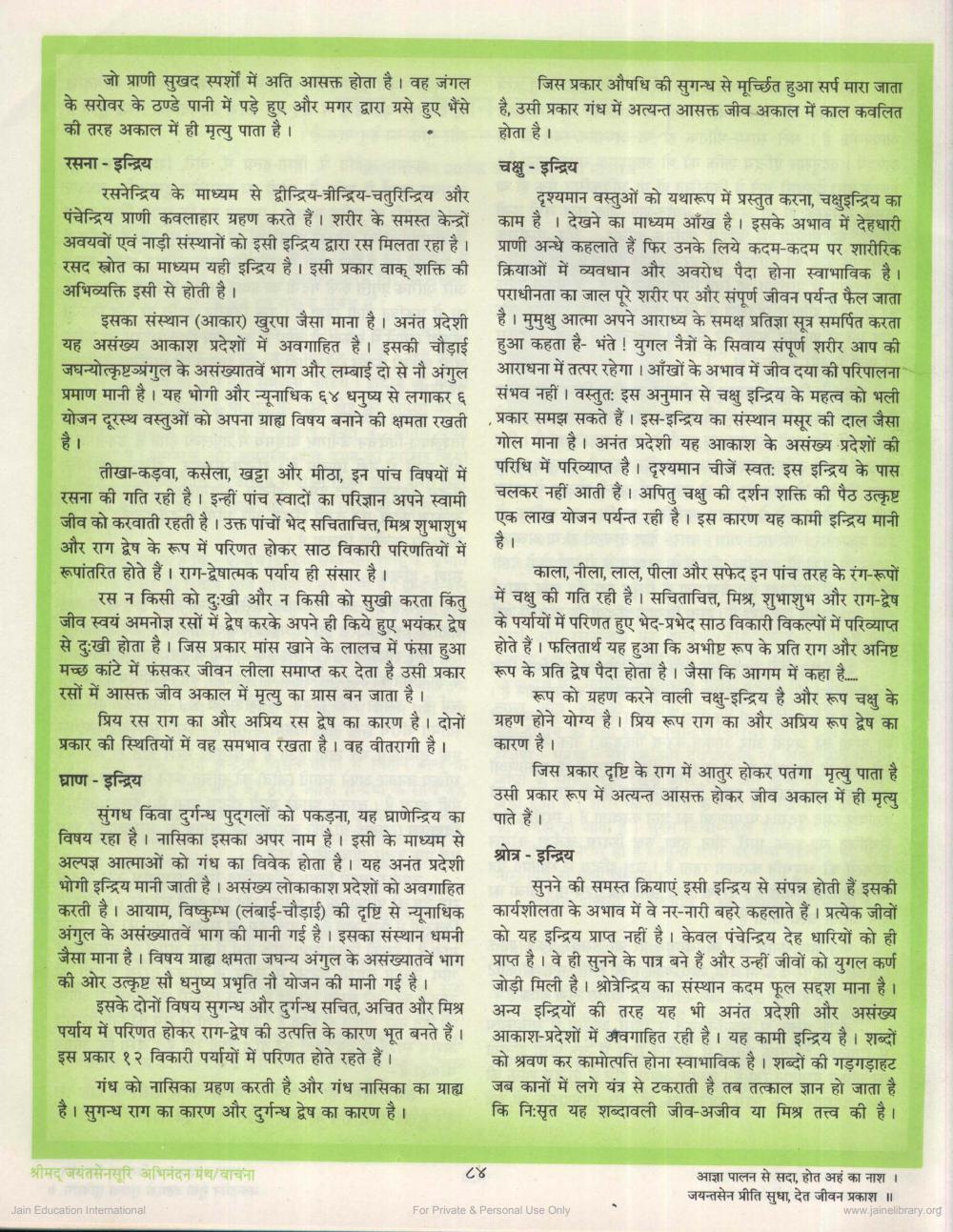________________
जो प्राणी सुखद स्पर्शों में अति आसक्त होता है। वह जंगल जिस प्रकार औषधि की सुगन्ध से मूर्च्छित हुआ सर्प मारा जाता के सरोवर के ठण्डे पानी में पड़े हुए और मगर द्वारा ग्रसे हुए भैंसे है, उसी प्रकार गंध में अत्यन्त आसक्त जीव अकाल में काल कवलित की तरह अकाल में ही मृत्यु पाता है।
होता है। रसना- इन्द्रिय
चक्षु- इन्द्रिय रसनेन्द्रिय के माध्यम से द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय और दृश्यमान वस्तुओं को यथारूप में प्रस्तुत करना, चक्षुइन्द्रिय का पंचेन्द्रिय प्राणी कवलाहार ग्रहण करते हैं। शरीर के समस्त केन्द्रों काम है । देखने का माध्यम आँख है। इसके अभाव में देहधारी
अवयवों एवं नाड़ी संस्थानों को इसी इन्द्रिय द्वारा रस मिलता रहा है। प्राणी अन्धे कहलाते हैं फिर उनके लिये कदम-कदम पर शारीरिक रसद स्त्रोत का माध्यम यही इन्द्रिय है। इसी प्रकार वाक् शक्ति की क्रियाओं में व्यवधान और अवरोध पैदा होना स्वाभाविक है। अभिव्यक्ति इसी से होती है।
पराधीनता का जाल पूरे शरीर पर और संपूर्ण जीवन पर्यन्त फैल जाता इसका संस्थान (आकार) खरपा जैसा माना है। अनंत प्रदेशी है। मुमुक्षु आत्मा अपने आराध्य के समक्ष प्रतिज्ञा सूत्र समर्पित करता यह असंख्य आकाश प्रदेशों में अवगाहित है। इसकी चौडाई हुआ कहता है- भंते ! युगल नेत्रों के सिवाय संपूर्ण शरीर आप की जघन्योत्कष्टअंगल के असंख्यातवें भाग और लम्बाई दो से नौ अंगल आराधना में तत्पर रहेगा। आँखों के अभाव में जीव दया की परिपालना प्रमाण मानी है। यह भोगी और न्यूनाधिक ६४ धनुष्य से लगाकर ६
संभव नहीं । वस्तुत: इस अनुमान से चक्षु इन्द्रिय के महत्व को भली योजन दूरस्थ वस्तुओं को अपना ग्राह्य विषय बनाने की क्षमता रखती , प्रकार समझ सकते हैं। इस-इन्द्रिय का संस्थान मसूर की दाल जैसा
गोल माना है। अनंत प्रदेशी यह आकाश के असंख्य प्रदेशों की तीखा-कड़वा, कसेला, खट्टा और मीठा, इन पांच विषयों में
परिधि में परिव्याप्त है। दृश्यमान चीजें स्वत: इस इन्द्रिय के पास रसना की गति रही है। इन्हीं पांच स्वादों का परिज्ञान अपने स्वामी
चलकर नहीं आती हैं। अपितु चक्षु की दर्शन शक्ति की पैठ उत्कृष्ट जीव को करवाती रहती है । उक्त पांचों भेद सचिताचित्त, मिश्र शुभाशुभ
एक लाख योजन पर्यन्त रही है। इस कारण यह कामी इन्द्रिय मानी और राग द्वेष के रूप में परिणत होकर साठ विकारी परिणतियों में रूपांतरित होते हैं। राग-द्वेषात्मक पर्याय ही संसार है।
काला, नीला, लाल, पीला और सफेद इन पांच तरह के रंग-रूपों रस न किसी को दःखी और न किसी को सखी करता किंत में चक्षु की गति रही है। सचिताचित्त, मिश्र, शुभाशुभ और राग-द्वेष जीव स्वयं अमनोज्ञ रसों में द्वेष करके अपने ही किये हुए भयंकर द्वेष के पर्यायों में परिणत हुए भेद-प्रभेद साठ विकारी विकल्पों में परिव्याप्त से दुःखी होता है। जिस प्रकार मांस खाने के लालच में फंसा हुआ होते हैं । फलितार्थ यह हुआ कि अभीष्ट रूप के प्रति राग और अनिष्ट मच्छ कांटे में फंसकर जीवन लीला समाप्त कर देता है उसी प्रकार रूप के प्रति द्वेष पैदा होता है। जैसा कि आगम में कहा है... रसों में आसक्त जीव अकाल में मृत्यु का ग्रास बन जाता है।
रूप को ग्रहण करने वाली चक्ष-इन्द्रिय है और रूप चक्षु के प्रिय रस राग का और अप्रिय रस द्वेष का कारण है। दोनों ग्रहण होने योग्य है। प्रिय रूप राग का और अप्रिय रूप द्वेष का प्रकार की स्थितियों में वह समभाव रखता है। वह वीतरागी है। कारण है।
या जिस प्रकार दृष्टि के राग में आतुर होकर पतंगा मृत्यु पाता है। घ्राण- इन्द्रिय
उसी प्रकार रूप में अत्यन्त आसक्त होकर जीव अकाल में ही मृत्यु सुंगध किंवा दुर्गन्ध पुद्गलों को पकड़ना, यह घ्राणेन्द्रिय का पाते हैं। विषय रहा है। नासिका इसका अपर नाम है। इसी के माध्यम से अल्पज्ञ आत्माओं को गंध का विवेक होता है। यह अनंत प्रदेशी
श्रोत्र - इन्द्रिय भोगी इन्द्रिय मानी जाती है। असंख्य लोकाकाश प्रदेशों को अवगाहित सुनने की समस्त क्रियाएं इसी इन्द्रिय से संपन्न होती हैं इसकी करती है। आयाम, विष्कुम्भ (लंबाई-चौड़ाई) की दृष्टि से न्यूनाधिक कार्यशीलता के अभाव में वे नर-नारी बहरे कहलाते हैं। प्रत्येक जीवों अंगुल के असंख्यातवें भाग की मानी गई है। इसका संस्थान धमनी को यह इन्द्रिय प्राप्त नहीं है। केवल पंचेन्द्रिय देह धारियों को ही जैसा माना है। विषय ग्राह्य क्षमता जघन्य अंगुल के असंख्यातवें भाग प्राप्त है। वे ही सुनने के पात्र बने हैं और उन्हीं जीवों को युगल कर्ण की ओर उत्कृष्ट सौ धनुष्य प्रभृति नौ योजन की मानी गई है। जोड़ी मिली है। श्रोत्रेन्द्रिय का संस्थान कदम फूल सद्दश माना है।
इसके दोनों विषय सुगन्ध और दुर्गन्ध सचित, अचित और मिश्र अन्य इन्द्रियों की तरह यह भी अनंत प्रदेशी और असंख्य पर्याय में परिणत होकर राग-द्वेष की उत्पत्ति के कारण भूत बनते हैं। आकाश-प्रदेशों में अवगाहित रही है। यह कामी इन्द्रिय है। शब्दों इस प्रकार १२ विकारी पर्यायों में परिणत होते रहते हैं।
को श्रवण कर कामोत्पत्ति होना स्वाभाविक है। शब्दों की गड़गड़ाहट गंध को नासिका ग्रहण करती है और गंध नासिका का ग्राह्य । जब कानों में लगे यंत्र से टकराती है तब तत्काल ज्ञान हो जाता है। है। सुगन्ध राग का कारण और दर्गन्ध द्वेष का कारण है। कि नि:सृत यह शब्दावली जीव-अजीव या मिश्र तत्त्व की है।
श्रीमद् जयंतसेनसूरि अभिनंदन ग्रंथ/वाचना
आज्ञा पालन से सदा, होत अहं का नाश । जयन्तसेन प्रीति सुधा, देत जीवन प्रकाश ॥
www.jainelibrary.org
Jain Education International
For Private & Personal Use Only