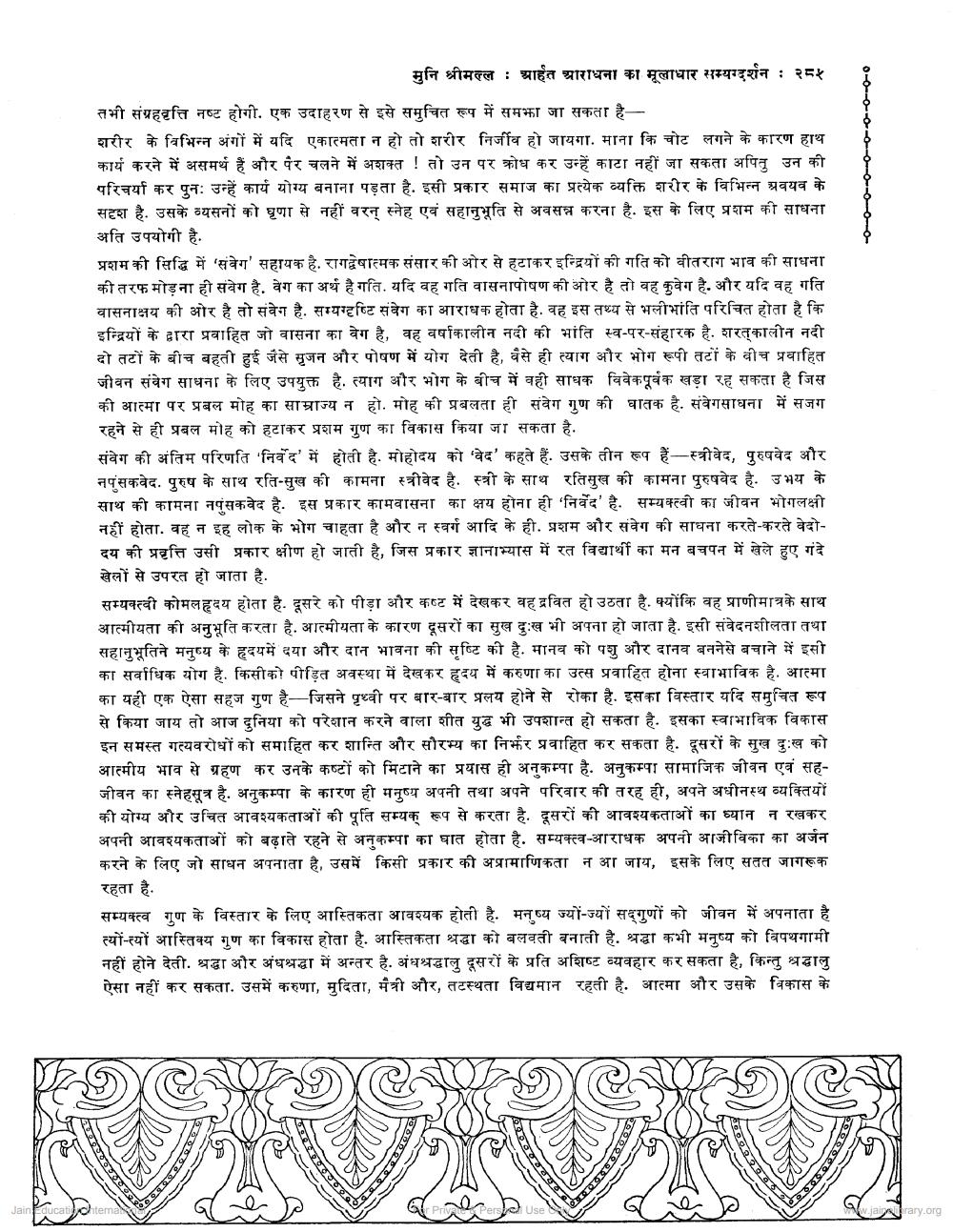________________
-0-0-0--0-0--0--0--0--0-0
मुनि श्रीमल्ल : आर्हत आराधना का मूलाधार सम्यग्दर्शन : २८५ तभी संग्रहवृत्ति नष्ट होगी. एक उदाहरण से इसे समुचित रूप में समझा जा सकता हैशरीर के विभिन्न अंगों में यदि एकात्मता न हो तो शरीर निर्जीव हो जायगा. माना कि चोट लगने के कारण हाथ कार्य करने में असमर्थ हैं और पैर चलने में अशक्त ! तो उन पर क्रोध कर उन्हें काटा नहीं जा सकता अपितु उन की परिचर्या कर पुन: उन्हें कार्य योग्य बनाना पड़ता है. इसी प्रकार समाज का प्रत्येक व्यक्ति शरीर के विभिन्न अवयव के सदृश है. उसके व्यसनों को घृणा से नहीं वरन् स्नेह एवं सहानुभूति से अवसन्न करना है. इस के लिए प्रशम की साधना अति उपयोगी है. प्रशम की सिद्धि में 'संवेग' सहायक है. रागद्वेषात्मक संसार की ओर से हटाकर इन्द्रियों की गति को वीतराग भाव की साधना की तरफ मोड़ना ही संवेग है. वेग का अर्थ है गति. यदि वह गति वासनापोषण की ओर है तो वह कुवेग है. और यदि वह गति वासनाक्षय की ओर है तो संवेग है. सम्यग्दृष्टि संवेग का आराधक होता है. वह इस तथ्य से भलीभांति परिचित होता है कि इन्द्रियों के द्वारा प्रवाहित जो वासना का वेग है, वह वर्षाकालीन नदी की भांति स्व-पर-संहारक है. शरत्कालीन नदी दो तटों के बीच बहती हुई जैसे सृजन और पोषण में योग देती है, वैसे ही त्याग और भोग रूपी तटों के बीच प्रवाहित जीवन संवेग साधना के लिए उपयुक्त है. त्याग और भोग के बीच में वही साधक विवेकपूर्वक खड़ा रह सकता है जिस की आत्मा पर प्रबल मोह का साम्राज्य न हो. मोह की प्रबलता ही संवेग गुण की घातक है. संवेगसाधना में सजग रहने से ही प्रबल मोह को हटाकर प्रशम गुण का विकास किया जा सकता है. संवेग की अंतिम परिणति 'निर्वेद' में होती है. मोहोदय को 'वेद' कहते हैं. उसके तीन रूप हैं-स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद. पुरुष के साथ रति-सुख की कामना स्त्रीवेद है. स्त्री के साथ रतिसुख की कामना पुरुषवेद है. उभय के साथ की कामना नपुंसकवेद है. इस प्रकार कामवासना का क्षय होना ही 'निर्वेद' है. सम्यक्त्वी का जीवन भोगलक्षी नहीं होता. वह न इह लोक के भोग चाहता है और न स्वर्ग आदि के ही. प्रशम और संवेग की साधना करते-करते वेदोदय की प्रवृत्ति उसी प्रकार क्षीण हो जाती है, जिस प्रकार ज्ञानाभ्यास में रत विद्यार्थी का मन बचपन में खेले हुए गंदे खेलों से उपरत हो जाता है. सम्यक्त्वी कोमल हृदय होता है. दूसरे को पीड़ा और कष्ट में देखकर वह द्रवित हो उठता है. क्योंकि वह प्राणीमात्रके साथ आत्मीयता की अनुभूति करता है. आत्मीयता के कारण दूसरों का सुख दुःख भी अपना हो जाता है. इसी संवेदनशीलता तथा सहानुभूतिने मनुष्य के हृदयमें दया और दान भावना की सृष्टि की है. मानव को पशु और दानव बननेसे बचाने में इसी का सर्वाधिक योग है. किसीको पीड़ित अवस्था में देखकर हृदय में करुणा का उत्स प्रवाहित होना स्वाभाविक है. आत्मा का यही एक ऐसा सहज गुण है—जिसने पृथ्वी पर बार-बार प्रलय होने से रोका है. इसका विस्तार यदि समुचित रूप से किया जाय तो आज दुनिया को परेशान करने वाला शीत युद्ध भी उपशान्त हो सकता है. इसका स्वाभाविक विकास इन समस्त गत्यवरोधों को समाहित कर शान्ति और सौरभ्य का निर्भर प्रवाहित कर सकता है. दूसरों के सुख दुःख को आत्मीय भाव से ग्रहण कर उनके कष्टों को मिटाने का प्रयास ही अनुकम्पा है. अनुकम्पा सामाजिक जीवन एवं सहजीवन का स्नेहसूत्र है. अनुकम्पा के कारण ही मनुष्य अपनी तथा अपने परिवार की तरह ही, अपने अधीनस्थ व्यक्तियों की योग्य और उचित आवश्यकताओं की पूर्ति सम्यक् रूप से करता है. दूसरों की आवश्यकताओं का ध्यान न रखकर अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाते रहने से अनुकम्पा का घात होता है. सम्यक्त्व-आराधक अपनी आजीविका का अर्जन करने के लिए जो साधन अपनाता है, उसमें किसी प्रकार की अप्रामाणिकता न आ जाय, इसके लिए सतत जागरूक रहता है. सम्यक्त्व गुण के विस्तार के लिए आस्तिकता आवश्यक होती है. मनुष्य ज्यों-ज्यों सद्गुणों को जीवन में अपनाता है त्यों-त्यों आस्तिक्य गुण का विकास होता है. आस्तिकता श्रद्धा को बलवती बनाती है. श्रद्धा कभी मनुष्य को बिपथगामी नहीं होने देती. श्रद्धा और अंधश्रद्धा में अन्तर है. अंधश्रद्धालु दूसरों के प्रति अशिष्ट व्यवहार कर सकता है, किन्तु श्रद्धालु ऐसा नहीं कर सकता. उसमें करुणा, मुदिता, मैत्री और, तटस्थता विद्यमान रहती है. आत्मा और उसके विकास के
NOVतकता
SELEASEX
क9.9.-DI.
Jain ducato
Aredusesvi
w.jainrary.org
LA