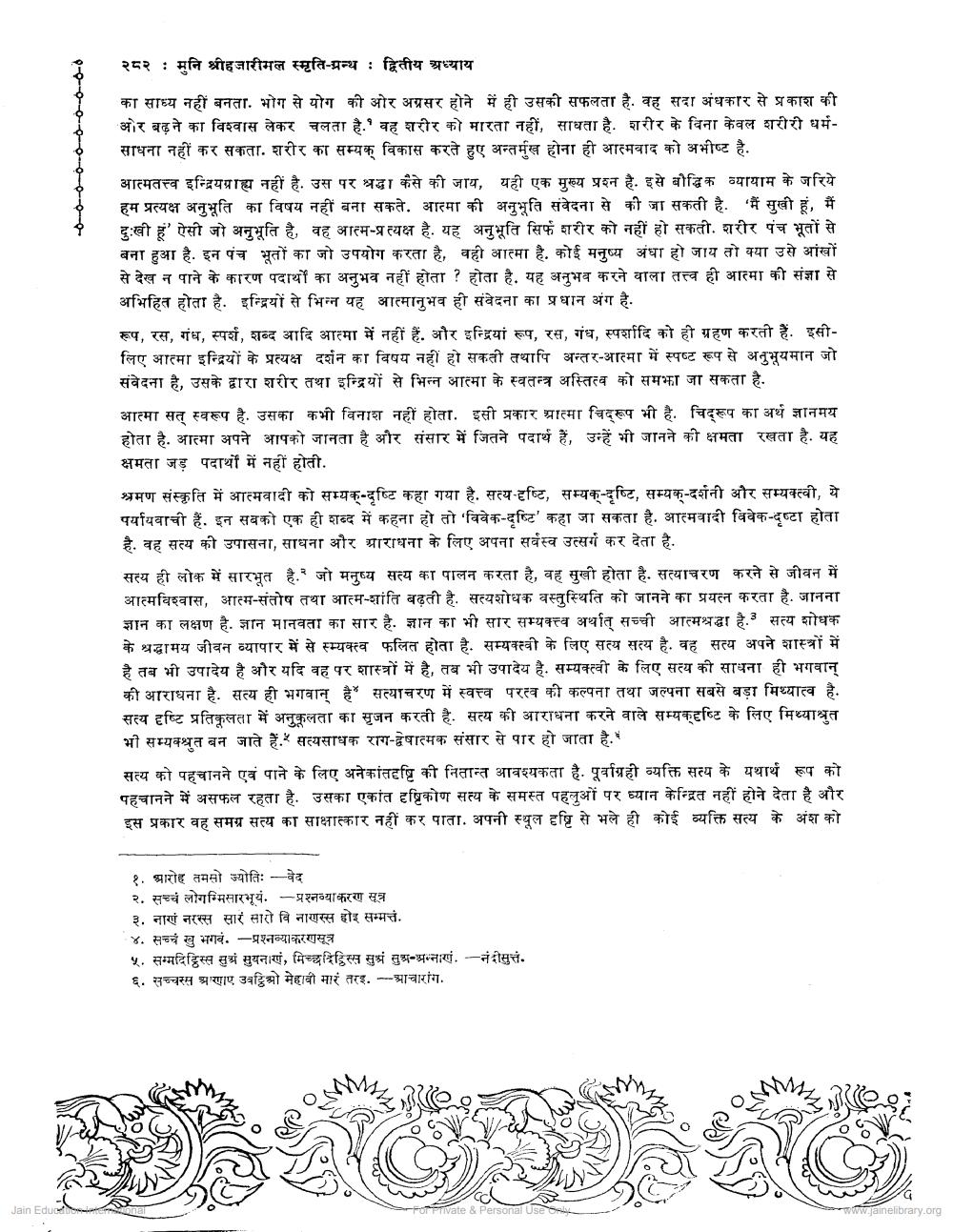________________
२८२ : मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-ग्रन्थ : द्वितीय अध्याय
هههههههه
का साध्य नहीं बनता. भोग से योग की ओर अग्रसर होने में ही उसकी सफलता है. वह सदा अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का विश्वास लेकर चलता है.' वह शरीर को मारता नहीं, साधता है. शरीर के विना केवल शरीरी धर्मसाधना नहीं कर सकता. शरीर का सम्यक् विकास करते हुए अन्तर्मुख होना ही आत्मवाद को अभीष्ट है. आत्मतत्त्व इन्द्रियग्राह्य नहीं है. उस पर श्रद्धा कैसे की जाय, यही एक मुख्य प्रश्न है. इसे बौद्धिक व्यायाम के जरिये हम प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय नहीं बना सकते. आत्मा की अनुभूति संवेदना से की जा सकती है. मैं सुखी हूं, मैं दुःखी हूं' ऐसी जो अनुभूति है, वह आत्म-प्रत्यक्ष है. यह अनुभूति सिर्फ शरीर को नहीं हो सकती. शरीर पंच भूतों से बना हुआ है. इन पंच भूतों का जो उपयोग करता है, वही आत्मा है. कोई मनुष्य अंधा हो जाय तो क्या उसे आंखों से देख न पाने के कारण पदार्थों का अनुभव नहीं होता ? होता है. यह अनुभव करने वाला तत्त्व ही आत्मा की संज्ञा से अभिहित होता है. इन्द्रियों से भिन्न यह आत्मानुभव ही संवेदना का प्रधान अंग है. रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि आत्मा में नहीं हैं. और इन्द्रियां रूप, रस, गंध, स्पर्शादि को ही ग्रहण करती हैं. इसीलिए आत्मा इन्द्रियों के प्रत्यक्ष दर्शन का विषय नहीं हो सकती तथापि अन्तर-आत्मा में स्पष्ट रूप से अनुभूयमान जो संवेदना है, उसके द्वारा शरीर तथा इन्द्रियों से भिन्न आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व को समझा जा सकता है. आत्मा सत् स्वरूप है. उसका कभी विनाश नहीं होता. इसी प्रकार प्रात्मा चिद्रूप भी है. चिद्रूप का अर्थ ज्ञानमय होता है. आत्मा अपने आपको जानता है और संसार में जितने पदार्थ हैं, उन्हें भी जानने की क्षमता रखता है. यह क्षमता जड़ पदार्थों में नहीं होती. श्रमण संस्कृति में आत्मवादी को सम्यक्-दृष्टि कहा गया है. सत्य-दृष्टि, सम्यक्-दृष्टि, सम्यक्-दर्शनी और सम्यक्त्वी, ये पर्यायवाची हैं. इन सबको एक ही शब्द में कहना हो तो 'विवेक-दृष्टि' कहा जा सकता है. आत्मवादी विवेक-दृष्टा होता है. वह सत्य की उपासना, साधना और आराधना के लिए अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर देता है. सत्य ही लोक में सारभुत है. जो मनुष्य सत्य का पालन करता है, वह सुखी होता है. सत्याचरण करने से जीवन में आत्मविश्वास, आत्म-संतोष तथा आत्म-शांति बढ़ती है. सत्यशोधक वस्तुस्थिति को जानने का प्रयत्न करता है. जानना ज्ञान का लक्षण है. ज्ञान मानवता का सार है. ज्ञान का भी सार सम्यक्त्त्व अर्थात् सच्ची आत्मश्रद्धा है. सत्य शोधक के श्रद्धामय जीवन व्यापार में से स्म्यक्त्व फलित होता है. सम्यक्त्वी के लिए सत्य सत्य है. वह सत्य अपने शास्त्रों में है तब भी उपादेय है और यदि वह पर शास्त्रों में है, तब भी उपादेय है. सम्यक्त्वी के लिए सत्य की साधना ही भगवान् की आराधना है. सत्य ही भगवान् है सत्याचरण में स्वत्त्व परत्व की कल्पना तथा जल्पना सबसे बड़ा मिथ्यात्व है. सत्य दृष्टि प्रतिकूलता में अनुकूलता का सृजन करती है. सत्य की आराधना करने वाले सम्यक्दृष्टि के लिए मिथ्याश्रुत भी सम्यक्थुत बन जाते हैं.५ सत्यसाधक राग-द्वेषात्मक संसार से पार हो जाता है. सत्य को पहचानने एवं पाने के लिए अनेकांतदृष्टि की नितान्त आवश्यकता है. पूर्वाग्रही व्यक्ति सत्य के यथार्थ रूप को पहचानने में असफल रहता है. उसका एकांत दृष्टिकोण सत्य के समस्त पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित नहीं होने देता है और इस प्रकार वह समग्र सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाता. अपनी स्थूल दृष्टि से भले ही कोई व्यक्ति सत्य के अंश को
१. पारोह तमसो ज्योतिः -वेद २. सच्चं लोगम्मिसारभूयं. -प्रश्नव्याकरण सूत्र ३. नाणं नरस्स सारं सारो वि नागरस होइ सम्मत्तं. ४. सच्चे खु भगवं. -प्रश्नव्याकरणसूत्र ५. सम्मदिट्ठिस्स सुअं सुयनाणं, मिच्छदिहिस्स सुअं सुअ-अन्नाणं. --नंदीसुत्तं. ६. सच्चरस प्राणाए उबढिओ मेहावी मारं तरइ. --आचारांग.
JainEducation
FORPrivate & Personal use only
www.jainelibrary.org