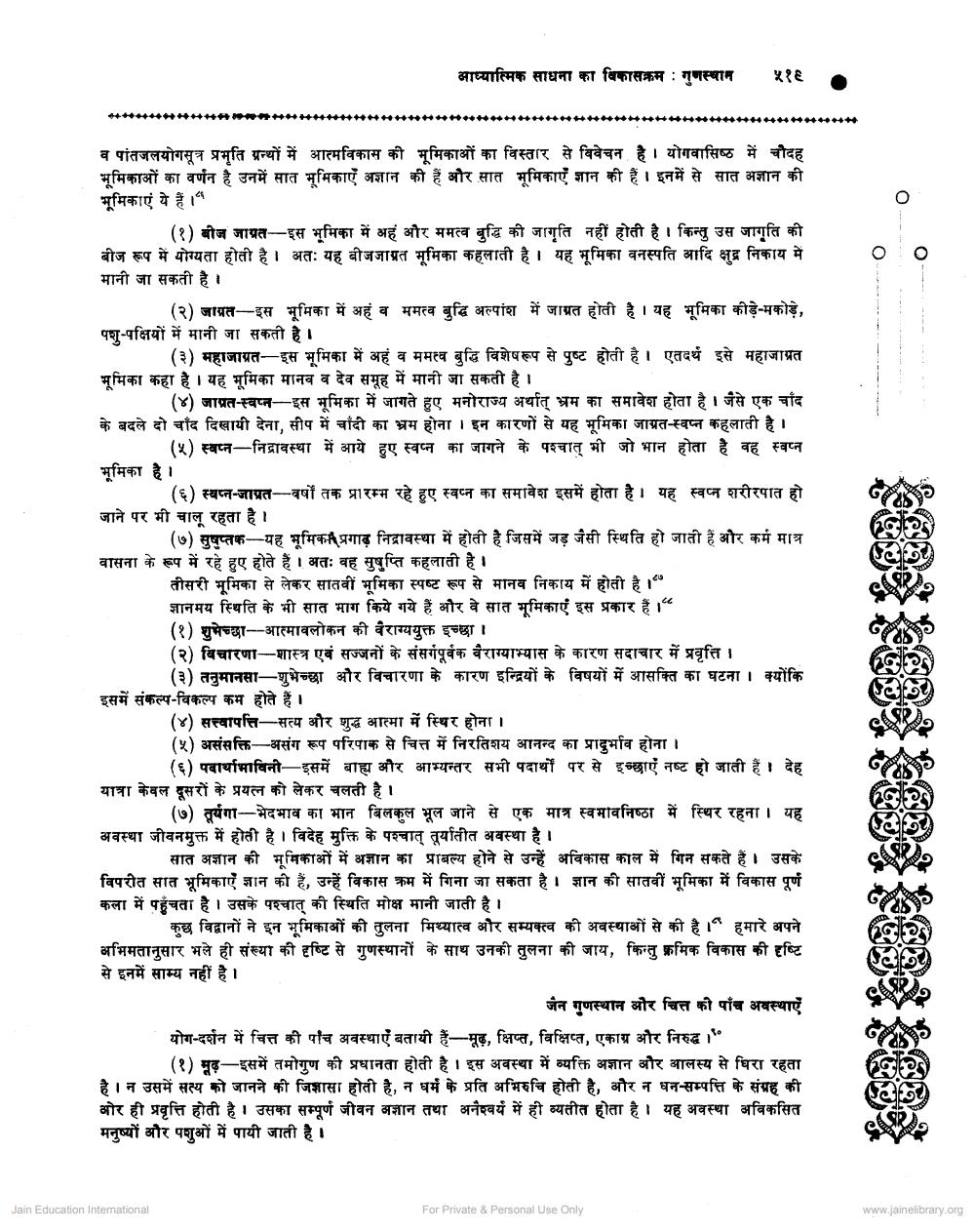________________
आध्यात्मिक साधना का विकासक्रम : गुणस्थान
५१६
व पांतजलयोगसूत्र प्रभृति ग्रन्थों में आत्मविकास की भूमिकाओं का विस्तार से विवेचन है। योगवासिष्ठ में चौदह भूमिकाओं का वर्णन है उनमें सात भूमिकाएँ अज्ञान की हैं और सात भूमिकाएँ ज्ञान की हैं। इनमें से सात अज्ञान की भूमिकाएं ये हैं ।
(१) बीज जाग्रत-इस भूमिका में अहं और ममत्व बुद्धि की जागृति नहीं होती है । किन्तु उस जागृति की बीज रूप में योग्यता होती है। अतः यह बीजजाग्रत भूमिका कहलाती है। यह भूमिका वनस्पति आदि क्षुद्र निकाय में मानी जा सकती है।
(२) जाग्रत-इस भूमिका में अहं व ममत्व बुद्धि अल्पांश में जाग्रत होती है । यह भूमिका कीड़े-मकोड़े, पशु-पक्षियों में मानी जा सकती है।
(३) महाजाग्रत-इस भूमिका में अहं व ममत्व बुद्धि विशेष रूप से पुष्ट होती है। एतदर्थ इसे महाजाग्रत भूमिका कहा है । यह भूमिका मानव व देव समूह में मानी जा सकती है।।
(४) जाग्रत-स्वप्न-इस भूमिका में जागते हुए मनोराज्य अर्थात् भ्रम का समावेश होता है । जैसे एक चाँद के बदले दो चाँद दिखायी देना, सीप में चाँदी का भ्रम होना । इन कारणों से यह भूमिका जाग्रत-स्वप्न कहलाती है।
(५) स्वप्न-निद्रावस्था में आये हुए स्वप्न का जागने के पश्चात् भी जो भान होता है वह स्वप्न भूमिका है।
(६) स्वप्न-जाग्रत-वर्षों तक प्रारम्भ रहे हुए स्वप्न का समावेश इसमें होता है। यह स्वप्न शरीरपात हो जाने पर भी चालू रहता है।
(७) सुषुप्तक-यह भूमिका प्रगाढ़ निद्रावस्था में होती है जिसमें जड़ जैसी स्थिति हो जाती हैं और कर्म मात्र वासना के रूप में रहे हुए होते हैं । अतः वह सुषुप्ति कहलाती है।
तीसरी भूमिका से लेकर सातवीं भूमिका स्पष्ट रूप से मानव निकाय में होती है। ज्ञानमय स्थिति के भी सात भाग किये गये हैं और वे सात भूमिकाएं इस प्रकार हैं।" (१) शुभेच्छा--आत्मावलोकन की वैराग्ययुक्त इच्छा। (२) विचारणा-शास्त्र एवं सज्जनों के संसर्गपूर्वक वैराग्याभ्यास के कारण सदाचार में प्रवृत्ति ।
(३) तनुमानसा-शुभेच्छा और विचारणा के कारण इन्द्रियों के विषयों में आसक्ति का घटना । क्योंकि इसमें संकल्प-विकल्प कम होते हैं।
(४) सत्त्वापत्ति-सत्य और शुद्ध आत्मा में स्थिर होना। (५) असंसक्ति-असंग रूप परिपाक से चित्त में निरतिशय आनन्द का प्रादुर्भाव होना।
(६) पदार्थाभाविनी-इसमें बाह्य और आभ्यन्तर सभी पदार्थों पर से इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। देह यात्रा केवल दूसरों के प्रयत्न को लेकर चलती है।
(७) तूर्यगा-भेदभाव का भान बिलकुल भूल जाने से एक मात्र स्वभावनिष्ठा में स्थिर रहना । यह अवस्था जीवनमुक्त में होती है । विदेह मुक्ति के पश्चात् तूर्यातीत अवस्था है।
सात अज्ञान की भूमिकाओं में अज्ञान का प्राबल्य होने से उन्हें अविकास काल में गिन सकते हैं। उसके विपरीत सात भूमिकाएं ज्ञान की हैं, उन्हें विकास क्रम में गिना जा सकता है। ज्ञान की सातवीं भूमिका में विकास पूर्ण कला में पहुंचता है। उसके पश्चात् की स्थिति मोक्ष मानी जाती है।
कुछ विद्वानों ने इन भूमिकाओं की तुलना मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की अवस्थाओं से की है। हमारे अपने अभिमतानुसार भले ही संख्या की दृष्टि से गुणस्थानों के साथ उनकी तुलना की जाय, किन्तु क्रमिक विकास की दृष्टि से इनमें साम्य नहीं है।
जैन गुणस्थान और चित्त को पाँच अवस्थाएं योग-दर्शन में चित्त की पांच अवस्थाएं बतायी हैं-मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध ।
(१) मूढ़-इसमें तमोगुण की प्रधानता होती है । इस अवस्था में व्यक्ति अज्ञान और आलस्य से घिरा रहता है । न उसमें सत्य को जानने की जिज्ञासा होती है, न धर्म के प्रति अभिरुचि होती है, और न धन-सम्पत्ति के संग्रह की ओर ही प्रवृत्ति होती है। उसका सम्पूर्ण जीवन अज्ञान तथा अनैश्वर्य में ही व्यतीत होता है। यह अवस्था अविकसित मनुष्यों और पशुओं में पायी जाती है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org