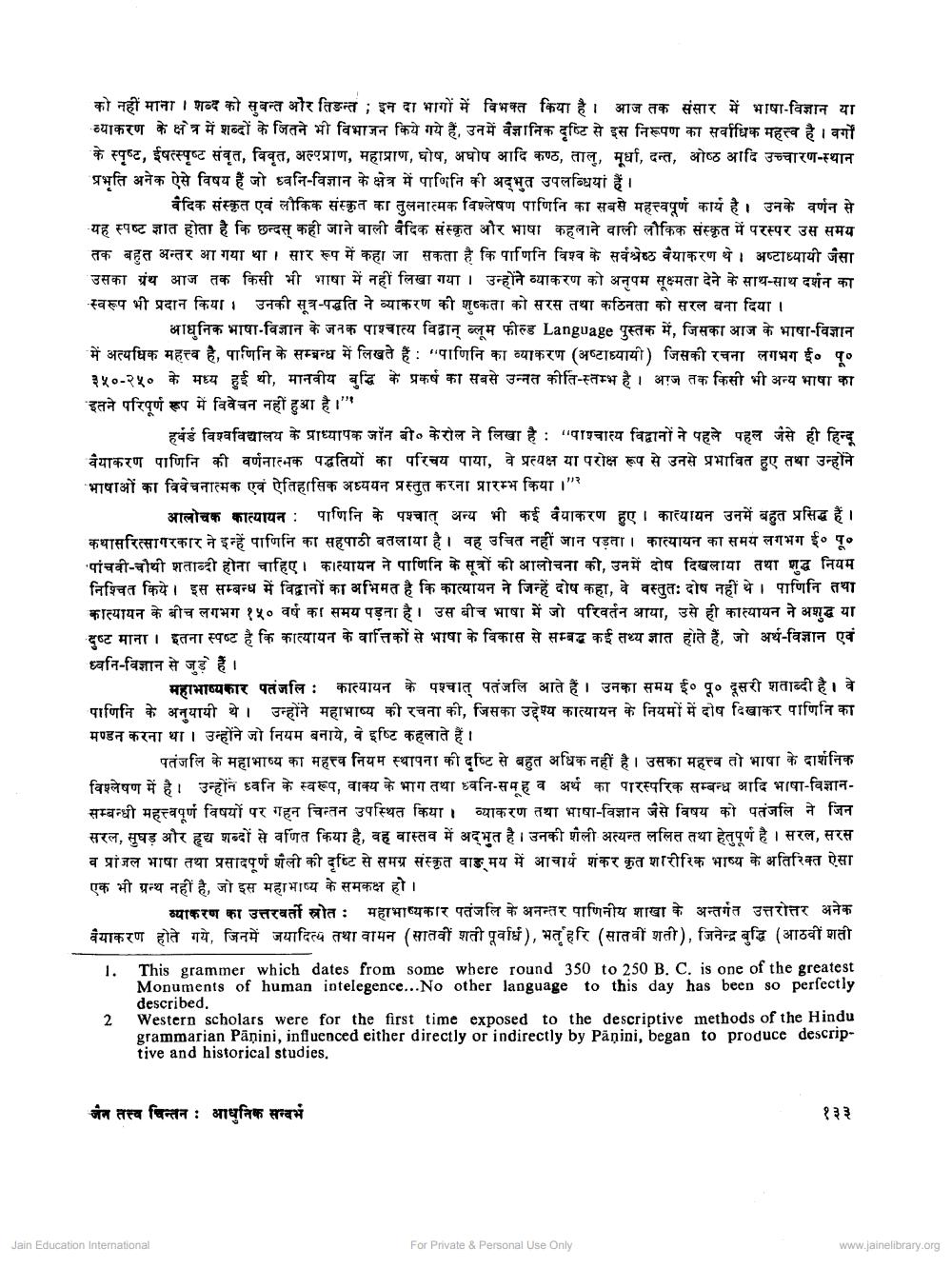________________
को नहीं माना । शब्द को सुबन्त और तिङन्त ; इन दा भागों में विभक्त किया है। आज तक संसार में भाषा-विज्ञान या व्याकरण के क्षेत्र में शब्दों के जितने भी विभाजन किये गये हैं, उनमें वैज्ञानिक दृष्टि से इस निरूपण का सर्वाधिक महत्त्व है । वर्गों के स्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट संवृत, विवृत, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष आदि कण्ठ, तालु, मूर्धा, दन्त, ओष्ठ आदि उच्चारण-स्थान प्रभति अनेक ऐसे विषय हैं जो ध्वनि-विज्ञान के क्षेत्र में पाणिनि की अद्भुत उपलब्धियां हैं।
वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत का तुलनात्मक विश्लेषण पाणिनि का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है। उनके वर्णन से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि छन्दस् कही जाने वाली वैदिक संस्कृत और भाषा कहलाने वाली लौकिक संस्कृत में परस्पर उस समय तक बहुत अन्तर आ गया था। सार रूप में कहा जा सकता है कि पाणिनि विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण थे। अष्टाध्यायी जैसा उसका ग्रंथ आज तक किसी भी भाषा में नहीं लिखा गया। उन्होंने व्याकरण को अनपम सूक्ष्मता देने के साथ-साथ दर्शन का स्वरूप भी प्रदान किया। उनकी सूत्र-पद्धति ने व्याकरण की शुष्कता को सरस तथा कठिनता को सरल बना दिया ।
आधुनिक भाषा-विज्ञान के जनक पाश्चात्य विद्वान् ब्लूम फील्ड Language पुस्तक में, जिसका आज के भाषा-विज्ञान में अत्यधिक महत्त्व है, पाणिनि के सम्बन्ध में लिखते हैं : "पाणिनि का व्याकरण (अष्टाध्यायी) जिसकी रचना लगभग ई० पू० ३५०-२५० के मध्य हुई थी, मानवीय बुद्धि के प्रकर्ष का सबसे उन्नत कीर्ति-स्तम्भ है। आज तक किसी भी अन्य भाषा का इतने परिपूर्ण रूप में विवेचन नहीं हुआ है।"
हर्वर्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक जॉन बी० केरोल ने लिखा है : "पाश्चात्य विद्वानों ने पहले पहल जैसे ही हिन्दू वैयाकरण पाणिनि की वर्णनात्मक पद्धतियों का परिचय पाया, वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनसे प्रभावित हुए तथा उन्होंने 'भाषाओं का विवेचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत करना प्रारम्भ किया।"
आलोचक कात्यायन : पाणिनि के पश्चात् अन्य भी कई वैयाकरण हुए। कात्यायन उनमें बहुत प्रसिद्ध हैं। कथासरित्सागरकार ने इन्हें पाणिनि का सहपाठी बतलाया है। वह उचित नहीं जान पड़ता। कात्यायन का समय लगभग ई० पू० 'पांचवी-चौथी शताब्दी होना चाहिए। कात्यायन ने पाणिनि के सूत्रों की आलोचना की, उनमें दोष दिखलाया तथा शुद्ध नियम निश्चित किये। इस सम्बन्ध में विद्वानों का अभिमत है कि कात्यायन ने जिन्हें दोष कहा, वे वस्तुतः दोष नहीं थे। पाणिनि तथा कात्यायन के बीच लगभग १५० वर्ष का समय पड़ता है। उस बीच भाषा में जो परिवर्तन आया, उसे ही कात्यायन ने अशुद्ध या दुष्ट माना। इतना स्पष्ट है कि कात्यायन के वात्तिकों से भाषा के विकास से सम्बद्ध कई तथ्य ज्ञात होते हैं, जो अर्थ-विज्ञान एवं ध्वनि-विज्ञान से जुड़े हैं।
महाभाष्यकार पतंजलि: कात्यायन के पश्चात् पतंजलि आते हैं। उनका समय ई०पू० दूसरी शताब्दी है। वे पाणिनि के अनुयायी थे। उन्होंने महाभाष्य की रचना की, जिसका उद्देश्य कात्यायन के नियमों में दोष दिखाकर पाणिनि का मण्डन करना था। उन्होंने जो नियम बनाये, वे इष्टि कहलाते हैं।
पतंजलि के महाभाष्य का महत्त्व नियम स्थापना की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है। उसका महत्त्व तो भाषा के दार्शनिक विश्लेषण में है। उन्होंने ध्वनि के स्वरूप, वाक्य के भाग तथा ध्वनि-समूह व अर्थ का पारस्परिक सम्बन्ध आदि भाषा-विज्ञानसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयों पर गहन चिन्तन उपस्थित किया। व्याकरण तथा भाषा-विज्ञान जैसे विषय को पतंजलि ने जिन सरल, सुघड़ और हृद्य शब्दों से वर्णित किया है, वह वास्तव में अद्भुत है। उनकी शैली अत्यन्त ललित तथा हेतुपूर्ण है । सरल, सरस व प्रांजल भाषा तथा प्रसादपूर्ण शैली की दृष्टि से समग्र संस्कृत वाङमय में आचार्य शंकर कृत शारीरिक भाष्य के अतिरिक्त ऐसा एक भी ग्रन्थ नहीं है, जो इस महाभाष्य के समकक्ष हो।
व्याकरण का उत्तरवर्ती स्रोत: महाभाष्यकार पतंजलि के अनन्तर पाणिनीय शाखा के अन्तर्गत उत्तरोत्तर अनेक वैयाकरण होते गये, जिनमें जयादित्य तथा वामन (सातवीं शती पूर्वार्ध), भर्तृहरि (सातवीं शती), जिनेन्द्र बुद्धि (आठवीं शती 1. This grammer which dates from some where round 350 to 250 B. C. is one of the greatest
Monuments of human intelegence...No other language to this day has been so perfectly
described. 2 Western scholars were for the first time exposed to the descriptive methods of the Hindu
grammarian Pāņini, influenced either directly or indirectly by Pāņini, began to produce descriptive and historical studies.
जैन तत्त्व चिन्तन : आधुनिक सन्दर्भ
१३३
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org