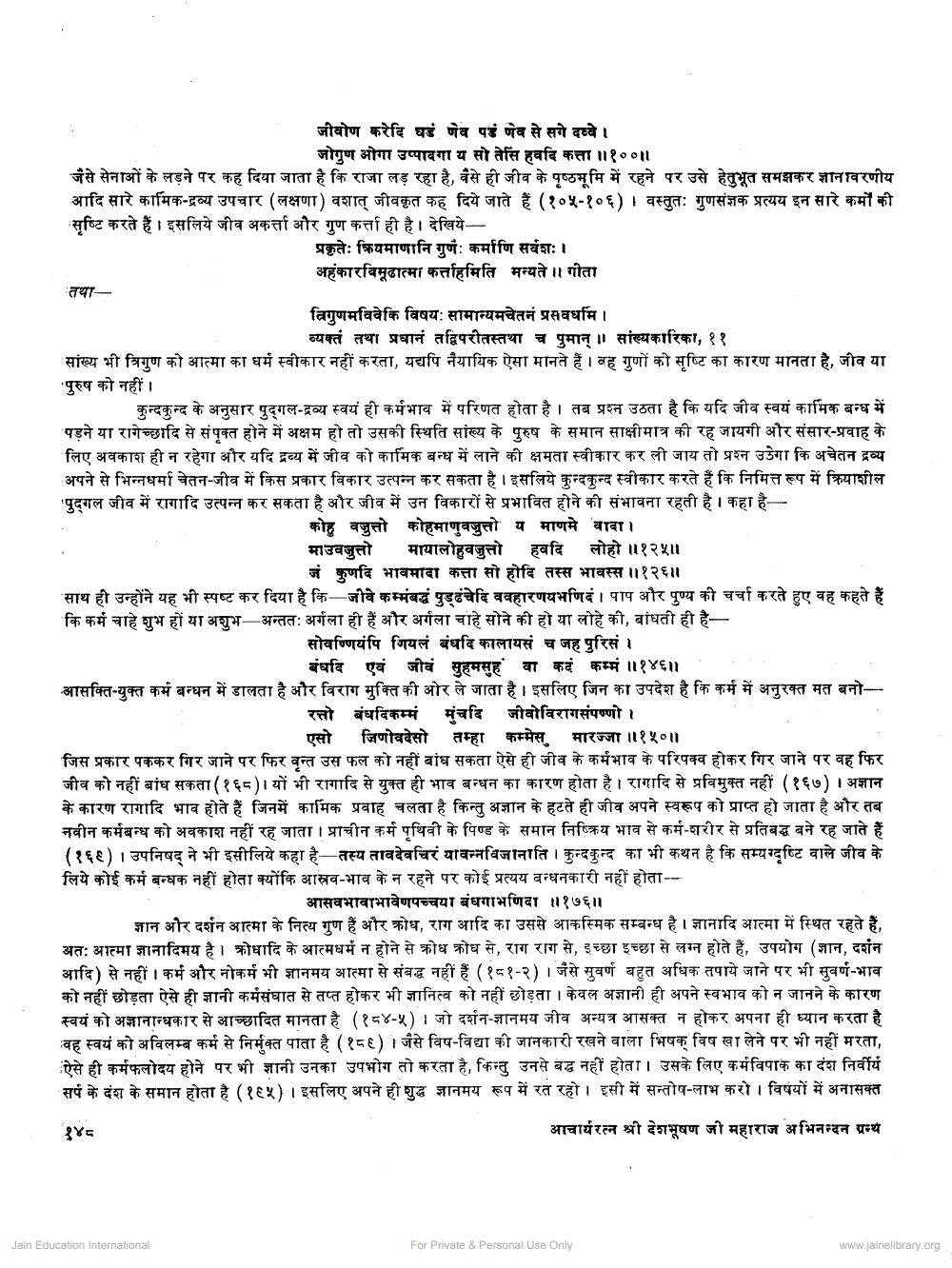________________
जीवोण करेदि घडं व पडणेव से सगे दब्वे ।
जोगुण ओगा उप्पादगा य सो तेसि हवदि कत्ता ॥१०॥ जैसे सेनाओं के लड़ने पर कह दिया जाता है कि राजा लड़ रहा है, वैसे ही जीव के पृष्ठभूमि में रहने पर उसे हेतुभूत समझकर ज्ञानावरणीय आदि सारे कार्मिक-द्रव्य उपचार (लक्षणा) वशात् जीवकृत कह दिये जाते हैं (१०५-१०६) । वस्तुत: गुणसंज्ञक प्रत्यय इन सारे कर्मों की सृष्टि करते हैं । इसलिये जीव अकर्ता और गुण कर्ता ही है। देखिये--
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः ।
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ गीता तथा
त्रिगुणमविवेकि विषय: सामान्यमचेतनं प्रसवमि ।
व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान् ॥ सांख्यकारिका, ११ सांख्य भी त्रिगुण को आत्मा का धर्म स्वीकार नहीं करता, यद्यपि नैयायिक ऐसा मानते हैं । वह गुणों को सृष्टि का कारण मानता है, जीव या 'पुरुष को नहीं।
कुन्दकुन्द के अनुसार पुद्गल-द्रव्य स्वयं ही कर्मभाव में परिणत होता है। तब प्रश्न उठता है कि यदि जीव स्वयं कार्मिक बन्ध में पड़ने या रागेच्छादि से संपृक्त होने में अक्षम हो तो उसकी स्थिति सांख्य के पुरुष के समान साक्षीमात्र की रह जायगी और संसार-प्रवाह के लिए अवकाश ही न रहेगा और यदि द्रव्य में जीव को कार्मिक बन्ध में लाने की क्षमता स्वीकार कर ली जाय तो प्रश्न उठेगा कि अचेतन द्रव्य अपने से भिन्नधर्मा चेतन-जीव में किस प्रकार विकार उत्पन्न कर सकता है। इसलिये कुन्दकुन्द स्वीकार करते हैं कि निमित्त रूप में क्रियाशील पुद्गल जीव में रागादि उत्पन्न कर सकता है और जीव में उन विकारों से प्रभावित होने की संभावना रहती है। कहा है
कोहु वजुत्तो कोहमाणुवजुत्तो य माणमे वादा। माउवजुत्तो मायालोहुवजुत्तो हवदि लोहो ॥१२॥
जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ॥१२६॥ साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि-जीवे कम्मंबद्धं पुढंचेदि ववहारणयभणिदं । पाप और पुण्य की चर्चा करते हुए वह कहते हैं कि कर्म चाहे शुभ हों या अशुभ–अन्तत: अर्गला ही हैं और अर्गला चाहे सोने की हो या लोहे की, बांधती ही है
सोवणियंपि गियलं बंधदि कालायसं च जह पुरिसं ।
बंधदि एवं जीवं सुहमसुह वा कदं कम्मं ॥१४६॥ आसक्ति-युक्त कर्म बन्धन में डालता है और विराग मुक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए जिन का उपदेश है कि कर्म में अनुरक्त मत बनो
रत्तो बंधदिकम्मं मुंचदि जीवोविरागसंपण्णो।
एसो जिणोवदेसो तम्हा कम्मेस मारज्जा ॥१५०॥ जिस प्रकार पककर गिर जाने पर फिर वृन्त उस फल को नहीं बांध सकता ऐसे ही जीव के कर्मभाव के परिपक्व होकर गिर जाने पर वह फिर जीव को नहीं बांध सकता (१६८)। यों भी रागादि से युक्त ही भाव बन्धन का कारण होता है। रागादि से प्रविमुक्त नहीं (१६७) । अज्ञान के कारण रागादि भाव होते हैं जिनमें कार्मिक प्रवाह चलता है किन्तु अज्ञान के हटते ही जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है और तब नवीन कर्मबन्ध को अवकाश नहीं रह जाता। प्राचीन कर्म पृथिवी के पिण्ड के समान निष्क्रिय भाव से कर्म-शरीर से प्रतिबद्ध बने रह जाते हैं (१६६) । उपनिषद् ने भी इसीलिये कहा है–तस्य तावदेवचिरं यावन्नविजानाति । कुन्दकुन्द का भी कथन है कि सम्यग्दृष्टि वाले जीव के लिये कोई कर्म बन्धक नहीं होता क्योंकि आस्रव-भाव के न रहने पर कोई प्रत्यय बन्धनकारी नहीं होता--
आसवभावाभावेणपच्चया बंधगाभणिदा ॥१७६॥ ज्ञान और दर्शन आत्मा के नित्य गुण हैं और क्रोध, राग आदि का उससे आकस्मिक सम्बन्ध है । ज्ञानादि आत्मा में स्थित रहते हैं, अत: आत्मा ज्ञानादिमय है। क्रोधादि के आत्मधर्म न होने से क्रोध क्रोध से, राग राग से, इच्छा इच्छा से लग्न होते हैं, उपयोग (ज्ञान, दर्शन आदि) से नहीं । कर्म और नोकर्म भी ज्ञानमय आत्मा से संबद्ध नहीं हैं (१८१-२) । जैसे सुवर्ण बहुत अधिक तपाये जाने पर भी सुवर्ण-भाव को नहीं छोड़ता ऐसे ही ज्ञानी कर्मसंघात से तप्त होकर भी ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता। केवल अज्ञानी ही अपने स्वभाव को न जानने के कारण स्वयं को अज्ञानान्धकार से आच्छादित मानता है (१८४-५) । जो दर्शन-ज्ञानमय जीव अन्यत्र आसक्त न होकर अपना ही ध्यान करता है वह स्वयं को अविलम्ब कर्म से निर्मुक्त पाता है (१८६) । जैसे विष-विद्या की जानकारी रखने वाला भिषक् विष खा लेने पर भी नहीं मरता, ऐसे ही कर्मफलोदय होने पर भी ज्ञानी उनका उपभोग तो करता है, किन्तु उनसे बद्ध नहीं होता। उसके लिए कर्मविपाक का दंश निर्वीर्य सर्प के दंश के समान होता है (१६५) । इसलिए अपने ही शुद्ध ज्ञानमय रूप में रत रहो। इसी में सन्तोष-लाभ करो । विषयों में अनासक्त
१४८
आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org