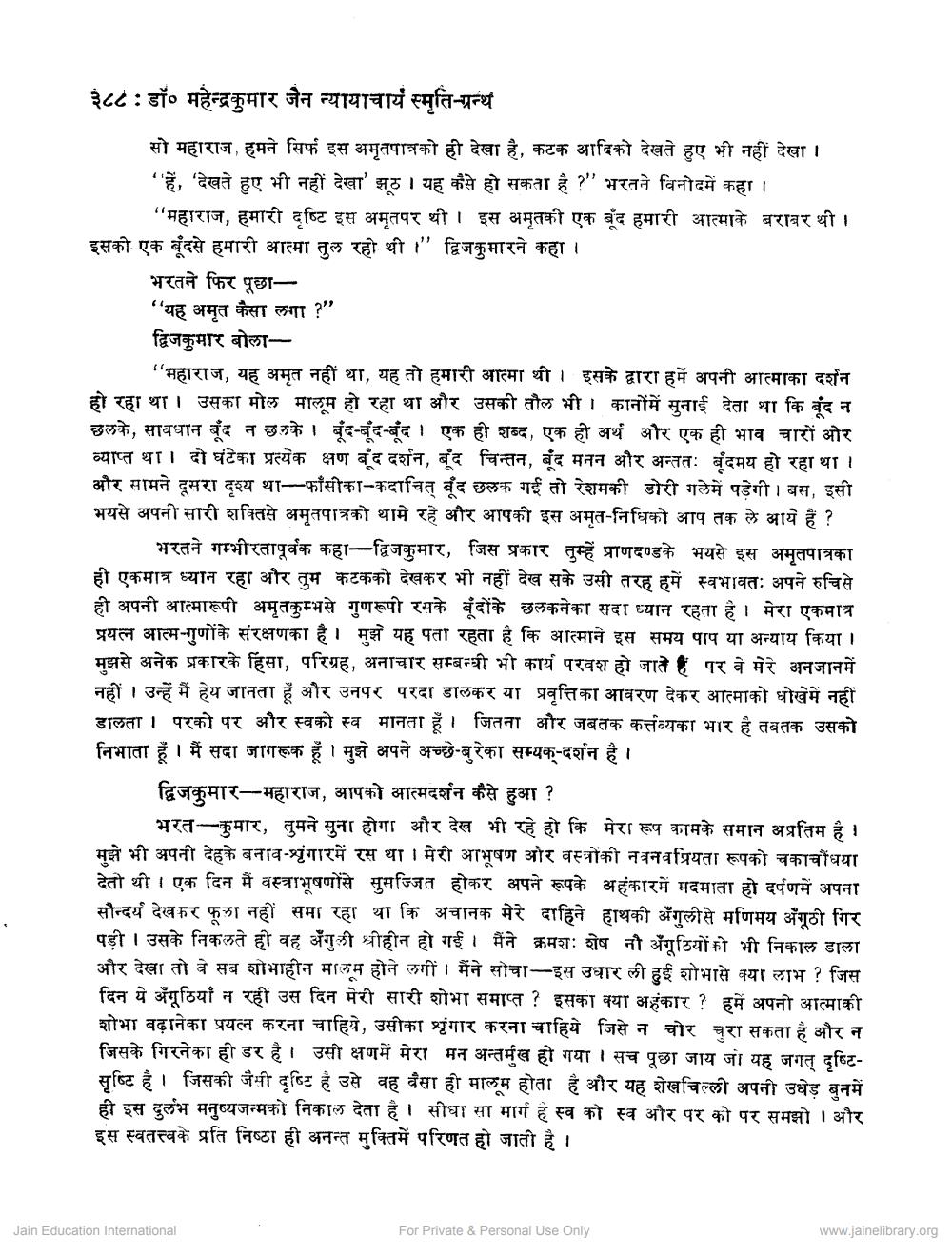________________
३८८ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ
सो महाराज, हमने सिर्फ इस अमृतपात्रको ही देखा है, कटक आदिको देखते हुए भी नहीं देखा । ''हे, 'देखते हुए भी नहीं देखा' झूठ । यह कैसे हो सकता है ?" भरतने विनोदमें कहा ।
"महाराज, हमारी दृष्टि इस अमृतपर थी। इस अमृतकी एक बंद हमारी आत्माके बराबर थी। इसको एक बूंदसे हमारी आत्मा तुल रही थी।" द्विजकुमारने कहा ।
भरतने फिर पूछा"यह अमृत कैसा लगा?" द्विजकुमार बोला
"महाराज, यह अमत नहीं था, यह तो हमारी आत्मा थी। इसके द्वारा हमें अपनी आत्माका दर्शन हो रहा था। उसका मोल मालम हो रहा था और उसकी तौल भी। कानोंमें सुनाई देता था कि बंद न छलके, सावधान बूंद न छलके । बूंद-बूंद-बूंद । एक ही शब्द, एक ही अर्थ और एक ही भाव चारों ओर व्याप्त था। दो घंटेका प्रत्येक क्षण बंद दर्शन, बूंद चिन्तन, बूंद मनन और अन्ततः बूंदमय हो रहा था। और सामने दूसरा दृश्य था-फाँसीका-कदाचित् बूंद छलक गई तो रेशमकी डोरी गले में पड़ेगी। बस, इसी भयसे अपनी सारी शक्तिसे अमृतपात्रको थामे रहे और आपकी इस अमत-निधिको आप तक ले आये हैं ?
भरतने गम्भीरतापूर्वक कहा-द्विजकुमार, जिस प्रकार तुम्हें प्राणदण्डके भयसे इस अमृतपात्रका ही एकमात्र ध्यान रहा और तुम कटकको देखकर भी नहीं देख सके उसी तरह हमें स्वभावतः अपने रुचिसे ही अपनी आत्मारूपी अमृतकुम्भसे गुणरूपी रसके बूंदोंके छलकनेका सदा ध्यान रहता है। मेरा एकमात्र प्रयत्न आत्म-गुणोंके संरक्षणका है। मुझे यह पता रहता है कि आत्माने इस समय पाप या अन्याय किया । मझसे अनेक प्रकारके हिंसा, परिग्रह, अनाचार सम्बन्धी भी कार्य परवश हो जाते है पर वे मेरे अनजानमें नहीं । उन्हें मैं हेय जानता हूँ और उनपर परदा डालकर या प्रवृत्तिका आवरण देकर आत्माको धोखेमें नहीं डालता । परको पर और स्वको स्व मानता हूँ। जितना और जबतक कर्त्तव्यका भार है तबतक उसको निभाता हूँ। मैं सदा जागरूक हूँ। मुझे अपने अच्छे-बुरेका सम्यक्-दर्शन है।
द्विजकुमार-महाराज, आपको आत्मदर्शन कैसे हुआ ?
भरत-कुमार, तुमने सुना होगा और देख भी रहे हो कि मेरा रूप कामके समान अप्रतिम है। मझे भी अपनी देहके बनाव-शृंगारमें रस था । मेरी आभूषण और वस्त्रोंकी नवनवप्रियता रूपको चकाचौंधया देतो थी। एक दिन मैं वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित होकर अपने रूपके अहंकारमें मदमाता हो दर्पणमें अपना सौन्दर्य देखकर फूला नहीं समा रहा था कि अचानक मेरे दाहिने हाथकी अँगुलीसे मणिमय अँगूठी गिर पड़ी। उसके निकलते ही वह अँगुली श्रीहीन हो गई। मैंने क्रमशः शेष नौ अँगूठियों को भी निकाल डाला और देखा तो वे सब शोभाहीन मालम होने लगीं। मैंने सोचा-इस उधार ली हुई शोभासे क्या लाभ ? जिस दिन ये अंगूठियाँ न रहीं उस दिन मेरी सारी शोभा समाप्त? इसका क्या अहंकार ? हमें अपनी आत्माकी शोभा बढ़ानेका प्रयत्न करना चाहिये, उसीका श्रृंगार करना चाहिये जिसे न चोर चुरा सकता है और न जिसके गिरनेका ही डर है। उसी क्षणमें मेरा मन अन्तर्मुख हो गया। सच पूछा जाय जो यह जगत् दृष्टिसृष्टि है। जिसकी जैसी दृष्टि है उसे वह वैसा ही मालूम होता है और यह शेखचिल्ली अपनी उधेड़ बुनमें ही इस दुर्लभ मनुष्यजन्मको निकाल देता है । सीधा सा मार्ग हे स्व को स्व और पर को पर समझो । और इस स्वतत्त्वके प्रति निष्ठा ही अनन्त मुक्तिमें परिणत हो जाती है ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org