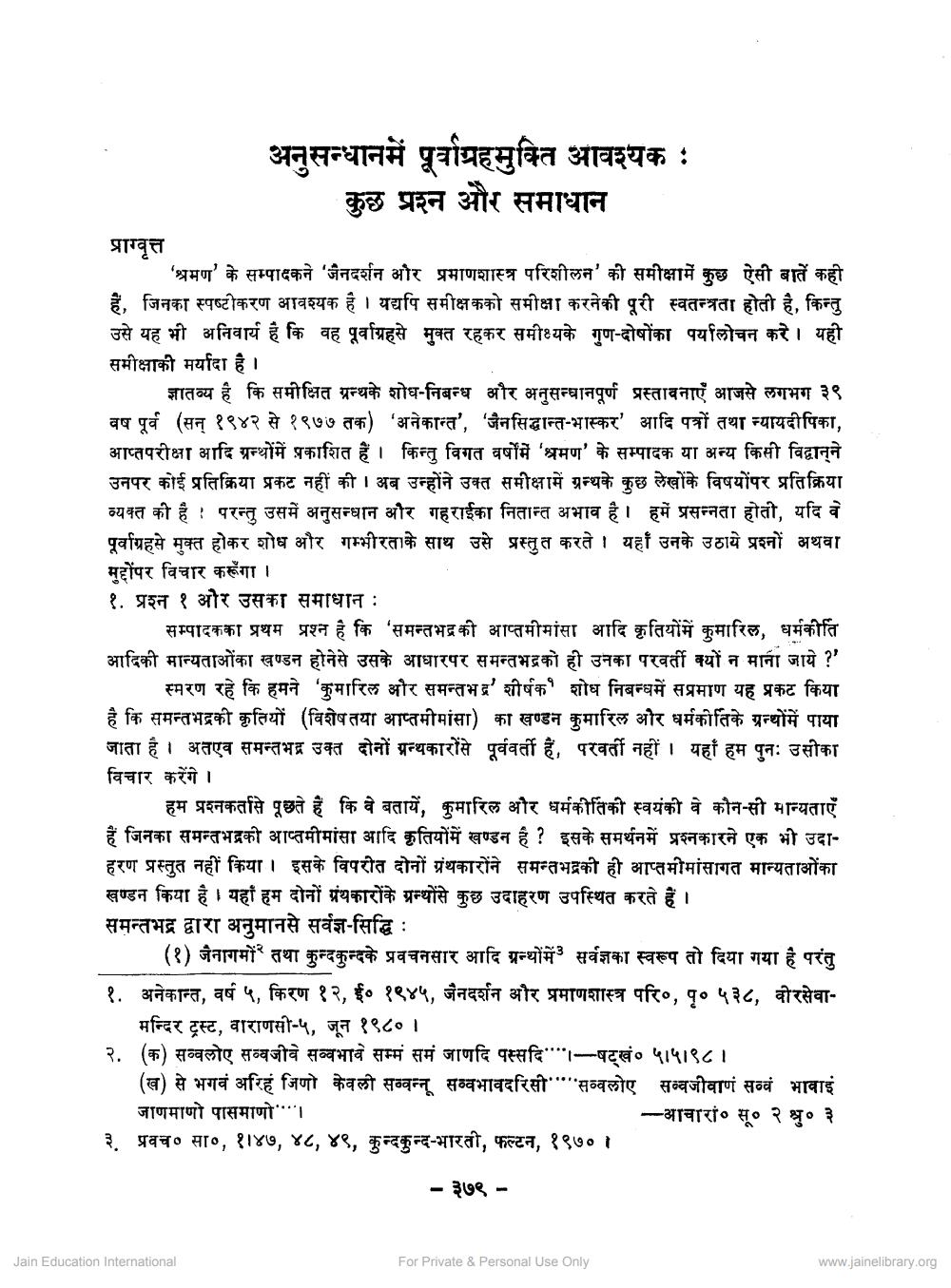________________
अनुसन्धानमें पूर्वाग्रहमुक्ति आवश्यक :
कुछ प्रश्न और समाधान
प्राग्वृत्त
___ 'श्रमण' के सम्पादकने 'जैनदर्शन और प्रमाणशास्त्र परिशीलन' की समीक्षामें कुछ ऐसी बातें कही है, जिनका स्पष्टीकरण आवश्यक है । यद्यपि समीक्षकको समीक्षा करनेकी पूरी स्वतन्त्रता होती है, किन्तु उसे यह भी अनिवार्य है कि वह पूर्वाग्रहसे मुक्त रहकर समीक्ष्यके गुण-दोषोंका पर्यालोचन करे। यही समीक्षाकी मर्यादा है।
ज्ञातव्य है कि समीक्षित ग्रन्थके शोध-निबन्ध और अनुसन्धानपूर्ण प्रस्तावनाएं आजसे लगभग ३९ वष पूर्व (सन् १९४२ से १९७७ तक) 'अनेकान्त', 'जैन सिद्धान्त-भास्कर' आदि पत्रों तथा न्यायदीपिका, आप्तपरीक्षा आदि ग्रन्थोंमें प्रकाशित हैं। किन्तु विगत वर्षों में 'श्रमण' के सम्पादक या अन्य किसी विद्वान्ने उनपर कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की । अब उन्होंने उक्त समीक्षामें ग्रन्थके कुछ लेखोंके विषयोंपर प्रतिक्रिया व्यक्त की है । परन्तु उसमें अनुसन्धान और गहराईका नितान्त अभाव है। हमें प्रसन्नता होती, यदि वे पूर्वाग्रहसे मुक्त होकर शोध और गम्भीरताके साथ उसे प्रस्तुत करते । यहाँ उनके उठाये प्रश्नों अथवा मुद्दोंपर विचार करूँगा। १. प्रश्न १ और उसका समाधान :
सम्पादकका प्रथम प्रश्न है कि 'समन्तभद्र की आप्तमीमांसा आदि कृतियोंमें कुमारिल, धर्मकीर्ति आदिकी मान्यताओंका खण्डन होनेसे उसके आधारपर समन्तभद्रको ही उनका परवर्ती क्यों न माना जाये ?'
स्मरण रहे कि हमने 'कुमारिल और समन्तभद्र' शीर्षक शोध निबन्धमें सप्रमाण यह प्रकट किया है कि समन्तभद्रकी कृतियों (विशेषतया आप्तमीमांसा) का खण्डन कुमारिल और धर्मकोतिके ग्रन्थोंमें पाया जाता है। अतएव समन्तभद्र उक्त दोनों ग्रन्थकारोंसे पूर्ववर्ती हैं, परवर्ती नहीं। यहाँ हम पुनः उसीका विचार करेंगे।
हम प्रश्नकर्तासे पूछते हैं कि वे बतायें, कुमारिल और धर्मकीतिकी स्वयंकी वे कौन-सी मान्यताएँ हैं जिनका समन्तभद्रकी आप्तमीमांसा आदि कृतियोंमें खण्डन है ? इसके समर्थन में प्रश्नकारने एक भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया। इसके विपरीत दोनों ग्रंथकारोंने समन्तभद्रकी ही आप्तमीमांसागत मान्यताओंका खण्डन किया है। यहाँ हम दोनों ग्रंथकारोंके ग्रन्थोंसे कुछ उदाहरण उपस्थित करते हैं। समन्तभद्र द्वारा अनुमानसे सर्वज्ञ-सिद्धि :
(१) जैनागमों तथा कुन्दकुन्दके प्रवचनसार आदि ग्रन्थों में सर्वज्ञका स्वरूप तो दिया गया है परंतु १. अनेकान्त, वर्ष ५, किरण १२, ई० १९४५, जैनदर्शन और प्रमाणशास्त्र परि०, पृ० ५३८, वीरसेवा
मन्दिर ट्रस्ट, वाराणसी-५, जून १९८० ।। २. (क) सव्वलोए सव्वजीवे सब्वभावे सम्म समं जाणदि पस्सदि""-षदख० ५।५।९८ ।
(ख) से भगवं अरिहं जिणो केवली सम्वन्न सव्वभावदरिसी'सव्वलोए सम्वजीवाणं सव्वं भावाई जाणमाणो पासमाणो।
-आवारां० सू० २ श्रु०३ ३. प्रवच० सा०, ११४७, ४८, ४९, कुन्दकुन्द-भारती, फल्टन, १९७० ।
-३७९
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org