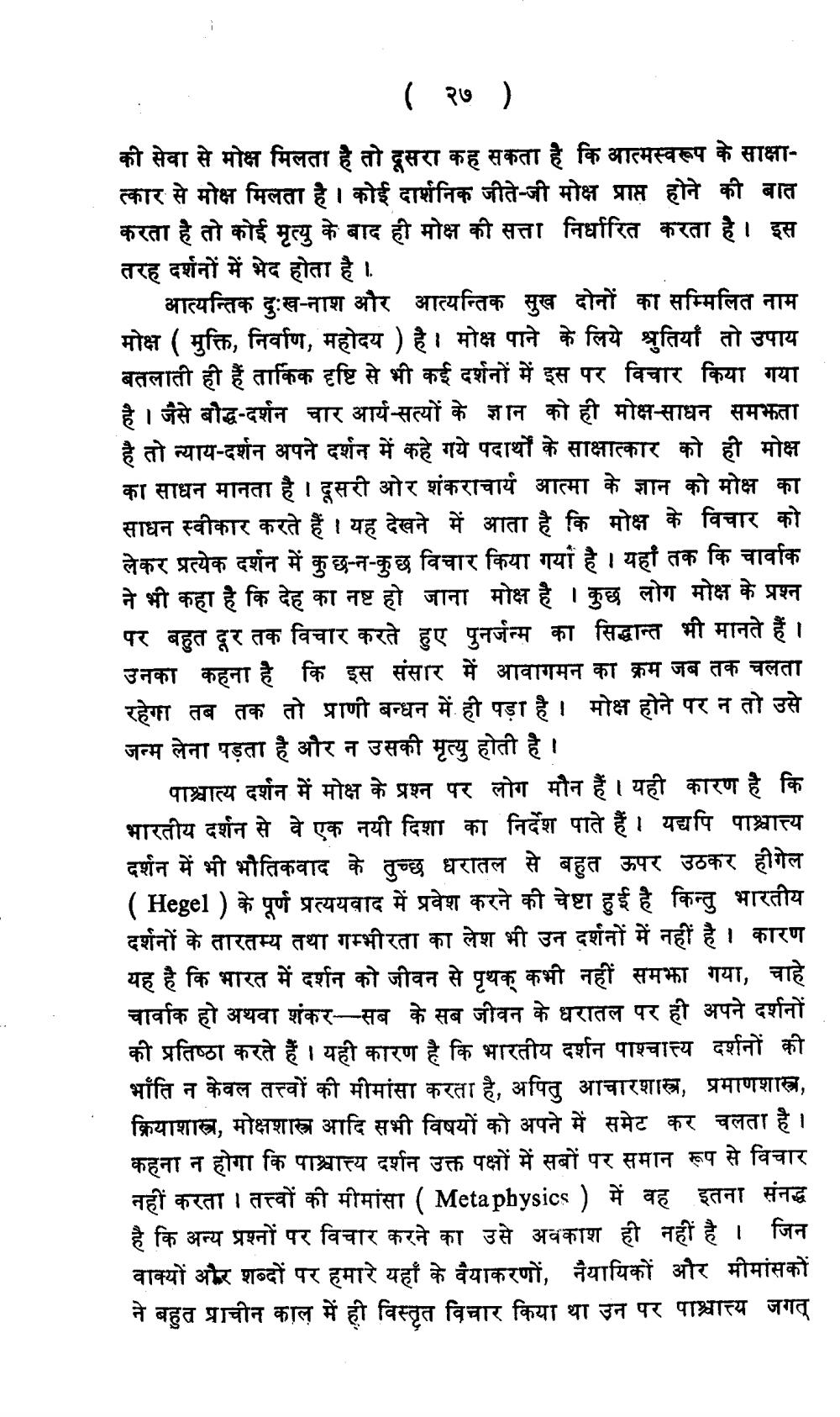________________
( २७ )
की सेवा से मोक्ष मिलता है तो दूसरा कह सकता है कि आत्मस्वरूप के साक्षात्कार से मोक्ष मिलता है। कोई दार्शनिक जीते-जी मोक्ष प्राप्त होने की बात करता है तो कोई मृत्यु के बाद ही मोक्ष की सत्ता निर्धारित करता है। इस तरह दर्शनों में भेद होता है ।
आत्यन्तिक दुःख-नाश और आत्यन्तिक सुख दोनों का सम्मिलित नाम मोक्ष ( मुक्ति, निर्वाण, महोदय ) है। मोक्ष पाने के लिये श्रुतियाँ तो उपाय बतलाती ही हैं तार्किक दृष्टि से भी कई दर्शनों में इस पर विचार किया गया है । जैसे बौद्ध-दर्शन चार आर्य-सत्यों के ज्ञान को ही मोक्ष-साधन समझता है तो न्याय-दर्शन अपने दर्शन में कहे गये पदार्थों के साक्षात्कार को ही मोक्ष का साधन मानता है । दूसरी ओर शंकराचार्य आत्मा के ज्ञान को मोक्ष का साधन स्वीकार करते हैं । यह देखने में आता है कि मोक्ष के विचार को लेकर प्रत्येक दर्शन में कुछ-न-कुछ विचार किया गया है। यहां तक कि चार्वाक ने भी कहा है कि देह का नष्ट हो जाना मोक्ष है । कुछ लोग मोक्ष के प्रश्न पर बहुत दूर तक विचार करते हुए पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी मानते हैं। उनका कहना है कि इस संसार में आवागमन का क्रम जब तक चलता रहेगा तब तक तो प्राणी बन्धन में ही पड़ा है। मोक्ष होने पर न तो उसे जन्म लेना पड़ता है और न उसकी मृत्यु होती है।
पाश्चात्य दर्शन में मोक्ष के प्रश्न पर लोग मौन हैं । यही कारण है कि भारतीय दर्शन से वे एक नयी दिशा का निर्देश पाते हैं। यद्यपि पाश्चात्त्य दर्शन में भी भौतिकवाद के तुच्छ धरातल से बहुत ऊपर उठकर हीगेल ( Hegel ) के पूर्ण प्रत्ययवाद में प्रवेश करने की चेष्टा हुई है किन्तु भारतीय दर्शनों के तारतम्य तथा गम्भीरता का लेश भी उन दर्शनों में नहीं है । कारण यह है कि भारत में दर्शन को जीवन से पृथक् कभी नहीं समझा गया, चाहे चार्वाक हो अथवा शंकर-सब के सब जीवन के धरातल पर ही अपने दर्शनों की प्रतिष्ठा करते हैं। यही कारण है कि भारतीय दर्शन पाश्चात्त्य दर्शनों की भाँति न केवल तत्त्वों की मीमांसा करता है, अपितु आचारशास्त्र, प्रमाणशास्त्र, क्रियाशास्त्र, मोक्षशास्त्र आदि सभी विषयों को अपने में समेट कर चलता है। कहना न होगा कि पाश्चात्त्य दर्शन उक्त पक्षों में सबों पर समान रूप से विचार नहीं करता । तत्त्वों की मीमांसा ( Metaphysics ) में वह इतना संनद्ध है कि अन्य प्रश्नों पर विचार करने का उसे अवकाश ही नहीं है । जिन वाक्यों और शब्दों पर हमारे यहाँ के वैयाकरणों, नैयायिकों और मीमांसकों ने बहुत प्राचीन काल में ही विस्तृत विचार किया था उन पर पाश्चात्त्य जगत्