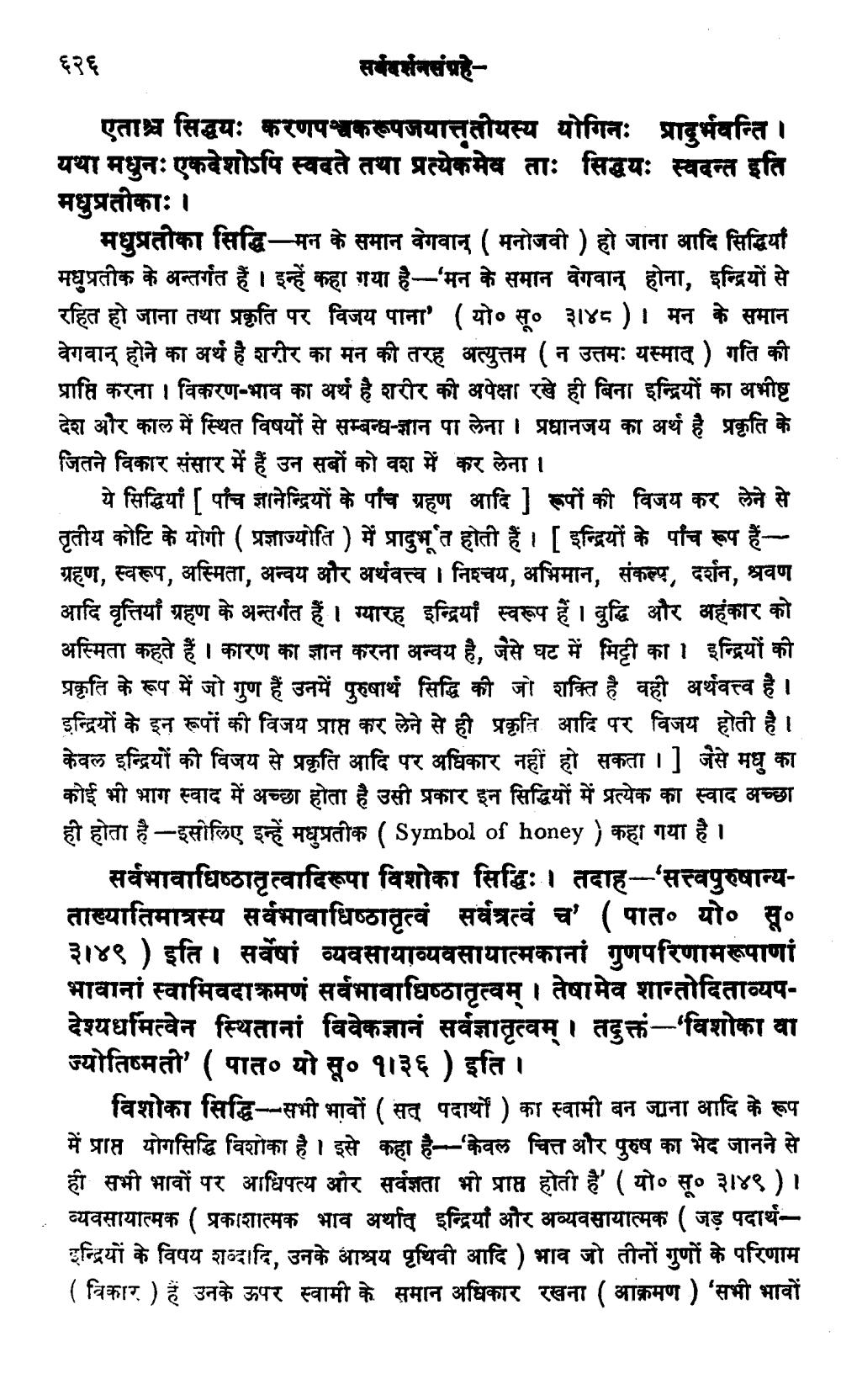________________
६२६
सर्ववसनसंग्रह एताश्च सिद्धयः करणपञ्चकरूपजयात्ततीयस्य योगिनः प्रादुर्भवन्ति । यथा मधुनः एकदेशोऽपि स्वदते तथा प्रत्येकमेव ताः सिद्धयः स्वदन्त इति मधुप्रतीकाः।
मधुप्रतीका सिद्धि-मन के समान वेगवान ( मनोजवी ) हो जाना आदि सिद्धियां मधुप्रतीक के अन्तर्गत हैं । इन्हें कहा गया है-'मन के समान वेगवान् होना, इन्द्रियों से रहित हो जाना तथा प्रकृति पर विजय पाना' ( यो० सू० ३।४८)। मन के समान वेगवान होने का अर्थ है शरीर का मन की तरह अत्युत्तम (न उत्तमः यस्मात् ) गति की प्राप्ति करना । विकरण-भाव का अर्थ है शरीर की अपेक्षा रखे ही बिना इन्द्रियों का अभीष्ट देश और काल में स्थित विषयों से सम्बन्ध-ज्ञान पा लेना । प्रधानजय का अर्थ है प्रकृति के जितने विकार संसार में हैं उन सबों को वश में कर लेना।
ये सिद्धियां [ पांच ज्ञानेन्द्रियों के पांच ग्रहण आदि ] रूपों की विजय कर लेने से तृतीय कोटि के योगी (प्रज्ञाज्योति ) में प्रादुर्भूत होती हैं। [ इन्द्रियों के पांच रूप हैंग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्त्व । निश्चय, अभिमान, संकल्प, दर्शन, श्रवण आदि वृत्तियाँ ग्रहण के अन्तर्गत हैं । ग्यारह इन्द्रियाँ स्वरूप हैं । बुद्धि और अहंकार को अस्मिता कहते हैं । कारण का ज्ञान करना अन्वय है, जैसे घट में मिट्टी का । इन्द्रियों की प्रकृति के रूप में जो गुण हैं उनमें पुरुषार्थ सिद्धि की जो शक्ति है वही अर्थवत्त्व है। इन्द्रियों के इन रूपों की विजय प्राप्त कर लेने से ही प्रकृति आदि पर विजय होती है। केवल इन्द्रियों की विजय से प्रकृति आदि पर अधिकार नहीं हो सकता । ] जैसे मधु का कोई भी भाग स्वाद में अच्छा होता है उसी प्रकार इन सिद्धियों में प्रत्येक का स्वाद अच्छा ही होता है - इसीलिए इन्हें मधुप्रतीक ( Symbol of honey ) कहा गया है। __ सर्वभावाधिष्ठातृत्वादिरूपा विशोका सिद्धिः । तदाह-'सत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वत्रत्वं च' (पात० यो० सू० ३।४९ ) इति । सर्वेषां व्यवसायाव्यवसायात्मकानां गुणपरिणामरूपाणां भावानां स्वामिवदाक्रमणं सर्वभावाधिष्ठातृत्वम् । तेषामेव शान्तोदिताव्यपदेश्यमित्वेन स्थितानां विवेकज्ञानं सर्वज्ञातृत्वम् । तदुक्तं-'विशोका वा ज्योतिष्मती' (पात० यो सू० ११३६ ) इति ।
विशोका सिद्धि-सभी भावों ( सत् पदार्थों ) का स्वामी बन जाना आदि के रूप में प्राप्त योगसिद्धि विशोका है। इसे कहा है-'केवल चित्त और पुरुष का भेद जानने से ही सभी भावों पर आधिपत्य और सर्वज्ञता भी प्राप्त होती है ( यो० सू० ३।४९)। व्यवसायात्मक ( प्रकाशात्मक भाव अर्थात इन्द्रियां और अव्यवसायात्मक ( जड़ पदार्थइन्द्रियों के विषय शब्दादि, उनके आश्रय पृथिवी आदि ) भाव जो तीनों गुणों के परिणाम ( विकार ) हैं उनके ऊपर स्वामी के समान अधिकार रखना ( आक्रमण ) 'सभी भावों