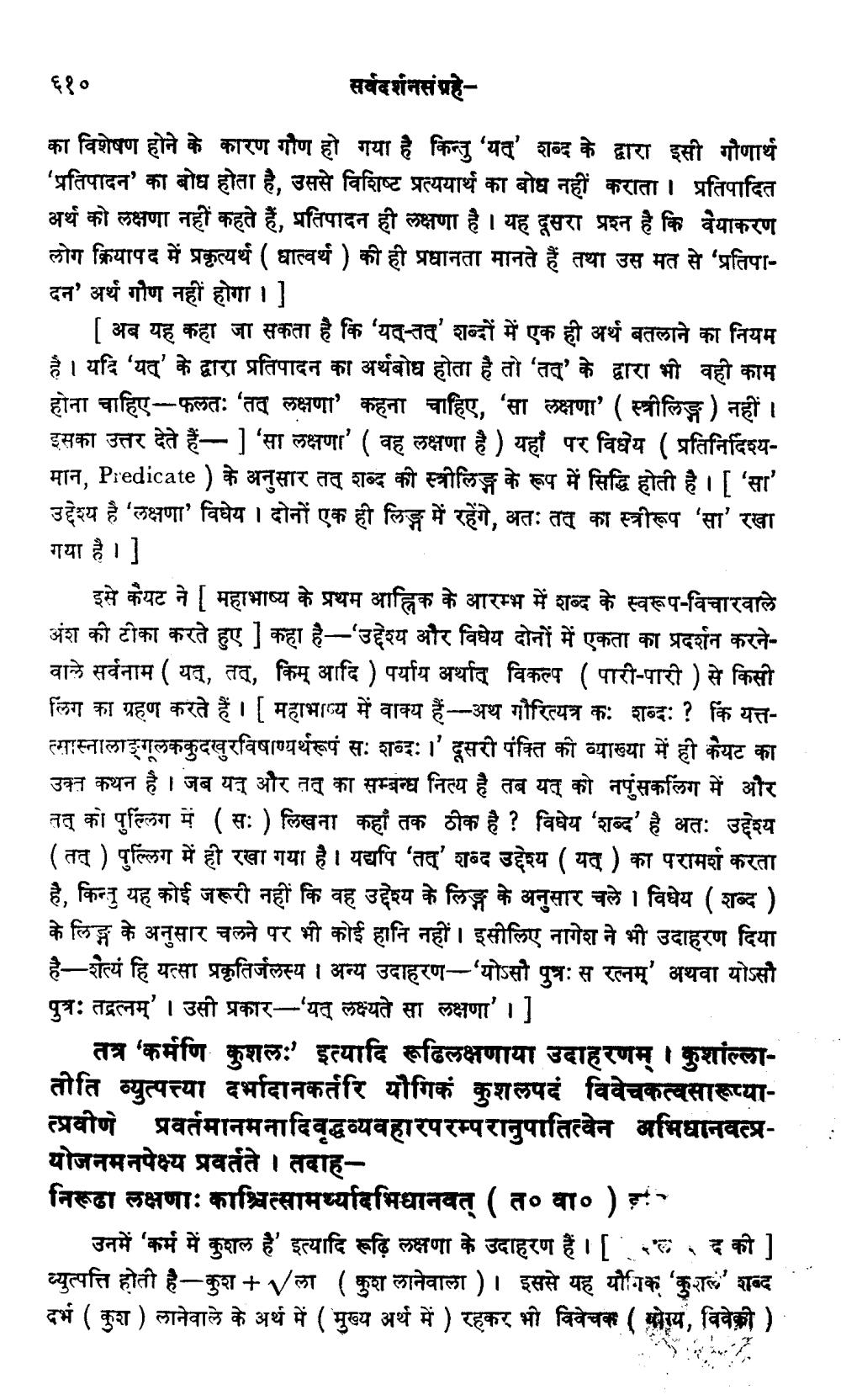________________
६१०
सर्वदर्शनसंग्रहे
का विशेषण होने के कारण गौण हो गया है किन्तु 'यत्' शब्द के द्वारा इसी गौणार्थ 'प्रतिपादन ' का बोध होता है, उससे विशिष्ट प्रत्ययार्थ का बोध नहीं कराता । प्रतिपादित अर्थ को लक्षणा नहीं कहते हैं, प्रतिपादन ही लक्षणा है । यह दूसरा प्रश्न है कि वैयाकरण लोग क्रियापद में प्रकृत्यर्थ ( धात्वर्थ ) की ही प्रधानता मानते हैं तथा उस मत से 'प्रतिपादन' अर्थ गौण नहीं होगा । ]
[ अब यह कहा जा सकता है कि 'यत्तत्' शब्दों में एक ही अर्थ बतलाने का नियम है । यदि 'यत्' के द्वारा प्रतिपादन का अर्थबोध होता है तो 'तत्' के द्वारा भी वही काम होना चाहिए - फलतः 'तत् लक्षणा' कहना चाहिए, 'सा लक्षणा' ( स्त्रीलिङ्ग ) नहीं । इसका उत्तर देते हैं- ] ' सा लक्षणा' ( वह लक्षणा है ) यहाँ पर विधेय ( प्रतिनिर्दिश्यमान, Predicate ) के अनुसार तत् शब्द की स्त्रीलिङ्ग के रूप में सिद्धि होती है । [ 'सा' उद्देश्य है 'लक्षणा' विधेय । दोनों एक ही लिङ्ग में रहेंगे, अतः तत् का स्त्रीरूप 'सा' रखा गया है । ]
इसे कैट ने [ महाभाष्य के प्रथम आह्निक के आरम्भ में शब्द के स्वरूप- विचारवाले अंश की टीका करते हुए ] कहा है- 'उद्देश्य और विधेय दोनों में एकता का प्रदर्शन करने - वाले सर्वनाम ( यत्, तत् किम् आदि ) पर्याय अर्थात् विकल्प ( पारी - पारी) से किसी लिंग का ग्रहण करते हैं । [ महाभाष्य में वाक्य हैं - अथ गौरित्यत्र कः शब्दः ? किं यत्तत्सास्नालाङ्गूलककुदखुरविषाण्यर्थरूपं सः शब्दः । ' दूसरी पंक्ति की व्याख्या में ही कैयट का उक्त कथन है । जब यत् और तत् का सम्बन्ध नित्य है तब यत् को नपुंसकलिंग में और तत् को पुल्लिंग में ( स ) लिखना कहाँ तक ठीक है ? विधेय 'शब्द' है अतः उद्देश्य ( तत् ) पुल्लिंग में ही रखा गया है । यद्यपि 'तत्' शब्द उद्देश्य ( यत् ) का परामर्श करता है, किन्तु यह कोई जरूरी नहीं कि वह उद्देश्य के लिङ्ग के अनुसार चले । विधेय ( शब्द ) के लिङ्ग के अनुसार चलने पर भी कोई हानि नहीं । इसीलिए नागेश ने भी उदाहरण दिया है - शैत्यं हि यत्सा प्रकृतिर्जलस्य । अन्य उदाहरण - 'योऽसौ पुत्रः स रत्नम्' अथवा योऽसौ पुत्रः तद्रत्नम् ' | उसी प्रकार - 'यत् लक्ष्यते सा लक्षणा' । ]
तत्र 'कर्मणि कुशल:' इत्यादि रूढिलक्षणाया उदाहरणम् । कुशांल्लातीति व्युत्पत्त्या दर्भादानकर्तरि यौगिकं कुशलपदं विवेचकत्वसारूप्याप्रवीणे प्रवर्तमानमनादिवृद्धव्यवहारपरम्परानुपातित्वेन अभिधानवत्प्रयोजनमनपेक्ष्य प्रवर्तते । तदाह
निरूढा लक्षणाः काश्चित्सामर्थ्यादभिधानवत् ( त० वा० )
उनमें 'कर्म में कुशल है' इत्यादि रूढ़ि लक्षणा के उदाहरण हैं । [ द की ] व्युत्पत्ति होती है - कुश + V ला ( कुश लानेवाला ) । इससे यह यौगिक 'कुशल' शब्द दर्भ ( कुश ) लानेवाले के अर्थ में ( मुख्य अर्थ में ) रहकर भी विवेचक ( योग्य, विवेक्री )