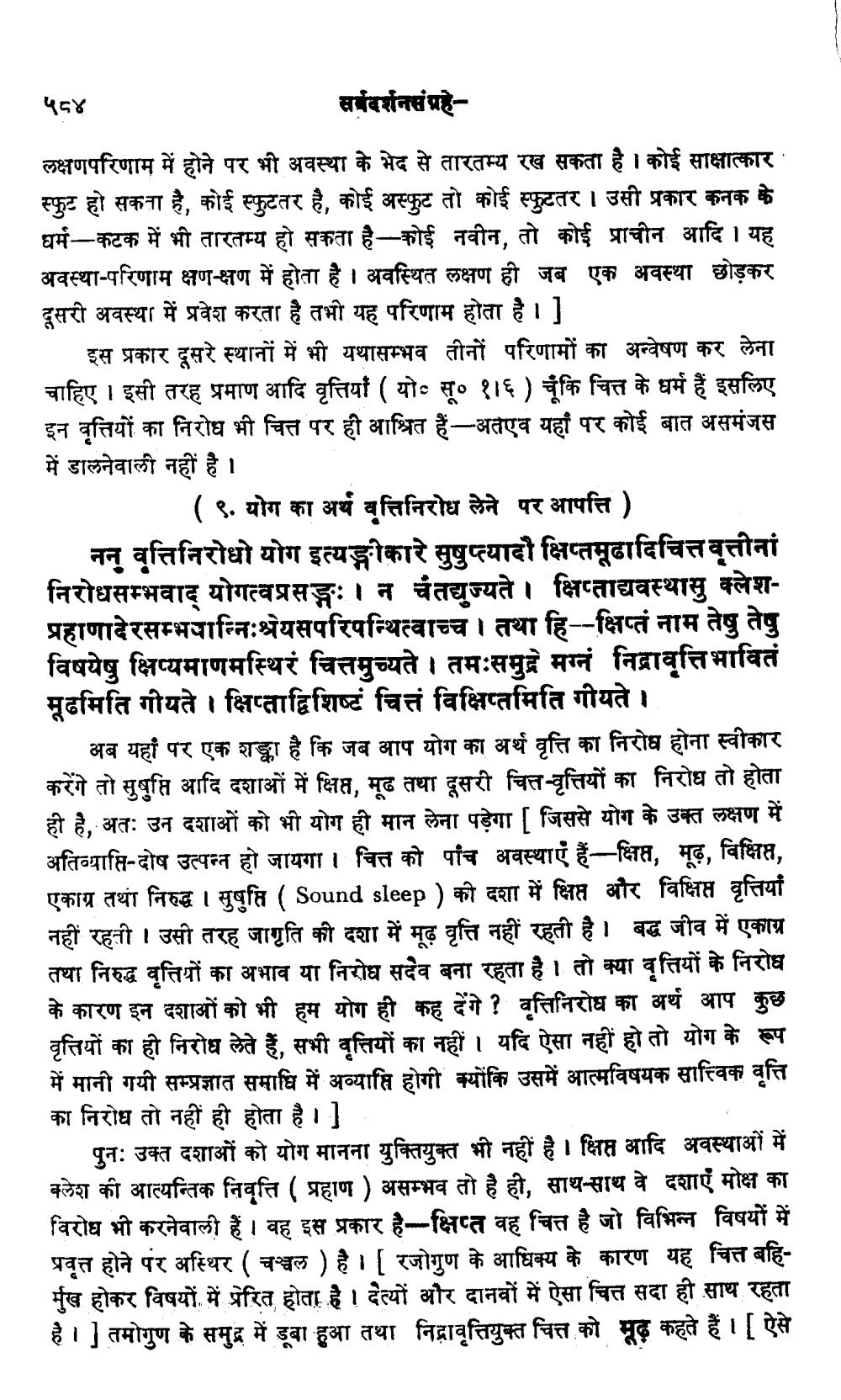________________
सर्वदर्शनसंग्रहे
लक्षणपरिणाम में होने पर भी अवस्था के भेद से तारतम्य रख सकता है । कोई साक्षात्कार स्फुट हो सकता है, कोई स्फुटतर है, कोई अस्फुट तो कोई स्फुटतर । उसी प्रकार कनक के धर्म - कटक में भी तारतम्य हो सकता है— कोई नवीन, तो कोई प्राचीन आदि । यह अवस्था - परिणाम क्षण-क्षण में होता है । अवस्थित लक्षण ही जब एक अवस्था छोड़कर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तभी यह परिणाम होता है । ]
इस प्रकार दूसरे स्थानों में भी यथासम्भव तीनों परिणामों का अन्वेषण कर लेना चाहिए । इसी तरह प्रमाण आदि वृत्तियाँ ( यो सू० ११६ ) चूंकि चित्त के धर्म हैं इसलिए इन वृत्तियों का निरोध भी चित्त पर ही आश्रित हैं - अतएव यहां पर कोई बात असमंजस में डालनेवाली नहीं है ।
( ९. योग का अर्थ वृत्तिनिरोध लेने पर आपत्ति )
ननु वृत्तिनिरोधो योग इत्यङ्गीकारे सुषुप्त्यादौ क्षिप्तमूढादिचित्तवृत्तीनां निरोधसम्भवाद् योगत्वप्रसङ्गः । न चैतद्युज्यते । क्षिप्ताद्यवस्थासु क्लेशप्रहाणादेरसम्भवान्निःश्रेयसपरिपन्थित्वाच्च । तथा हि--क्षिप्तं नाम तेषु तेषु विषयेषु क्षिप्यमाणमस्थिरं चित्तमुच्यते । तमः समुद्रे मग्नं निद्रावृत्तिभावितं मूढमिति गीयते । क्षिप्ताद्विशिष्टं चित्तं विक्षिप्तमिति गीयते ।
५८४
अब यहाँ पर एक शङ्का है कि जब आप योग का अर्थ वृत्ति का निरोध होना स्वीकार करेंगे तो सुषुप्ति आदि दशाओं में क्षिप्त, मूढ तथा दूसरी चित्त वृत्तियों का निरोध तो होता ही है, अतः उन दशाओं को भी योग ही मान लेना पड़ेगा [ जिससे योग के उक्त लक्षण में अतिव्याप्ति - दोष उत्पन्न हो जायगा । चित्त को पांच अवस्थाएं हैं- क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरुद्ध । सुषुप्ति ( Sound sleep ) की दशा में क्षिप्त और विक्षिप्त वृत्तियाँ नहीं रहती । उसी तरह जागृति की दशा में मूढ़ वृत्ति नहीं रहती है । बद्ध जीव में एकाग्र तथा निरुद्ध वृत्तियों का अभाव या निरोध सदेव बना रहता है । तो क्या वृत्तियों के निरोध के कारण इन दशाओं को भी हम योग ही कह देंगे ? वृत्तिनिरोध का अर्थ आप कुछ वृत्तियों का ही निरोध लेते हैं, सभी वृत्तियों का नहीं । यदि ऐसा नहीं हो तो योग के रूप में मानी गयी सम्प्रज्ञात समाधि में अव्याप्ति होगी क्योंकि उसमें आत्मविषयक सात्त्विक वृत्ति का निरोध तो नहीं ही होता है । ]
पुनः उक्त दशाओं को योग मानना युक्तियुक्त भी नहीं है । क्षिप्त आदि अवस्थाओं में क्लेश की आत्यन्तिक निवृत्ति ( प्रहाण ) असम्भव तो है ही, साथ-साथ वे दशाएं मोक्ष का विरोध भी करनेवाली हैं । वह इस प्रकार है - क्षिप्त वह चित्त है जो विभिन्न विषयों में प्रवृत्त होने पर अस्थिर ( चञ्चल ) है । [ रजोगुण के आधिक्य के कारण यह चित्त बहिर्मुख होकर विषयों में प्रेरित होता है । देत्यों और दानवों में ऐसा चित्त सदा ही साथ रहता है । ] तमोगुण के समुद्र में डूबा हुआ तथा निद्रावृत्तियुक्त चित्त को मूढ़ कहते हैं । [ ऐसे