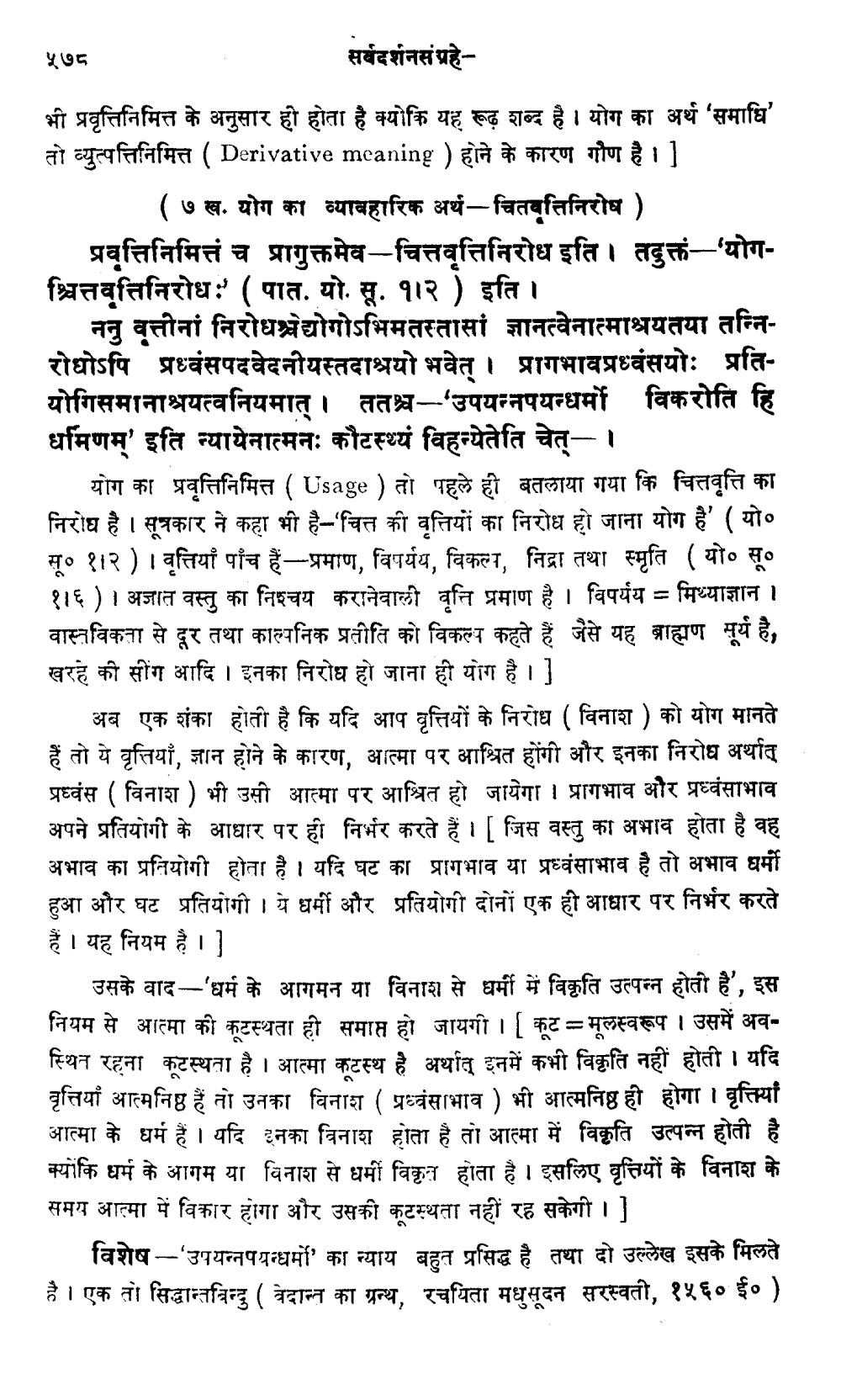________________
५७८
सर्वदर्शनसंग्रहे
भी प्रवृत्तिनिमित्त के अनुसार ही होता है क्योकि यह रूढ शब्द है । योग का अर्थ 'समाधि' तो व्युत्पत्तिनिमित्त ( Derivative meaning ) होने के कारण गौण है। ]
( ७ ख. योग का व्यावहारिक अर्थ-चितवृत्तिनिरोध ) प्रवृत्तिनिमित्तं च प्रागुक्तमेव-चित्तवृत्तिनिरोध इति। तदुक्तं-'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: ( पात. यो. सू. १२ ) इति ।
ननु वृत्तीनां निरोधश्चेद्योगोऽभिमतस्तासां ज्ञानत्वेनात्माश्रयतया तन्निरोधोऽपि प्रध्वंसपदवेदनीयस्तदाश्रयो भवेत् । प्रागभावप्रध्वंसयोः प्रतियोगिसमानाश्रयत्वनियमात् । ततश्च-'उपयन्नपयन्धर्मो विकरोति हि धर्मिणम्' इति न्यायेनात्मनः कौटस्थ्यं विहन्येतेति चेत् । __ योग का प्रवृत्तिनिमित्त ( Usage ) तो पहले ही बतलाया गया कि चित्तवृत्ति का निरोध है । सूत्रकार ने कहा भी है-'चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है' ( यो० सू० ११२ ) । वृत्तियाँ पाँच हैं-प्रमाण, विपर्यय, विकल, निद्रा तथा स्मृति ( यो० सू० ११६ )। अजात वस्तु का निश्चय करानेवाली वृत्ति प्रमाण है । विपर्यय = मिथ्याज्ञान । वास्तविकता से दूर तथा काल्पनिक प्रतीति को विकल्प कहते हैं जैसे यह ब्राह्मण सूर्य है, खरहे की सींग आदि । इनका निरोध हो जाना ही योग है। ]
अब एक शंका होती है कि यदि आप वृत्तियों के निरोध ( विनाश ) को योग मानते हैं तो ये वृत्तियाँ, ज्ञान होने के कारण, आत्मा पर आश्रित होंगी और इनका निरोध अर्थात् प्रध्वंस ( विनाश ) भी उसी आत्मा पर आश्रित हो जायेगा। प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव अपने प्रतियोगी के आधार पर ही निर्भर करते हैं । [ जिस वस्तु का अभाव होता है वह अभाव का प्रतियोगी होता है। यदि घट का प्रागभाव या प्रध्वंसाभाव है तो अभाव धर्मो हुआ और घट प्रतियोगी । ये धर्मी और प्रतियोगी दोनों एक ही आधार पर निर्भर करते हैं । यह नियम है । ]
उसके बाद-'धर्म के आगमन या विनाश से धर्मी में विकृति उत्पन्न होती है', इस नियम से आत्मा की कूटस्थता ही समाप्त हो जायगी। [ कूट = मूलस्वरूप । उसमें अवस्थित रहना कूटस्थता है । आत्मा कटस्थ है अर्थात् इनमें कभी विकृति नहीं होती। यदि वृत्तियाँ आत्मनिष्ठ हैं तो उनका विनाश ( प्रध्वंसाभाव ) भी आत्मनिष्ठ ही होगा । वृत्तियां आत्मा के धर्म हैं । यदि इनका विनाश होता है तो आत्मा में विकृति उत्पन्न होती है क्योंकि धर्म के आगम या विनाश से धर्मी विकृत होता है। इसलिए वृत्तियों के विनाश के समय आत्मा में विकार होगा और उसकी कूटस्थता नहीं रह सकेगी।]
विशेष –'उपयन्नपयन्धर्मो' का न्याय बहुत प्रसिद्ध है तथा दो उल्लेख इसके मिलते है। एक तो सिद्धान्तबिन्दु ( वेदान्त का ग्रन्थ, रचयिता मधुसूदन सरस्वती, १५६० ई० )