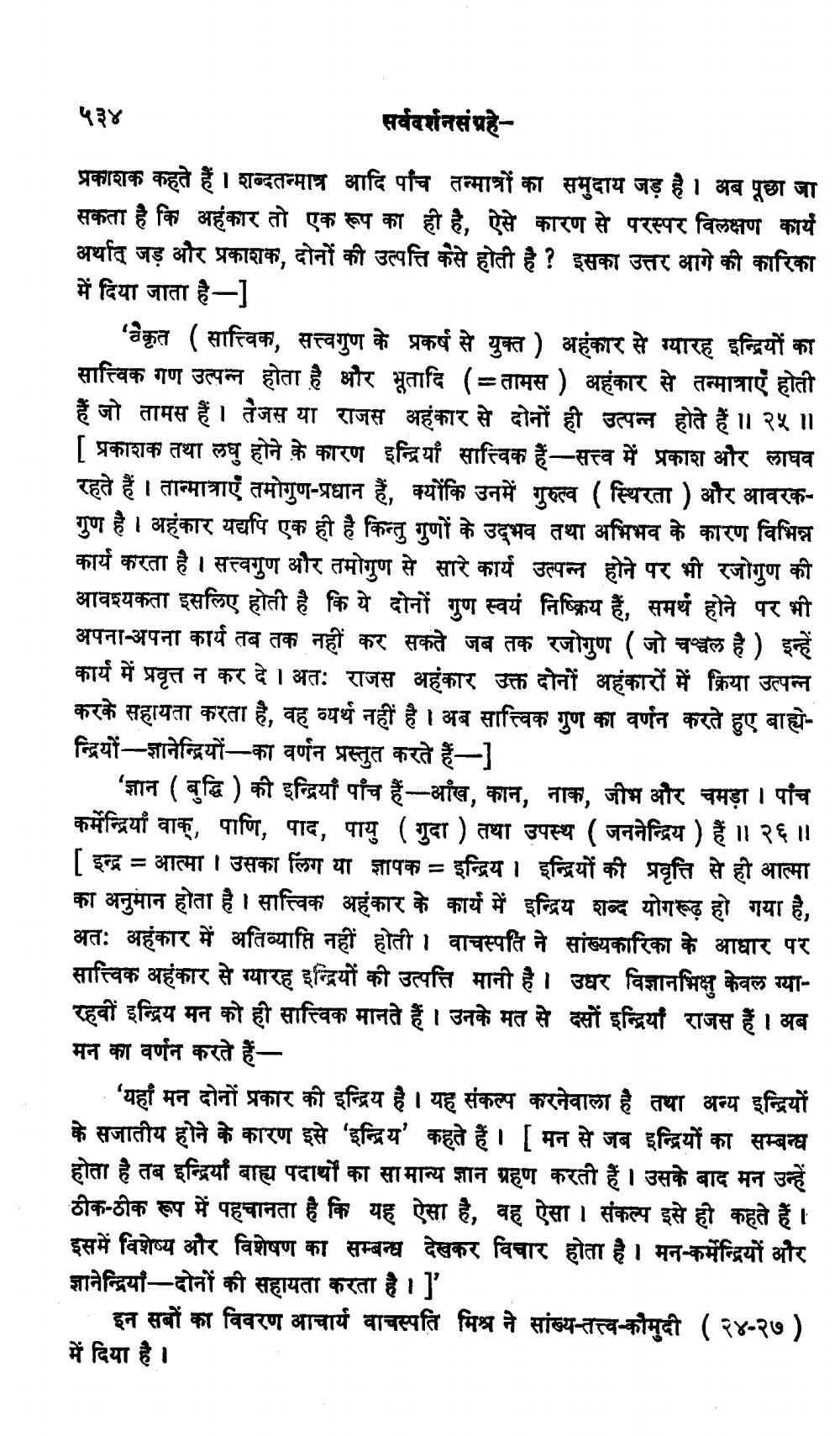________________
५३४
सर्वदर्शनसंग्रहे
प्रकाशक कहते हैं । शब्दतन्मात्र आदि पाँच तन्मात्रों का समुदाय जड़ है । अब पूछा जा सकता है कि अहंकार तो एक रूप का ही है, ऐसे कारण से परस्पर विलक्षण कार्य अर्थात् जड़ और प्रकाशक, दोनों की उत्पत्ति कैसे होती है ? इसका उत्तर आगे की कारिका में दिया जाता है - ]
'वैकृत ( सात्त्विक, सत्त्वगुण के प्रकर्ष से युक्त ) अहंकार से ग्यारह इन्द्रियों का सात्त्विक गण उत्पन्न होता है और भूतादि ( = तामस ) अहंकार से तन्मात्राएं होती हैं जो तामस हैं । तेजस या राजस अहंकार से दोनों ही उत्पन्न होते हैं ॥ २५ ॥ [ प्रकाशक तथा लघु होने के कारण इन्द्रियां सात्त्विक हैं-सत्त्व में प्रकाश और लाघव रहते हैं । तान्मात्राएं तमोगुण प्रधान हैं, क्योंकि उनमें गुरुत्व ( स्थिरता ) और आवरकगुण है । अहंकार यद्यपि एक ही है किन्तु गुणों के उद्भव तथा अभिभव के कारण विभिन्न कार्य करता है । सत्त्वगुण और तमोगुण से सारे कार्य उत्पन्न होने पर भी रजोगुण की आवश्यकता इसलिए होती है कि ये दोनों गुण स्वयं निष्क्रिय हैं, समर्थ होने पर भी अपना-अपना कार्य तब तक नहीं कर सकते जब तक रजोगुण ( जो चञ्चल है ) इन्हें कार्य में प्रवृत्त न कर दे । अतः राजस अहंकार उक्त दोनों अहंकारों में क्रिया उत्पन्न करके सहायता करता है, वह व्यर्थ नहीं है । अब सात्त्विक गुण का वर्णन करते हुए बाह्येन्द्रियों-ज्ञानेन्द्रियों- - का वर्णन प्रस्तुत करते हैं - ]
'ज्ञान ( बुद्धि ) की इन्द्रियाँ पांच हैं - आंख, कान, नाक, जीभ और चमड़ा | पाँच कर्मेन्द्रियां वाक् पाणि, पाद, पायु ( गुदा ) तथा उपस्थ ( जननेन्द्रिय ) हैं ॥ २६ ॥ [ इन्द्र = आत्मा । उसका लिंग या ज्ञापक = इन्द्रिय । इन्द्रियों की प्रवृत्ति से ही आत्मा का अनुमान होता है । सात्त्विक अहंकार के कार्य में इन्द्रिय शब्द योगरूढ़ हो गया है, अतः अहंकार में अतिव्याप्ति नहीं होती । वाचस्पति ने सांख्यकारिका के आधार पर सात्त्विक अहंकार से ग्यारह इन्द्रियों की उत्पत्ति मानी है। उधर विज्ञानभिक्षु केवल ग्यारहवीं इन्द्रिय मन को ही सात्त्विक मानते हैं । उनके मत से दसों इन्द्रियाँ राजस हैं । अब मन का वर्णन करते हैं
'यहाँ मन दोनों प्रकार की इन्द्रिय है । यह संकल्प करनेवाला है तथा अन्य इन्द्रियों के सजातीय होने के कारण इसे 'इन्द्रिय' कहते हैं । [ मन से जब इन्द्रियों का सम्बन्ध होता है तब इन्द्रियाँ बाह्य पदार्थों का सामान्य ज्ञान ग्रहण करती हैं । उसके बाद मन उन्हें ठीक-ठीक रूप में पहचानता है कि यह ऐसा है, वह ऐसा । संकल्प इसे ही कहते हैं । इसमें विशेष्य और विशेषण का सम्बन्ध देखकर विचार होता है । मन - कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियां - दोनों की सहायता करता है । ] '
इन सबों का विवरण आचार्य वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्त्व -कौमुदी ( २४-२७ ) में दिया है ।