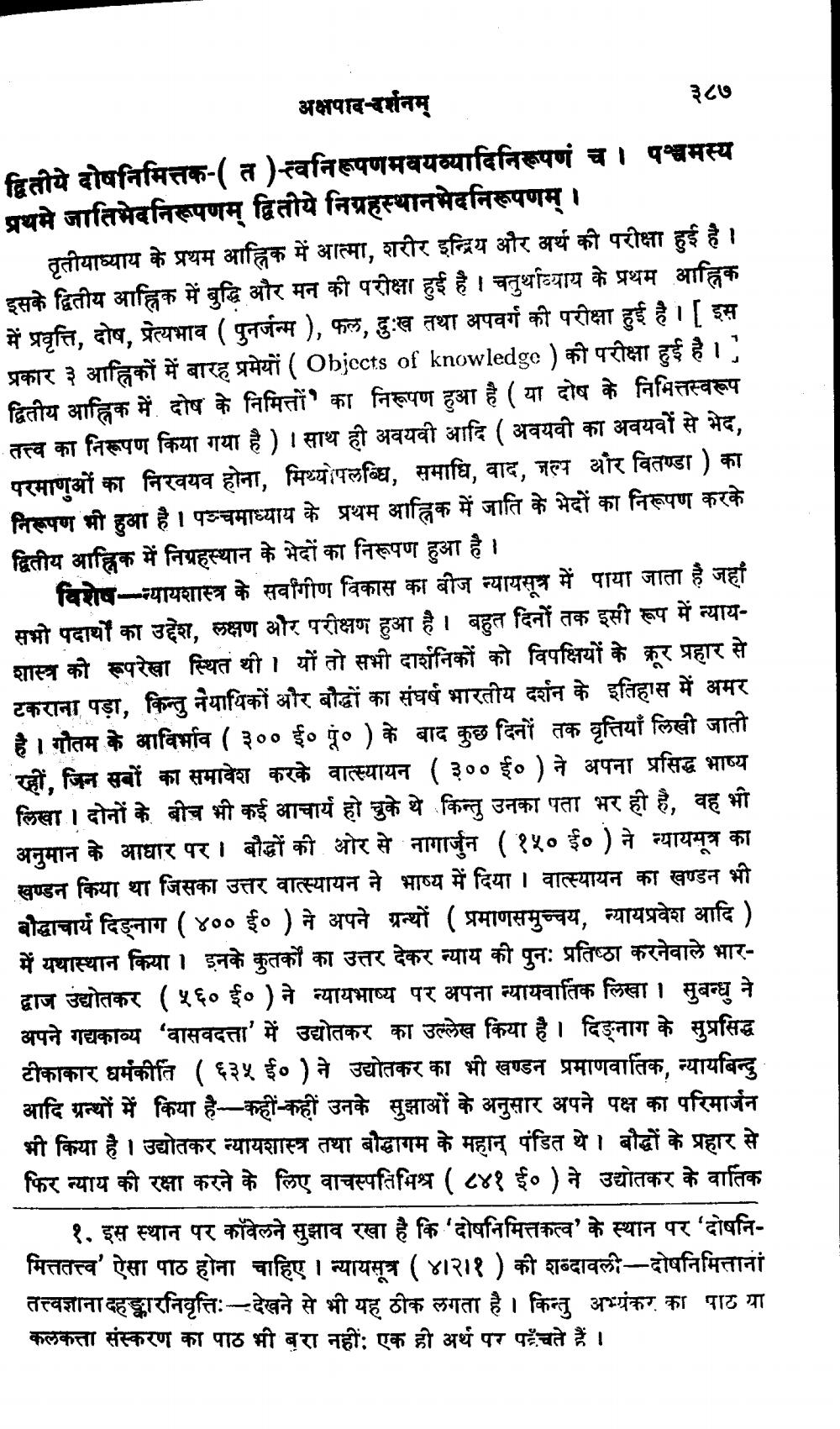________________
अक्षपाद - दर्शनम्
३८७
द्वितीये दोषनिमित्तक - ( त ) - त्वनिरूपणमवयव्यादिनिरूपणं च । पश्वमस्य प्रथमे जातिभेदनिरूपणम् द्वितीये निग्रहस्थानभेदनिरूपणम् ।
J
तृतीयाध्याय के प्रथम आह्निक में आत्मा, शरीर इन्द्रिय और अर्थ की परीक्षा हुई है । इसके द्वितीय आह्निक में बुद्धि और मन की परीक्षा हुई है। चतुर्थाध्याय के प्रथम आह्निक प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव ( पुनर्जन्म ), फल, दुःख तथा अपवर्ग की परीक्षा हुई है । [ इस प्रकार ३ आह्निकों में बारह प्रमेयों ( Objects of knowledge ) की परीक्षा हुई है । द्वितीय आह्निक में दोष के निमित्तों' का निरूपण हुआ है ( या दोष के निमित्तस्वरूप तत्त्व का निरूपण किया गया है ) । साथ ही अवयवी आदि ( अवयवी का अवयवों से भेद, परमाणुओं का निरवयव होना, मिथ्योपलब्धि, समाधि, वाद, जल्प और वितण्डा ) का निरूपण भी हुआ है । पञ्चमाध्याय के प्रथम आह्निक में जाति के भेदों का निरूपण करके द्वितीय आह्निक में निग्रहस्थान के भेदों का निरूपण हुआ है ।
विशेष न्यायशास्त्र के सर्वांगीण विकास का बीज न्यायसूत्र में पाया जाता है जहाँ सभी पदार्थों का उद्देश, लक्षण और परीक्षण हुआ है । बहुत दिनों तक इसी रूप में न्यायशास्त्र को रूपरेखा स्थित थी । यों तो सभी दार्शनिकों को विपक्षियों के क्रूर प्रहार से टकराना पड़ा, किन्तु नैयायिकों और बौद्धों का संघर्ष भारतीय दर्शन के इतिहास में अमर है । गौतम के आविर्भाव ( ३०० ई० पू० ) के बाद कुछ दिनों तक वृत्तियाँ लिखी जाती रहीं, जिन सबों का समावेश करके वात्स्यायन ( ३०० ई० ) ने अपना प्रसिद्ध भाष्य लिखा । दोनों के बीच भी कई आचार्य हो चुके थे किन्तु उनका पता भर ही है, वह भी अनुमान के आधार पर । बौद्धों की ओर से नागार्जुन ( १५० ई० ) ने न्यायसूत्र का ause किया था जिसका उत्तर वात्स्यायन ने भाष्य में दिया । वात्स्यायन का खण्डन भी बौद्धाचार्य दिङ्नाग ( ४०० ई० ) ने अपने ग्रन्थों ( प्रमाणसमुच्चय, न्यायप्रवेश आदि ) में यथास्थान किया । इनके कुतर्कों का उत्तर देकर न्याय की पुनः प्रतिष्ठा करनेवाले भारने द्वाज उद्योतकर ( ५६० ई० ) ने न्यायभाष्य पर अपना न्यायवार्तिक लिखा । सुबन्धु अपने गद्यकाव्य ' वासवदत्ता' में उद्योतकर का उल्लेख किया है । दिङ्नाग के सुप्रसिद्ध टीकाकार धर्मकीर्ति ( ६३५ ई० ) ने उद्योतकर का भी खण्डन प्रमाणवार्तिक, न्यायबिन्दु आदि ग्रन्थों में किया है--कहीं कहीं उनके सुझाओं के अनुसार अपने पक्ष का परिमार्जन भी किया है । उद्योतकर न्यायशास्त्र तथा बौद्धागम के महान् पंडित थे । बौद्धों के प्रहार से फिर न्याय की रक्षा करने के लिए वाचस्पतिमिश्र ( ८४१ ई० ) ने उद्योतकर के वार्तिक
१. इस स्थान पर कॉवेलने सुझाव रखा है कि 'दोषनिमित्तकत्व' के स्थान पर 'दोषनिमित्ततत्त्व' ऐसा पाठ होना चाहिए । न्यायसूत्र ( ४।२।१ ) की शब्दावली - दोषनिमित्तानां तत्त्वज्ञाना दहङ्कारनिवृत्तिः - देखने से भी यह ठीक लगता है । किन्तु अभ्यंकर का पाठ या कलकत्ता संस्करण का पाठ भी बरा नहीं: एक ही अर्थ पर पहुँचते हैं ।