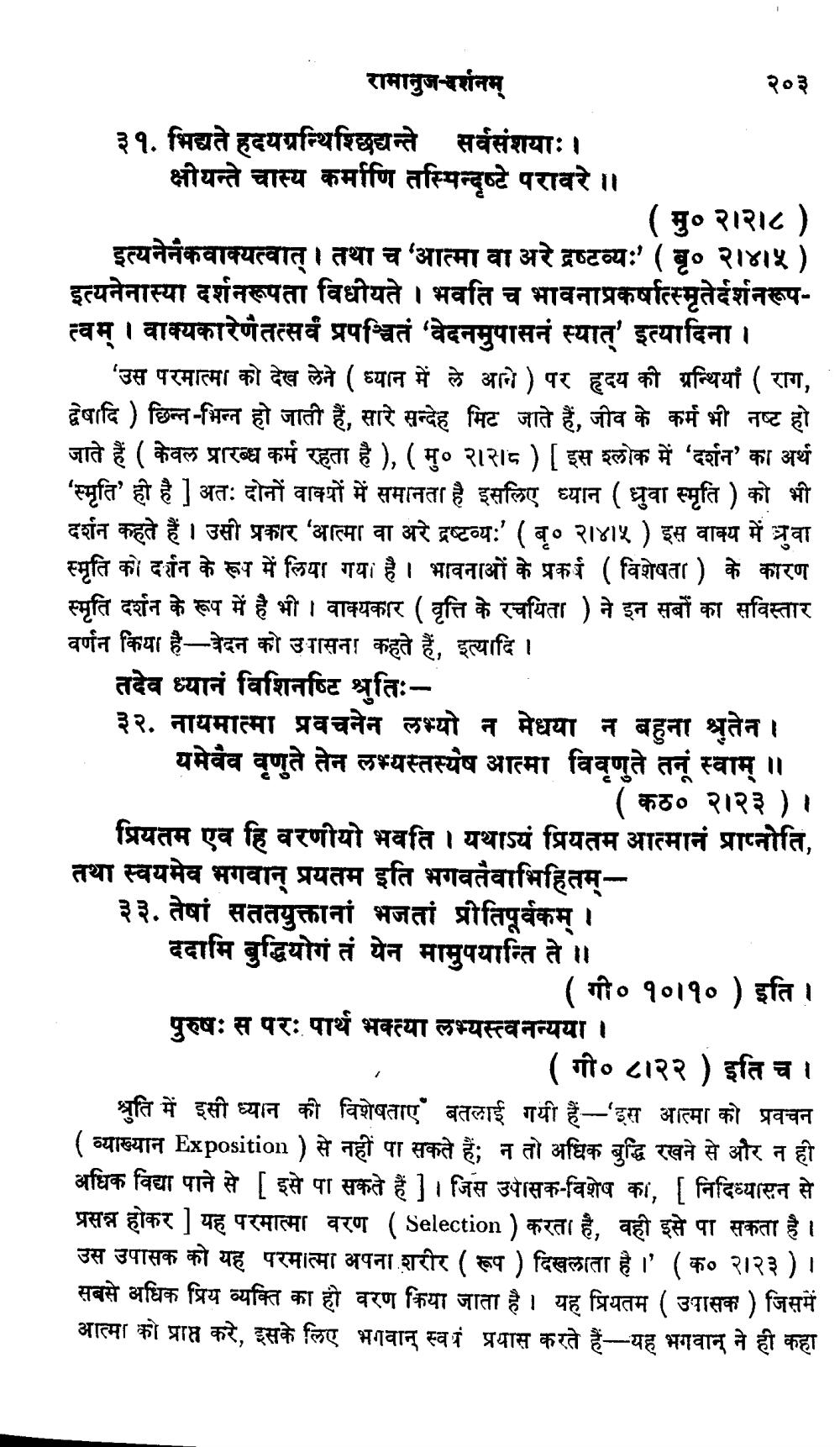________________
रामानुज-दर्शनम् ३१. भिद्यते हदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥
(मु० २।२।८) इत्यनेनंकवाक्यत्वात् । तथा च 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः' (बृ० २।४।५) इत्यनेनास्या दर्शनरूपता विधीयते । भवति च भावनाप्रकर्षात्स्मृतेर्दर्शनरूपत्वम् । वाक्यकारेणैतत्सर्वं प्रपञ्चितं 'वेदनमुपासनं स्यात्' इत्यादिना ।
'उस परमात्मा को देख लेने ( ध्यान में ले आने) पर हृदय की ग्रन्थियाँ ( राग, द्वेषादि ) छिन्न-भिन्न हो जाती हैं, सारे सन्देह मिट जाते हैं, जीव के कर्म भी नष्ट हो जाते हैं ( केवल प्रारब्ध कर्म रहता है ), (मु० २।२।८ ) [ इस श्लोक में 'दर्शन' का अर्थ 'स्मृति' ही है ] अतः दोनों वाक्यों में समानता है इसलिए ध्यान (ध्रुवा स्मृति ) को भी दर्शन कहते हैं । उसी प्रकार 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः' (बृ० २।४।५) इस वाक्य में त्रुवा स्मृति को दर्शन के रूप में लिया गया है। भावनाओं के प्रकर्ष (विशेषता ) के कारण स्मृति दर्शन के रूप में है भी । वाक्यकार ( वृत्ति के रचयिता ) ने इन सबों का सविस्तार वर्णन किया है-वेदन को आसना कहते हैं, इत्यादि ।
तदेव ध्यानं विशिनष्टि श्रुतिः३२. नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । यमेवैव वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम् ॥
(कठ० २।२३ )। प्रियतम एव हि वरणीयो भवति । यथाऽयं प्रियतम आत्मानं प्राप्नोति, तथा स्वयमेव भगवान् प्रयतम इति भगवतैवाभिहितम्३३. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥
( गी० १०।१० ) इति । पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ।
(गी० ८।२२ ) इति च । श्रुति में इसी ध्यान की विशेषताएं बतलाई गयी हैं-'इस आत्मा को प्रवचन ( व्याख्यान Exposition ) से नहीं पा सकते हैं; न तो अधिक बुद्धि रखने से और न ही अधिक विद्या पाने से [ इसे पा सकते हैं ] । जिस उपासक-विशेष का, [ निदिध्यासन से प्रसन्न होकर ] यह परमात्मा वरण ( Selection ) करता है, वही इसे पा सकता है। उस उपासक को यह परमात्मा अपना शरीर ( रूप ) दिखलाता है ।' (क० २।२३ ) । सबसे अधिक प्रिय व्यक्ति का हो वरण किया जाता है। यह प्रियतम ( उपासक ) जिसमें आत्मा को प्राप्त करे, इसके लिए भगवान् स्वयं प्रयास करते हैं-यह भगवान् ने ही कहा