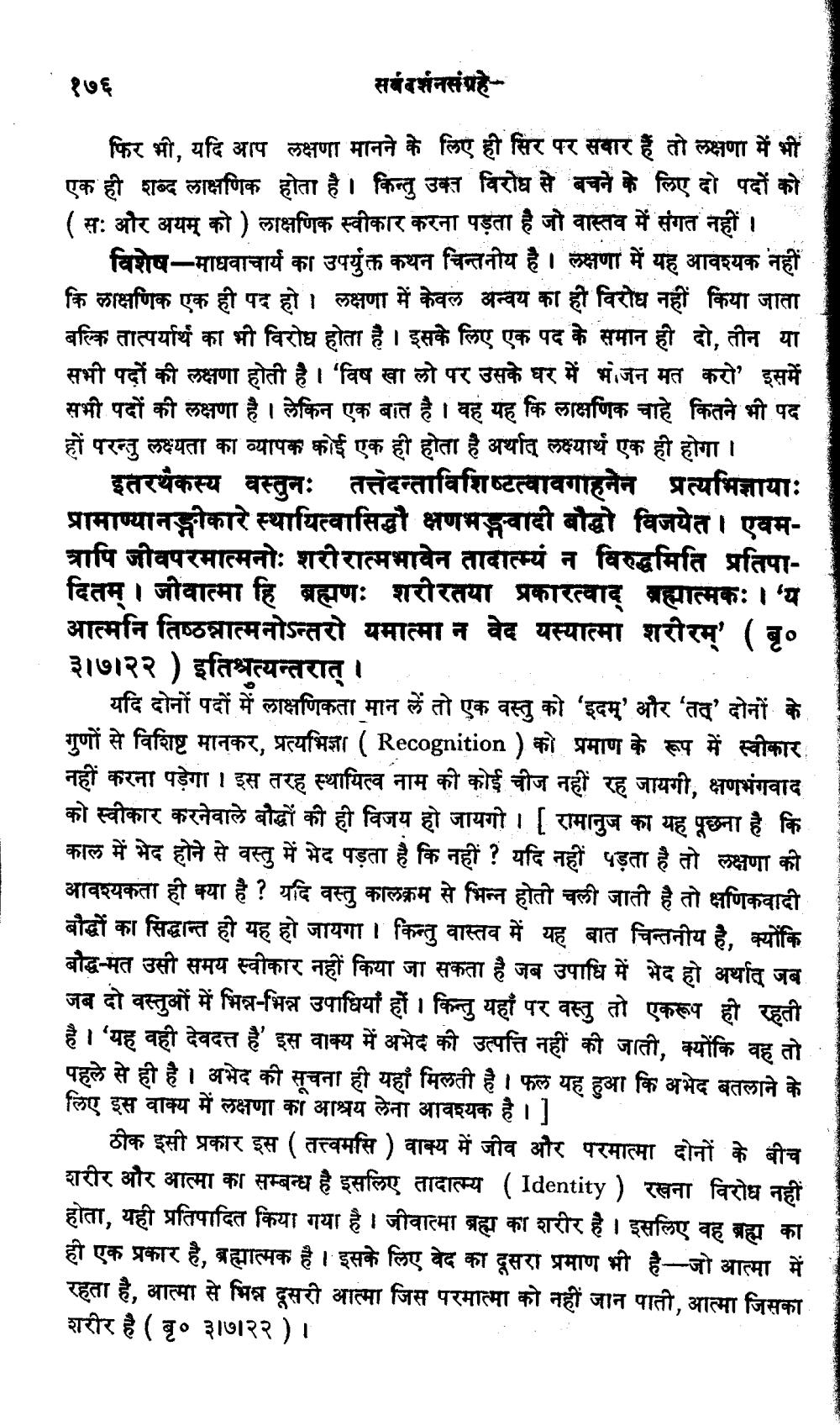________________
सर्वदर्शनसंग्रहे
फिर भी, यदि आप लक्षणा मानने के लिए ही सिर पर सवार हैं तो लक्षणा में भी एक ही शब्द लाक्षणिक होता है । किन्तु उक्त विरोध से बचने के लिए दो पदों को ( स: और अयम् को ) लाक्षणिक स्वीकार करना पड़ता है जो वास्तव में संगत नहीं ।
विशेष - माधवाचार्य का उपर्युक्त कथन चिन्तनीय है। लक्षणा में यह आवश्यक नहीं faraणक एक ही पद हो । लक्षणा में केवल अन्वय का ही विरोध नहीं किया जाता बल्कि तात्पर्यार्थं का भी विरोध होता है। इसके लिए एक पद के समान ही दो, तीन या सभी पदों की लक्षणा होती है । 'विष खा लो पर उसके घर में भोजन मत करो' इसमें सभी पदों की लक्षणा है । लेकिन एक बात है । वह यह कि लाक्षणिक चाहे कितने भी पद हों परन्तु लक्ष्यता का व्यापक कोई एक ही होता है अर्थात् लक्ष्यार्थं एक ही होगा ।
इतरथैकस्य वस्तुनः तत्तेदन्ताविशिष्टत्वावगाहनेन प्रत्यभिज्ञायाः प्रामाण्यानङ्गीकारे स्थायित्वासिद्धौ क्षणभङ्गवादी बौद्धो विजयेत। एवमत्रापि जीवपरमात्मनोः शरीरात्मभावेन तादात्म्यं न विरुद्धमिति प्रतिपा दितम् । जीवात्मा हि ब्रह्मणः शरीरतया प्रकारत्वाद् ब्रह्मात्मकः । 'य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्' ( बृ० ३।७।२२ ) इतिश्रुत्यन्तरात् ।
१७६
यदि दोनों पदों में लाक्षणिकता मान लें तो एक वस्तु को 'इदम्' और 'तत्' दोनों के गुणों से विशिष्ट मानकर, प्रत्यभिज्ञा ( Recognition ) को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करना पड़ेगा । इस तरह स्थायित्व नाम की कोई चीज नहीं रह जायगी, क्षणभंगवाद को स्वीकार करनेवाले बौद्धों की ही विजय हो जायगी । [ रामानुज का यह पूछना है कि काल में भेद होने से वस्तु में भेद पड़ता है कि नहीं ? यदि नहीं पड़ता है तो लक्षणा की आवश्यकता ही क्या है ? यदि वस्तु कालक्रम से भिन्न होती चली जाती है तो क्षणिकवादी
का सिद्धान्त हो यह हो जायगा । किन्तु वास्तव में यह बात चिन्तनीय है, क्योंकि बौद्ध-मत उसी समय स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब उपाधि में भेद हो अर्थात् जब जब दो वस्तुओं में भिन्न-भिन्न उपाधियाँ हों । किन्तु यहाँ पर वस्तु तो एकरूप ही रहती है । 'यह वही देवदत्त है' इस वाक्य में अभेद की उत्पत्ति नहीं की जाती, क्योंकि वह तो पहले से ही है । अभेद की सूचना ही यहाँ मिलती है । फल यह हुआ कि अभेद बतलाने के लिए इस वाक्य में लक्षणा का आश्रय लेना आवश्यक है । ]
ठीक इसी प्रकार इस ( तत्त्वमसि ) वाक्य में जीव और परमात्मा दोनों के बीच शरीर और आत्मा का सम्बन्ध है इसलिए तादात्म्य ( Identity ) रखना विरोध नहीं होता, यही प्रतिपादित किया गया है। जीवात्मा ब्रह्म का शरीर है । इसलिए वह ब्रह्म का ही एक प्रकार है, ब्रह्मात्मक है । इसके लिए वेद का दूसरा प्रमाण भी है— जो आत्मा में रहता है, आत्मा से भिन्न दूसरी आत्मा जिस परमात्मा को नहीं जान पाती, आत्मा जिसका शरीर है ( बृ० ३।७।२२ ) ।