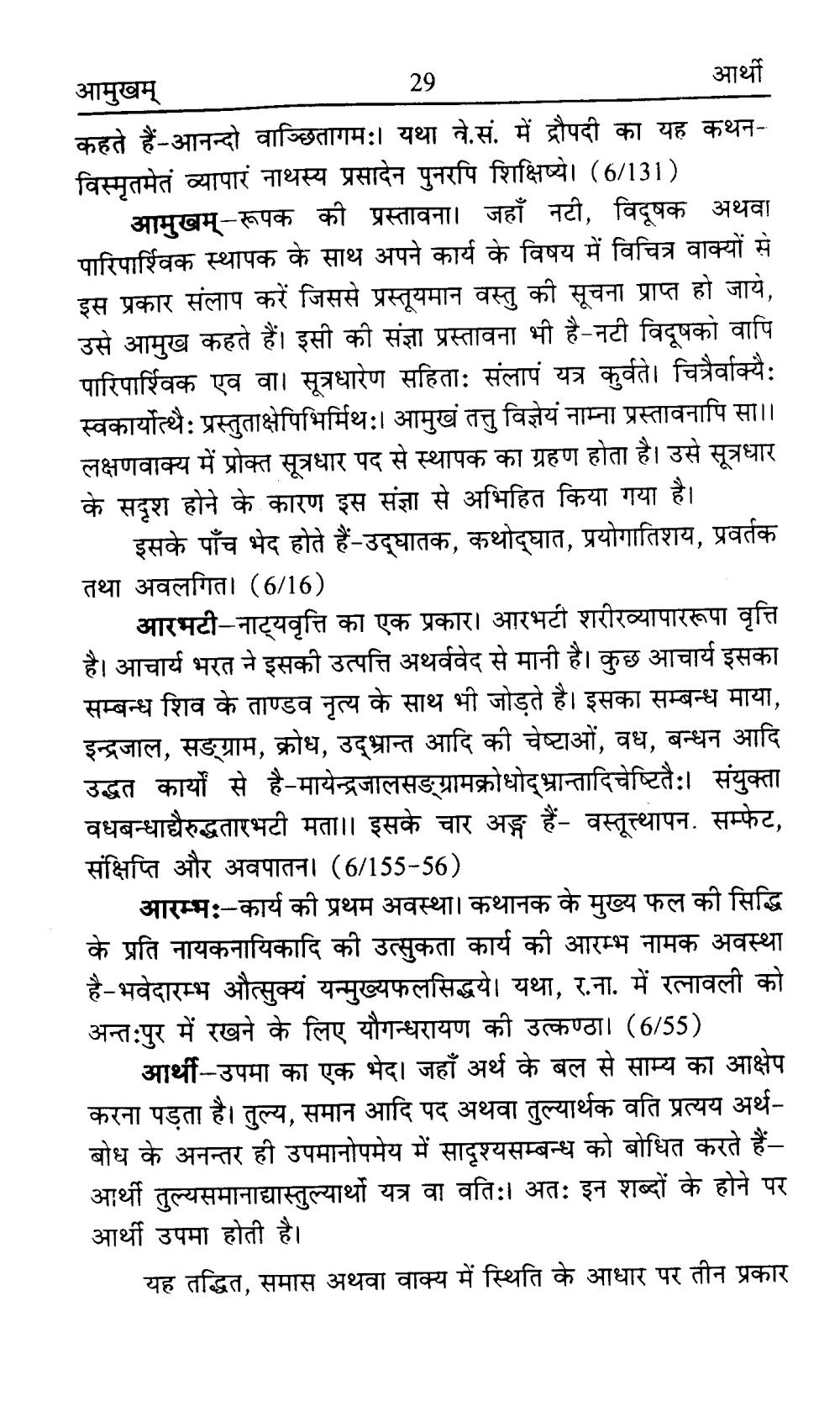________________
29
आमुखम्
आर्थी कहते हैं-आनन्दो वाञ्छितागमः। यथा वे.सं. में द्रौपदी का यह कथनविस्मृतमेतं व्यापारं नाथस्य प्रसादेन पुनरपि शिक्षिष्ये। (6/131)
आमुखम्-रूपक की प्रस्तावना। जहाँ नटी, विदूषक अथवा पारिपाश्विक स्थापक के साथ अपने कार्य के विषय में विचित्र वाक्यों से इस प्रकार संलाप करें जिससे प्रस्तूयमान वस्तु की सूचना प्राप्त हो जाये, उसे आमुख कहते हैं। इसी की संज्ञा प्रस्तावना भी है-नटी विदूषको वापि पारिपाश्विक एव वा। सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुर्वते। चित्रैर्वाक्यैः स्वकार्योत्थैः प्रस्तुताक्षेपिभिर्मिथः। आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा।। लक्षणवाक्य में प्रोक्त सूत्रधार पद से स्थापक का ग्रहण होता है। उसे सूत्रधार के सदृश होने के कारण इस संज्ञा से अभिहित किया गया है।
इसके पाँच भेद होते हैं-उद्घातक, कथोद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवर्तक तथा अवलगित। (6/16) ____ आरभटी-नाट्यवृत्ति का एक प्रकार। आरभटी शरीरव्यापाररूपा वृत्ति है। आचार्य भरत ने इसकी उत्पत्ति अथर्ववेद से मानी है। कुछ आचार्य इसका सम्बन्ध शिव के ताण्डव नृत्य के साथ भी जोड़ते है। इसका सम्बन्ध माया, इन्द्रजाल, सङ्ग्राम, क्रोध, उद्भ्रान्त आदि की चेष्टाओं, वध, बन्धन आदि उद्धत कार्यों से है-मायेन्द्रजालसङ्ग्रामक्रोधोद्भ्रान्तादिचेष्टितैः। संयुक्ता वधबन्धाद्यैरुद्धतारभटी मता।। इसके चार अङ्ग हैं- वस्तूत्त्थापन. सम्फेट, संक्षिप्ति और अवपातन। (6/155-56) ____ आरम्भ:-कार्य की प्रथम अवस्था। कथानक के मुख्य फल की सिद्धि के प्रति नायकनायिकादि की उत्सुकता कार्य की आरम्भ नामक अवस्था है-भवेदारम्भ औत्सुक्यं यन्मुख्यफलसिद्धये। यथा, र.ना. में रत्नावली को अन्तःपुर में रखने के लिए यौगन्धरायण की उत्कण्ठा। (6/55)
आर्थी-उपमा का एक भेद। जहाँ अर्थ के बल से साम्य का आक्षेप करना पड़ता है। तुल्य, समान आदि पद अथवा तुल्यार्थक वति प्रत्यय अर्थबोध के अनन्तर ही उपमानोपमेय में सादृश्यसम्बन्ध को बोधित करते हैंआर्थी तुल्यसमानाद्यास्तुल्यार्थी यत्र वा वतिः। अत: इन शब्दों के होने पर आर्थी उपमा होती है।
यह तद्धित, समास अथवा वाक्य में स्थिति के आधार पर तीन प्रकार