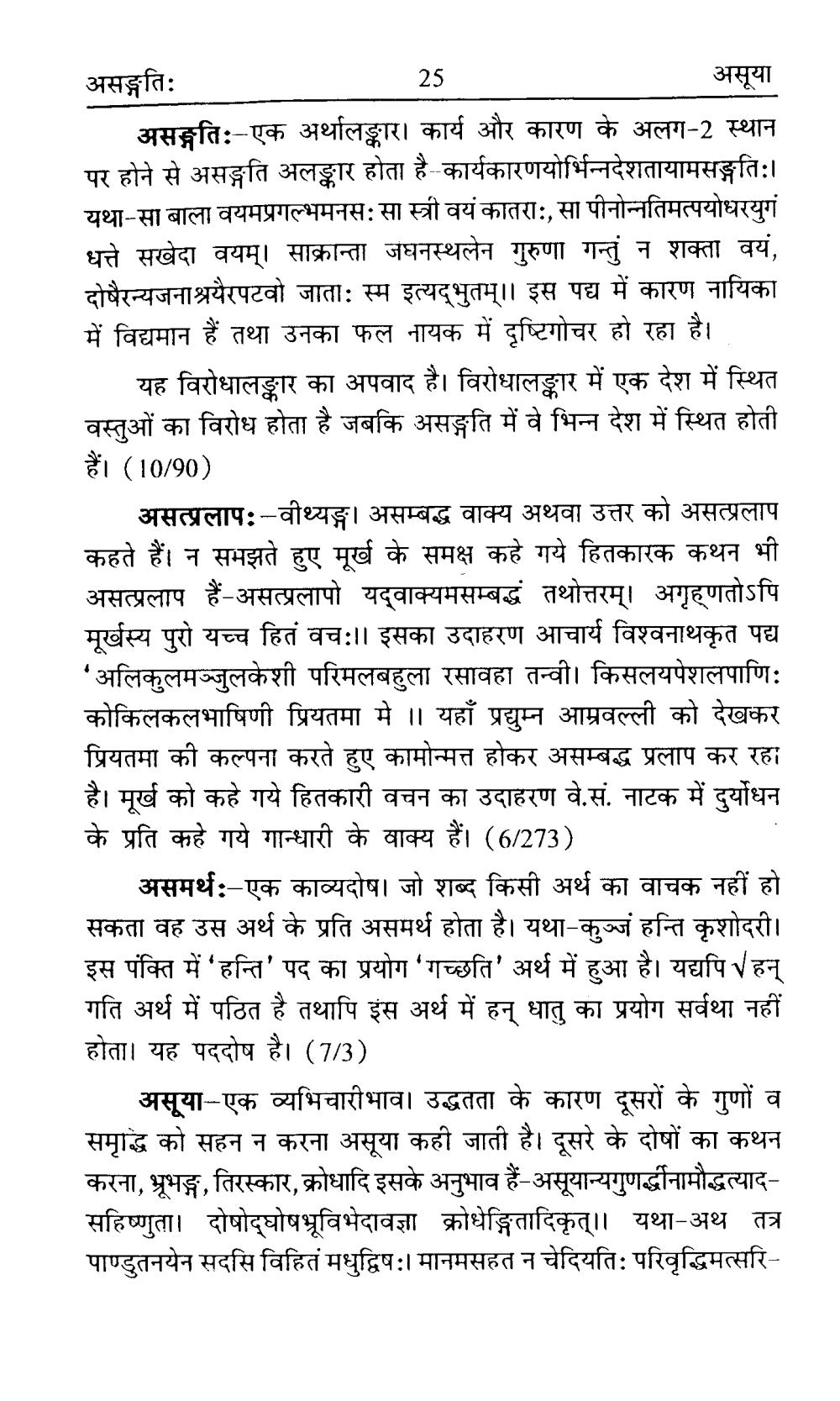________________
25
असूया
असङ्गतिः
असङ्गतिः-एक अर्थालङ्कार। कार्य और कारण के अलग-2 स्थान पर होने से असङ्गति अलङ्कार होता है- कार्यकारणयोर्भिन्नदेशतायामसङ्गतिः। यथा-सा बाला वयमप्रगल्भमनसः सा स्त्री वयं कातराः, सा पीनोन्नतिमत्पयोधरयुगं धत्ते सखेदा वयम्। साक्रान्ता जघनस्थलेन गुरुणा गन्तुं न शक्ता वयं, दोषैरन्यजनाश्रयैरपटवो जाताः स्म इत्यद्भुतम्।। इस पद्य में कारण नायिका में विद्यमान हैं तथा उनका फल नायक में दृष्टिगोचर हो रहा है।
यह विरोधालङ्कार का अपवाद है। विरोधालङ्कार में एक देश में स्थित वस्तुओं का विरोध होता है जबकि असङ्गति में वे भिन्न देश में स्थित होती हैं। (10/90)
असत्प्रलापः-वीथ्यङ्ग। असम्बद्ध वाक्य अथवा उत्तर को असत्प्रलाप कहते हैं। न समझते हुए मूर्ख के समक्ष कहे गये हितकारक कथन भी असत्प्रलाप हैं-असत्प्रलापो यद्वाक्यमसम्बद्धं तथोत्तरम्। अगृह्णतोऽपि मूर्खस्य पुरो यच्च हितं वचः।। इसका उदाहरण आचार्य विश्वनाथकृत पद्य 'अलिकुलमञ्जुलकेशी परिमलबहुला रसावहा तन्वी। किसलयपेशलपाणिः कोकिलकलभाषिणी प्रियतमा मे ।। यहाँ प्रद्युम्न आम्रवल्ली को देखकर प्रियतमा की कल्पना करते हुए कामोन्मत्त होकर असम्बद्ध प्रलाप कर रहा है। मूर्ख को कहे गये हितकारी वचन का उदाहरण वे.सं. नाटक में दुर्योधन के प्रति कहे गये गान्धारी के वाक्य हैं। (6/273) ___असमर्थः-एक काव्यदोष। जो शब्द किसी अर्थ का वाचक नहीं हो सकता वह उस अर्थ के प्रति असमर्थ होता है। यथा-कुशं हन्ति कृशोदरी। इस पंक्ति में 'हन्ति' पद का प्रयोग 'गच्छति' अर्थ में हुआ है। यद्यपि । हन् गति अर्थ में पठित है तथापि इस अर्थ में हन् धातु का प्रयोग सर्वथा नहीं होता। यह पददोष है। (7/3)
असूया-एक व्यभिचारीभाव। उद्धतता के कारण दूसरों के गुणों व समृद्धि को सहन न करना असूया कही जाती है। दूसरे के दोषों का कथन करना, भ्रूभङ्ग, तिरस्कार, क्रोधादि इसके अनुभाव हैं-असूयान्यगुणर्झनामौद्धत्यादसहिष्णुता। दोषोद्घोषभ्रूविभेदावज्ञा क्रोधेङ्गितादिकृत्।। यथा-अथ तत्र पाण्डुतनयेन सदसि विहितं मधुद्विषः। मानमसहत न चेदियतिः परिवृद्धिमत्सरि