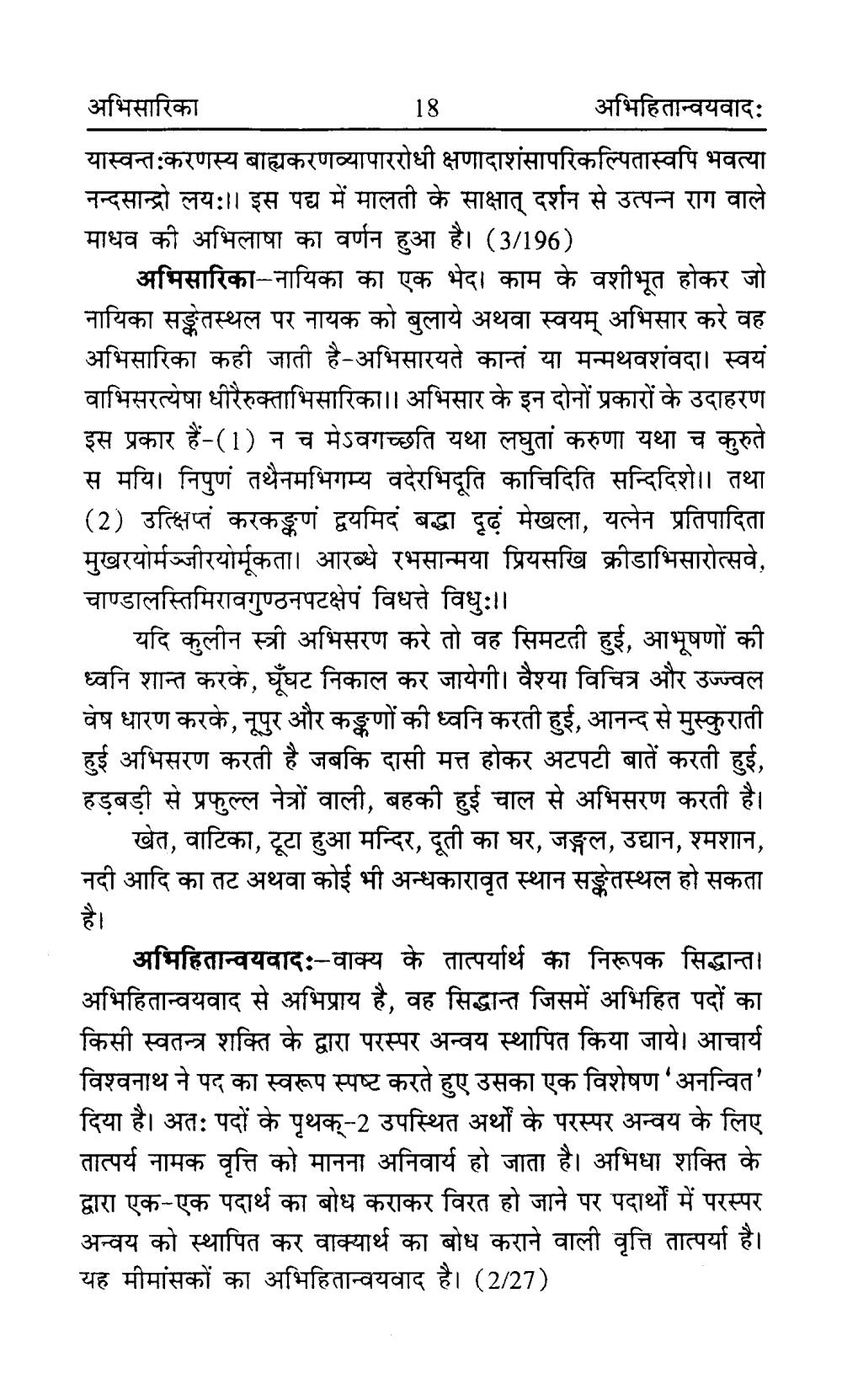________________
___
18
अभिसारिका
अभिहितान्वयवादः यास्वन्त:करणस्य बाह्यकरणव्यापाररोधी क्षणादाशंसापरिकल्पितास्वपि भवत्या नन्दसान्द्रो लयः।। इस पद्य में मालती के साक्षात् दर्शन से उत्पन्न राग वाले माधव की अभिलाषा का वर्णन हुआ है। (3/196) ___ अभिसारिका-नायिका का एक भेद। काम के वशीभूत होकर जो नायिका सङ्केतस्थल पर नायक को बुलाये अथवा स्वयम् अभिसार करे वह अभिसारिका कही जाती है-अभिसारयते कान्तं या मन्मथवशंवदा। स्वयं वाभिसरत्येषा धीरैरुक्ताभिसारिका।। अभिसार के इन दोनों प्रकारों के उदाहरण इस प्रकार हैं-(1) न च मेऽवगच्छति यथा लघुतां करुणा यथा च कुरुते स मयि। निपुणं तथैनमभिगम्य वदेरभिदूति काचिदिति सन्दिदिशे।। तथा (2) उत्क्षिप्तं करकङ्कणं द्वयमिदं बद्धा दृढं मेखला, यत्नेन प्रतिपादिता मुखरयोर्मञ्जीरयोर्मूकता। आरब्धे रभसान्मया प्रियसखि क्रीडाभिसारोत्सवे, चाण्डालस्तिमिरावगुण्ठनपटक्षेपं विधत्ते विधुः।। ___यदि कुलीन स्त्री अभिसरण करे तो वह सिमटती हुई, आभूषणों की ध्वनि शान्त करके, चूंघट निकाल कर जायेगी। वैश्या विचित्र और उज्ज्वल वेष धारण करके, नूपुर और कङ्कणों की ध्वनि करती हुई, आनन्द से मुस्कुराती हुई अभिसरण करती है जबकि दासी मत्त होकर अटपटी बातें करती हुई, हड़बड़ी से प्रफुल्ल नेत्रों वाली, बहकी हुई चाल से अभिसरण करती है।
खेत, वाटिका, टूटा हुआ मन्दिर, दूती का घर, जङ्गल, उद्यान, श्मशान, नदी आदि का तट अथवा कोई भी अन्धकारावृत स्थान सङ्केतस्थल हो सकता
है।
अभिहितान्वयवादः-वाक्य के तात्पर्यार्थ का निरूपक सिद्धान्त। अभिहितान्वयवाद से अभिप्राय है, वह सिद्धान्त जिसमें अभिहित पदों का किसी स्वतन्त्र शक्ति के द्वारा परस्पर अन्वय स्थापित किया जाये। आचार्य विश्वनाथ ने पद का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसका एक विशेषण 'अनन्वित' दिया है। अतः पदों के पृथक्-2 उपस्थित अर्थों के परस्पर अन्वय के लिए तात्पर्य नामक वृत्ति को मानना अनिवार्य हो जाता है। अभिधा शक्ति के द्वारा एक-एक पदार्थ का बोध कराकर विरत हो जाने पर पदार्थों में परस्पर अन्वय को स्थापित कर वाक्यार्थ का बोध कराने वाली वृत्ति तात्पर्या है। यह मीमांसकों का अभिहितान्वयवाद है। (2/27)