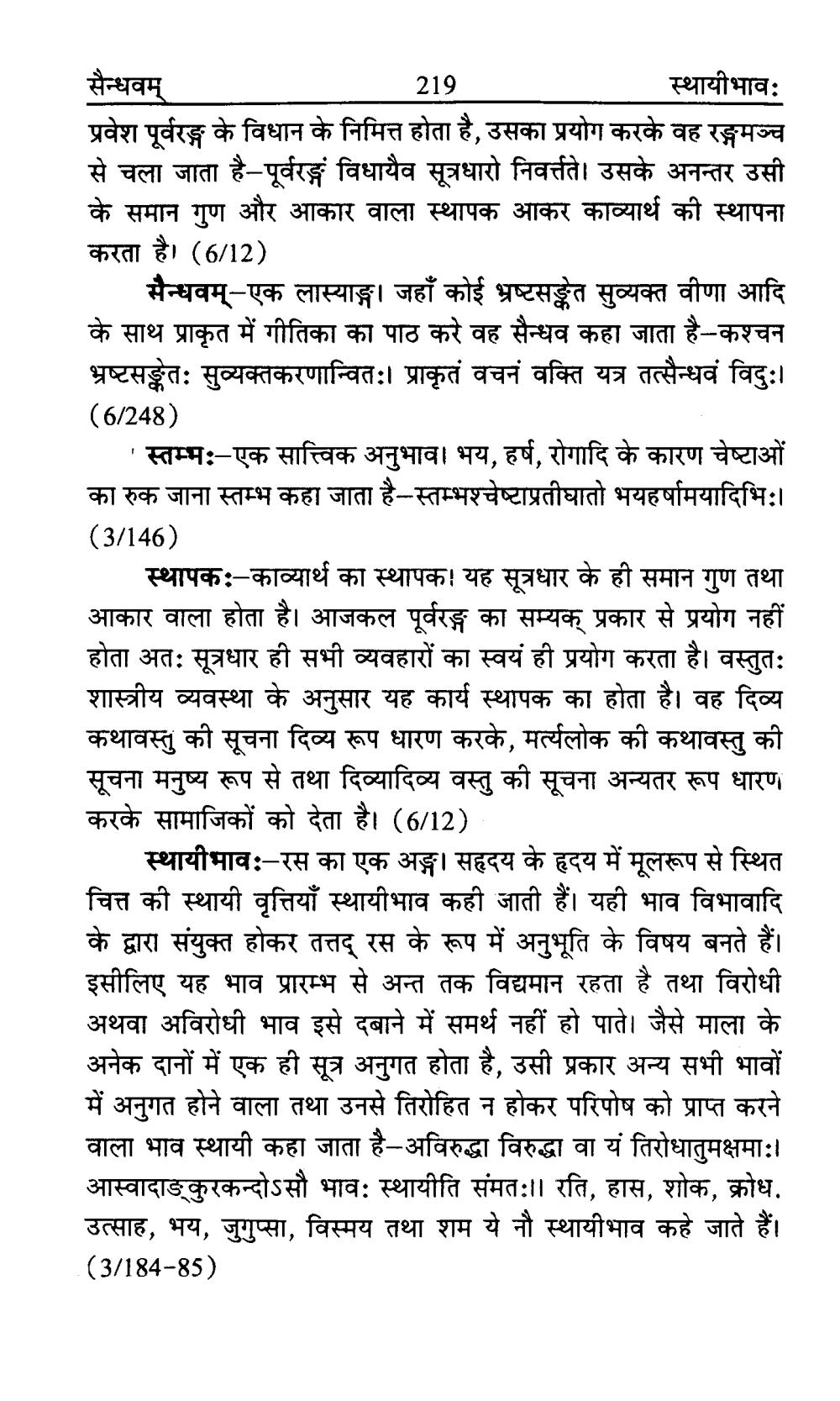________________
सैन्धवम्
219
__ स्थायीभावः प्रवेश पूर्वरङ्ग के विधान के निमित्त होता है, उसका प्रयोग करके वह रङ्गमञ्च से चला जाता है-पूर्वरङ्ग विधायैव सूत्रधारो निवर्त्तते। उसके अनन्तर उसी के समान गुण और आकार वाला स्थापक आकर काव्यार्थ की स्थापना करता है। (6/12)
मैन्धवम्-एक लास्याङ्ग। जहाँ कोई भ्रष्टसङ्केत सुव्यक्त वीणा आदि के साथ प्राकृत में गीतिका का पाठ करे वह सैन्धव कहा जाता है-कश्चन भ्रष्टसङ्केतः सुव्यक्तकरणान्वितः। प्राकृतं वचनं वक्ति यत्र तत्सैन्धवं विदुः। (6/248)
' स्तम्भ:-एक सात्त्विक अनुभाव। भय, हर्ष, रोगादि के कारण चेष्टाओं का रुक जाना स्तम्भ कहा जाता है-स्तम्भश्चेष्टाप्रतीघातो भयहर्षामयादिभिः। (3/146)
स्थापक:-काव्यार्थ का स्थापक। यह सूत्रधार के ही समान गुण तथा आकार वाला होता है। आजकल पूर्वरङ्ग का सम्यक् प्रकार से प्रयोग नहीं होता अतः सूत्रधार ही सभी व्यवहारों का स्वयं ही प्रयोग करता है। वस्तुतः शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार यह कार्य स्थापक का होता है। वह दिव्य कथावस्तु की सूचना दिव्य रूप धारण करके, मर्त्यलोक की कथावस्तु की सूचना मनुष्य रूप से तथा दिव्यादिव्य वस्तु की सूचना अन्यतर रूप धारण करके सामाजिकों को देता है। (6/12)
स्थायीभावः-रस का एक अङ्ग। सहृदय के हृदय में मूलरूप से स्थित चित्त की स्थायी वृत्तियाँ स्थायीभाव कही जाती हैं। यही भाव विभावादि के द्वारा संयुक्त होकर तत्तद् रस के रूप में अनुभूति के विषय बनते हैं। इसीलिए यह भाव प्रारम्भ से अन्त तक विद्यमान रहता है तथा विरोधी अथवा अविरोधी भाव इसे दबाने में समर्थ नहीं हो पाते। जैसे माला के अनेक दानों में एक ही सूत्र अनुगत होता है, उसी प्रकार अन्य सभी भावों में अनुगत होने वाला तथा उनसे तिरोहित न होकर परिपोष को प्राप्त करने वाला भाव स्थायी कहा जाता है-अविरुद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमाः। आस्वादाङ्कुरकन्दोऽसौ भावः स्थायीति संमतः।। रति, हास, शोक, क्रोध. उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय तथा शम ये नौ स्थायीभाव कहे जाते हैं। (3/184-85)