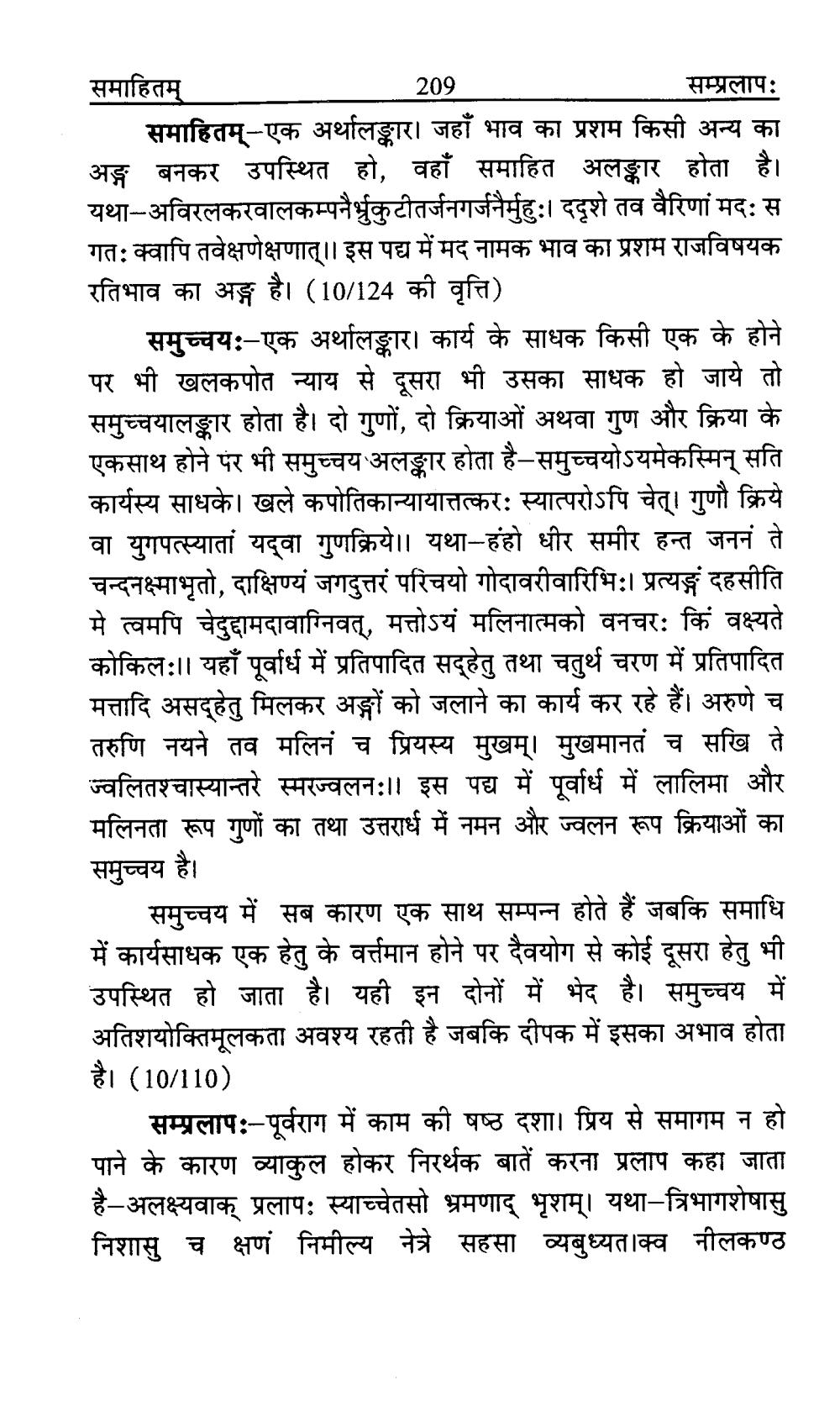________________
209
सम्प्रलाप:
समाहितम्
समाहितम्-एक अर्थालङ्कार। जहाँ भाव का प्रशम किसी अन्य का अङ्ग बनकर उपस्थित हो, वहाँ समाहित अलङ्कार होता है। यथा-अविरलकरवालकम्पनैर्भुकुटीतर्जनगर्जनैर्मुहुः। ददृशे तव वैरिणां मदः स गत: क्वापि तवेक्षणेक्षणात्।। इस पद्य में मद नामक भाव का प्रशम राजविषयक रतिभाव का अङ्ग है। (10/124 की वृत्ति)
समुच्चयः-एक अर्थालङ्कार। कार्य के साधक किसी एक के होने पर भी खलकपोत न्याय से दूसरा भी उसका साधक हो जाये तो समुच्चयालङ्कार होता है। दो गुणों, दो क्रियाओं अथवा गुण और क्रिया के एकसाथ होने पर भी समुच्चय अलङ्कार होता है-समुच्चयोऽयमेकस्मिन् सति कार्यस्य साधके। खले कपोतिकान्यायात्तत्कर: स्यात्परोऽपि चेत्। गुणौ क्रिये वा युगपत्स्यातां यद्वा गुणक्रिये।। यथा-हहो धीर समीर हन्त जननं ते चन्दनक्ष्माभृतो, दाक्षिण्यं जगदुत्तरं परिचयो गोदावरीवारिभिः। प्रत्यङ्गं दहसीति मे त्वमपि चेदुद्दामदावाग्निवत्, मत्तोऽयं मलिनात्मको वनचरः किं वक्ष्यते कोकिलः।। यहाँ पूर्वार्ध में प्रतिपादित सद्हेतु तथा चतुर्थ चरण में प्रतिपादित मत्तादि असद्हेतु मिलकर अङ्गों को जलाने का कार्य कर रहे हैं। अरुणे च तरुणि नयने तव मलिनं च प्रियस्य मुखम्। मुखमानतं च सखि ते ज्वलितश्चास्यान्तरे स्मरज्वलनः।। इस पद्य में पूर्वार्ध में लालिमा और मलिनता रूप गुणों का तथा उत्तरार्ध में नमन और ज्वलन रूप क्रियाओं का समुच्चय है।
समुच्चय में सब कारण एक साथ सम्पन्न होते हैं जबकि समाधि में कार्यसाधक एक हेतु के वर्तमान होने पर दैवयोग से कोई दूसरा हेतु भी उपस्थित हो जाता है। यही इन दोनों में भेद है। समुच्चय में अतिशयोक्तिमूलकता अवश्य रहती है जबकि दीपक में इसका अभाव होता है। (10/110)
सम्प्रलाप:-पूर्वराग में काम की षष्ठ दशा। प्रिय से समागम न हो पाने के कारण व्याकुल होकर निरर्थक बातें करना प्रलाप कहा जाता है-अलक्ष्यवाक् प्रलापः स्याच्चेतसो भ्रमणाद् भृशम्। यथा-त्रिभागशेषासु निशासु च क्षणं निमील्य नेत्रे सहसा व्यबुध्यत।क्व नीलकण्ठ