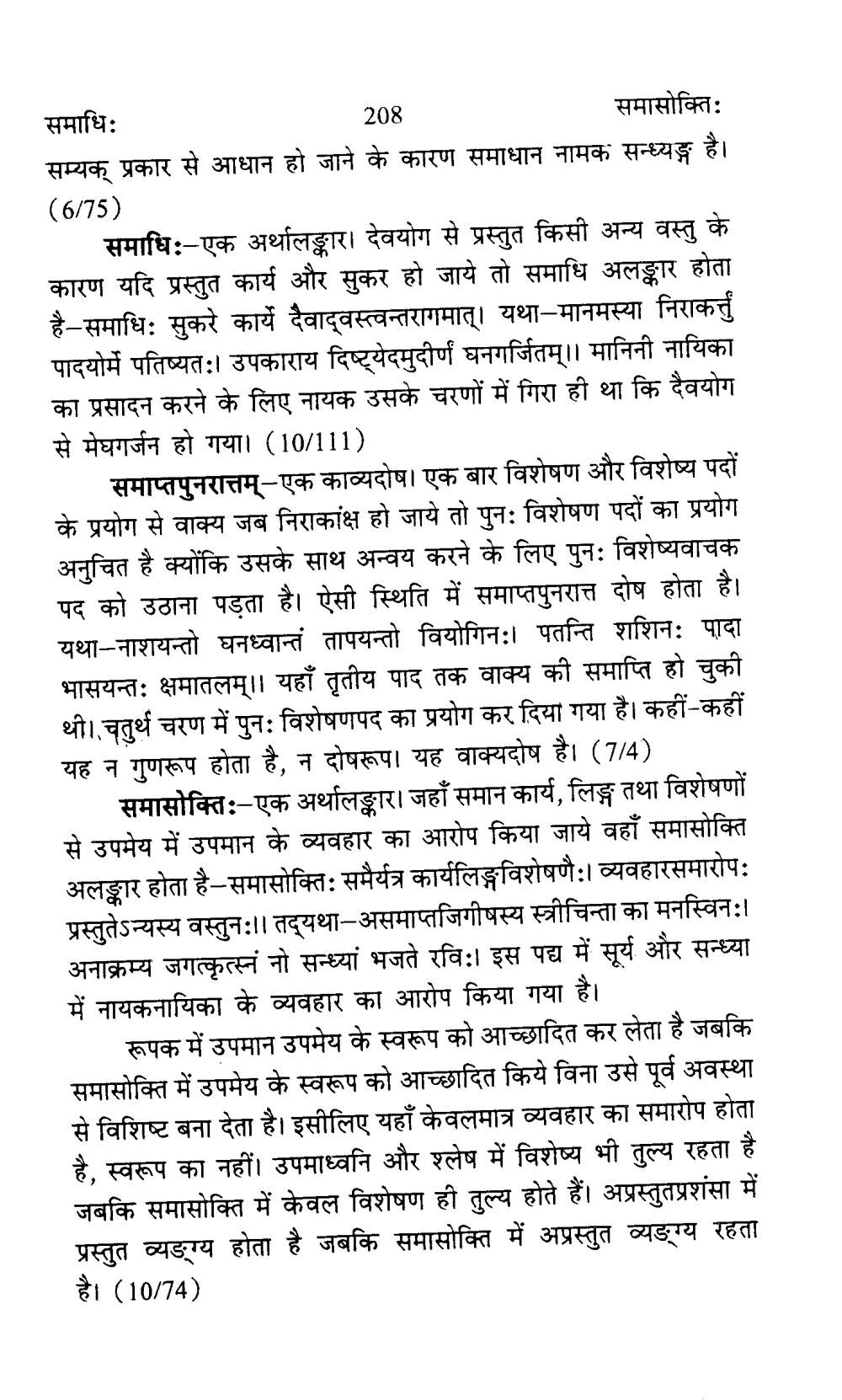________________
समाधिः
208
समासोक्तिः सम्यक् प्रकार से आधान हो जाने के कारण समाधान नामक सन्ध्यङ्ग है। (6/75)
समाधिः-एक अर्थालङ्कार। देवयोग से प्रस्तुत किसी अन्य वस्तु के कारण यदि प्रस्तुत कार्य और सुकर हो जाये तो समाधि अलङ्कार होता है-समाधिः सुकरे कार्ये दैवाद्वस्त्वन्तरागमात्। यथा-मानमस्या निराकर्तुं पादयोर्मे पतिष्यतः। उपकाराय दिष्ट्येदमुदीर्णं घनगर्जितम्।। मानिनी नायिका का प्रसादन करने के लिए नायक उसके चरणों में गिरा ही था कि दैवयोग से मेघगर्जन हो गया। (10/111)
समाप्तपुनरात्तम्-एक काव्यदोष। एक बार विशेषण और विशेष्य पदों के प्रयोग से वाक्य जब निराकांक्ष हो जाये तो पुनः विशेषण पदों का प्रयोग अनुचित है क्योंकि उसके साथ अन्वय करने के लिए पुनः विशेष्यवाचक पद को उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में समाप्तपुनरात्त दोष होता है। यथा-नाशयन्तो घनध्वान्तं तापयन्तो वियोगिनः। पतन्ति शशिनः पादा भासयन्तः क्षमातलम्।। यहाँ तृतीय पाद तक वाक्य की समाप्ति हो चुकी थी। चतुर्थ चरण में पुनः विशेषणपद का प्रयोग कर दिया गया है। कहीं-कहीं यह न गुणरूप होता है, न दोषरूप। यह वाक्यदोष है। (7/4)
समासोक्ति:-एक अर्थालङ्कार। जहाँ समान कार्य, लिङ्ग तथा विशेषणों से उपमेय में उपमान के व्यवहार का आरोप किया जाये वहाँ समासोक्ति अलङ्कार होता है-समासोक्तिः समैर्यत्र कार्यलिङ्गविशेषणैः। व्यवहारसमारोपः प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः।। तद्यथा-असमाप्तजिगीषस्य स्त्रीचिन्ता का मनस्विनः। अनाक्रम्य जगत्कृत्स्नं नो सन्ध्यां भजते रविः। इस पद्य में सूर्य और सन्ध्या में नायकनायिका के व्यवहार का आरोप किया गया है।
रूपक में उपमान उपमेय के स्वरूप को आच्छादित कर लेता है जबकि समासोक्ति में उपमेय के स्वरूप को आच्छादित किये विना उसे पूर्व अवस्था से विशिष्ट बना देता है। इसीलिए यहाँ केवलमात्र व्यवहार का समारोप होता है, स्वरूप का नहीं। उपमाध्वनि और श्लेष में विशेष्य भी तुल्य रहता है जबकि समासोक्ति में केवल विशेषण ही तुल्य होते हैं। अप्रस्तुतप्रशंसा में प्रस्तुत व्यङ्ग्य होता है जबकि समासोक्ति में अप्रस्तुत व्यङ्ग्य रहता है। (10/74)