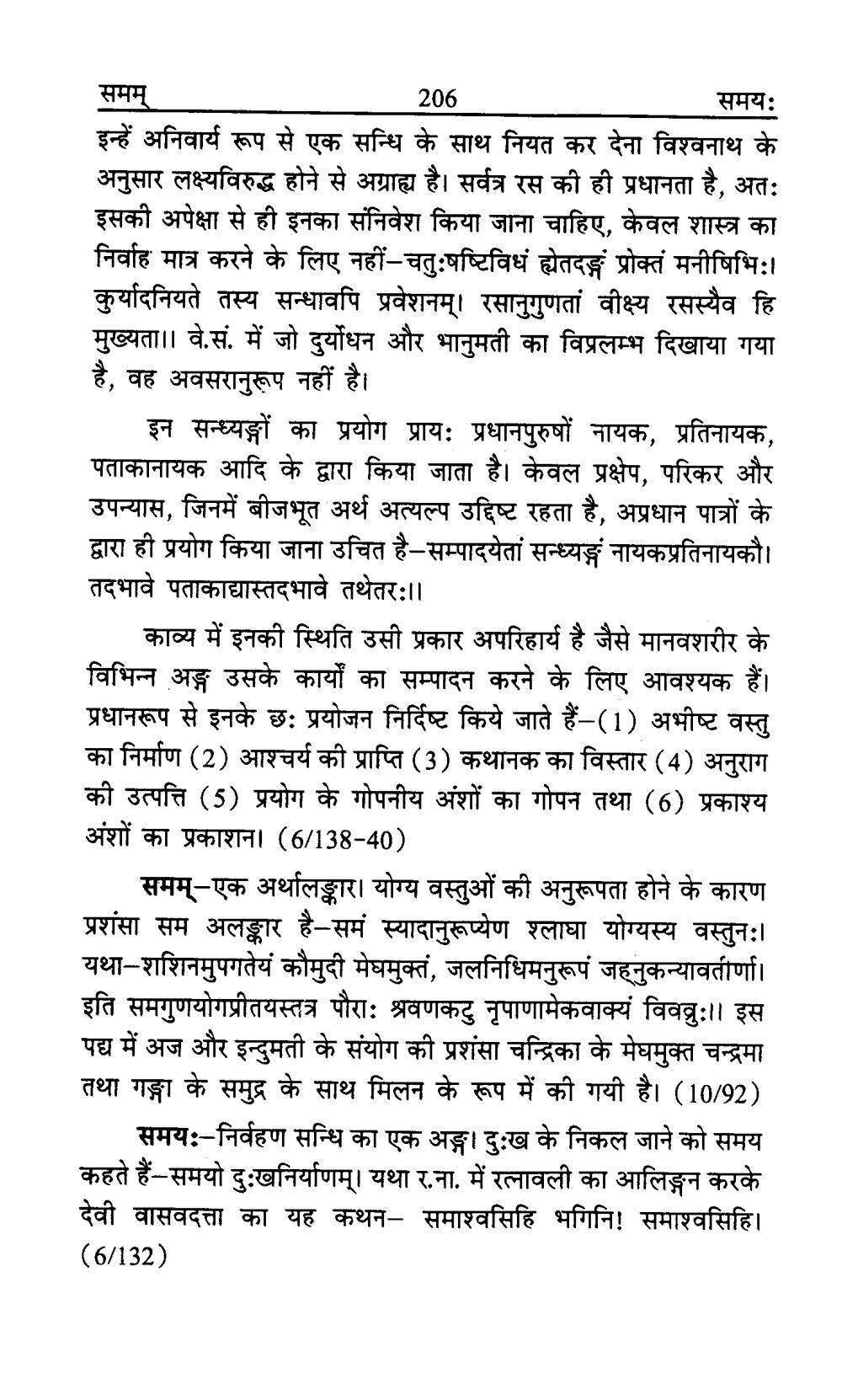________________
206
समम्
समयः इन्हें अनिवार्य रूप से एक सन्धि के साथ नियत कर देना विश्वनाथ के अनुसार लक्ष्यविरुद्ध होने से अग्राह्य है। सर्वत्र रस की ही प्रधानता है, अत: इसकी अपेक्षा से ही इनका संनिवेश किया जाना चाहिए, केवल शास्त्र का निर्वाह मात्र करने के लिए नहीं-चतुःषष्टिविधं ह्येतदङ्ग प्रोक्तं मनीषिभिः। कुर्यादनियते तस्य सन्धावपि प्रवेशनम्। रसानुगुणतां वीक्ष्य रसस्यैव हि मुख्यता।। वे.सं. में जो दुर्योधन और भानुमती का विप्रलम्भ दिखाया गया है, वह अवसरानुरूप नहीं है। ___इन सन्ध्यङ्गों का प्रयोग प्रायः प्रधानपुरुषों नायक, प्रतिनायक, पताकानायक आदि के द्वारा किया जाता है। केवल प्रक्षेप, परिकर और उपन्यास, जिनमें बीजभूत अर्थ अत्यल्प उद्दिष्ट रहता है, अप्रधान पात्रों के द्वारा ही प्रयोग किया जाना उचित है-सम्पादयेतां सन्ध्यङ्ग नायकप्रतिनायकौ। तदभावे पताकाद्यास्तदभावे तथेतरः।।
काव्य में इनकी स्थिति उसी प्रकार अपरिहार्य है जैसे मानवशरीर के विभिन्न अङ्ग उसके कार्यों का सम्पादन करने के लिए आवश्यक हैं। प्रधानरूप से इनके छः प्रयोजन निर्दिष्ट किये जाते हैं-(1) अभीष्ट वस्तु का निर्माण (2) आश्चर्य की प्राप्ति (3) कथानक का विस्तार (4) अनुराग की उत्पत्ति (5) प्रयोग के गोपनीय अंशों का गोपन तथा (6) प्रकाश्य अंशों का प्रकाशन। (6/138-40)
समम्-एक अर्थालङ्कार। योग्य वस्तुओं की अनुरूपता होने के कारण प्रशंसा सम अलङ्कार है-समं स्यादानुरूप्येण श्लाघा योग्यस्य वस्तुनः। यथा-शशिनमुपगतेयं कौमुदी मेघमुक्तं, जलनिधिमनुरूपं जहनुकन्यावतीर्णा। इति समगुणयोगप्रीतयस्तत्र पौराः श्रवणकटु नृपाणामेकवाक्यं विवग्रैः।। इस पद्य में अज और इन्दुमती के संयोग की प्रशंसा चन्द्रिका के मेघमुक्त चन्द्रमा तथा गङ्गा के समुद्र के साथ मिलन के रूप में की गयी है। (10/92)
समयः-निर्वहण सन्धि का एक अङ्ग। दु:ख के निकल जाने को समय कहते हैं-समयो दुःखनिर्याणम्। यथा र.ना. में रत्नावली का आलिङ्गन करके देवी वासवदत्ता का यह कथन- समाश्वसिहि भगिनि! समाश्वसिहि। (6/132)