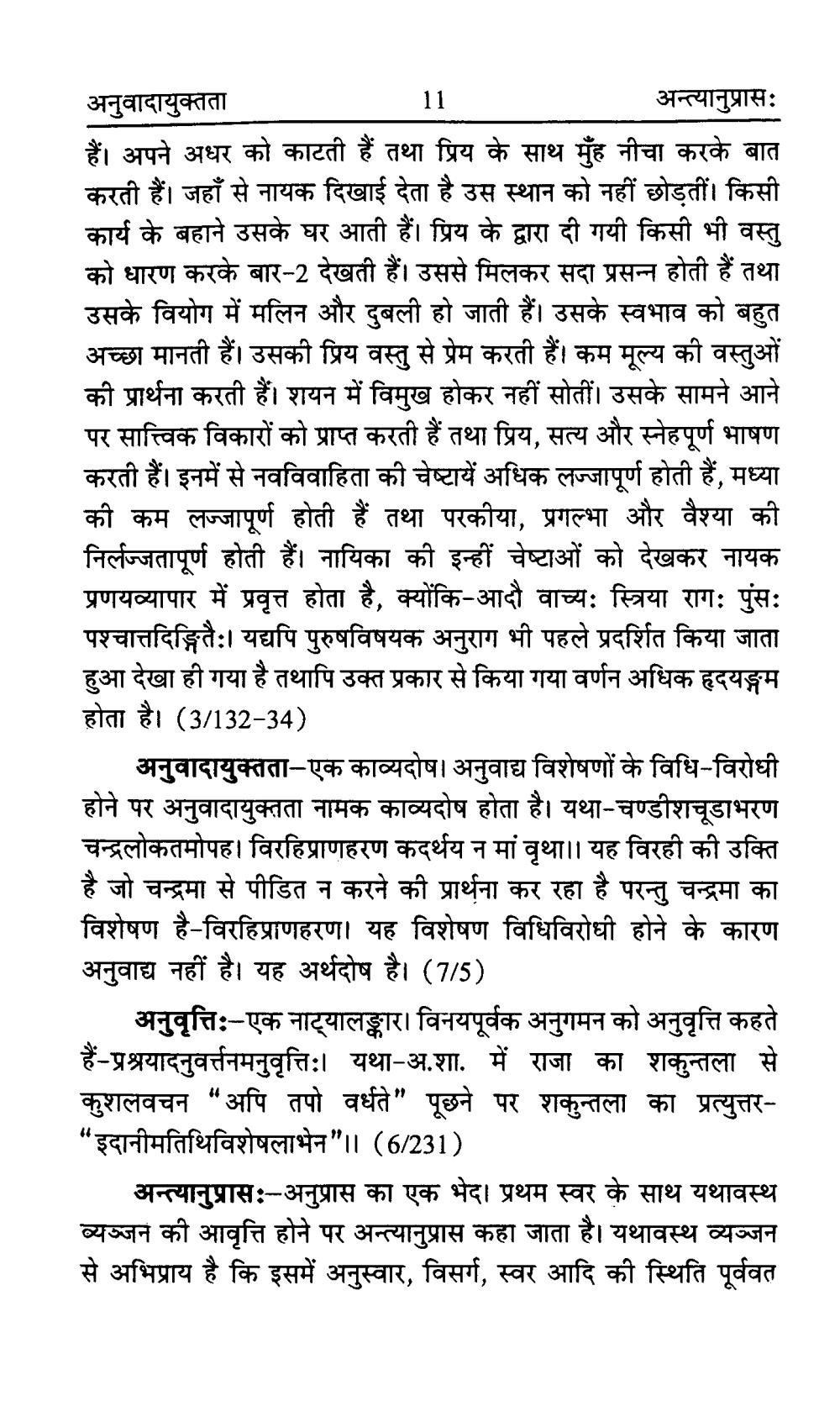________________
अनुवादायुक्तता
11
अन्त्यानुप्रासः
हैं। अपने अधर को काटती हैं तथा प्रिय के साथ मुँह नीचा करके बात करती हैं। जहाँ से नायक दिखाई देता है उस स्थान को नहीं छोड़तीं। किसी कार्य के बहाने उसके घर आती हैं। प्रिय के द्वारा दी गयी किसी भी वस्तु को धारण करके बार -2 देखती हैं। उससे मिलकर सदा प्रसन्न होती हैं तथा उसके वियोग में मलिन और दुबली हो जाती हैं। उसके स्वभाव को बहुत अच्छा मानती हैं। उसकी प्रिय वस्तु से प्रेम करती हैं। कम मूल्य की वस्तुओं की प्रार्थना करती हैं। शयन में विमुख होकर नहीं सोतीं। उसके सामने आने पर सात्त्विक विकारों को प्राप्त करती हैं तथा प्रिय, सत्य और स्नेहपूर्ण भाषण करती हैं। इनमें से नवविवाहिता की चेष्टायें अधिक लज्जापूर्ण होती हैं, मध्या की कम लज्जापूर्ण होती हैं तथा परकीया, प्रगल्भा और वैश्या की निर्लज्जतापूर्ण होती हैं। नायिका की इन्हीं चेष्टाओं को देखकर नायक प्रणयव्यापार में प्रवृत्त होता है, क्योंकि - आदौ वाच्यः स्त्रिया रागः पुंसः पश्चात्तदिङ्गितैः । यद्यपि पुरुषविषयक अनुराग भी पहले प्रदर्शित किया जाता हुआ देखा ही गया है तथापि उक्त प्रकार से किया गया वर्णन अधिक हृदयङ्गम होता है। (3/132-34 )
अनुवादायुक्तता - एक काव्यदोष । अनुवाद्य विशेषणों के विधि-विरोधी होने पर अनुवादायुक्तता नामक काव्यदोष होता है । यथा चण्डीशचूडाभरण चन्द्रलोकतमोपह। विरहिप्राणहरण कदर्थय न मां वृथा । । यह विरही की उक्ति है जो चन्द्रमा से पीडित न करने की प्रार्थना कर रहा है परन्तु चन्द्रमा का विशेषण है - विरहिप्राणहरण । यह विशेषण विधिविरोधी होने के कारण अनुवाद्य नहीं है। यह अर्थदोष है । ( 7/5)
अनुवृत्तिः - एक नाट्यालङ्कार । विनयपूर्वक अनुगमन को अनुवृत्ति कहते हैं - प्रश्रयादनुवर्त्तनमनुवृत्तिः । यथा - अ.शा. में राजा का शकुन्तला से कुशलवचन " अपि तपो वर्धते" पूछने पर शकुन्तला का प्रत्युत्तर" इदानीमतिथिविशेषलाभेन " ।। (6/231)
अन्त्यानुप्रासः - अनुप्रास का एक भेद । प्रथम स्वर के साथ यथावस्थ व्यञ्जन की आवृत्ति होने पर अन्त्यानुप्रास कहा जाता है। यथावस्थ व्यञ्जन से अभिप्राय है कि इसमें अनुस्वार, विसर्ग, स्वर आदि की स्थिति पूर्ववत