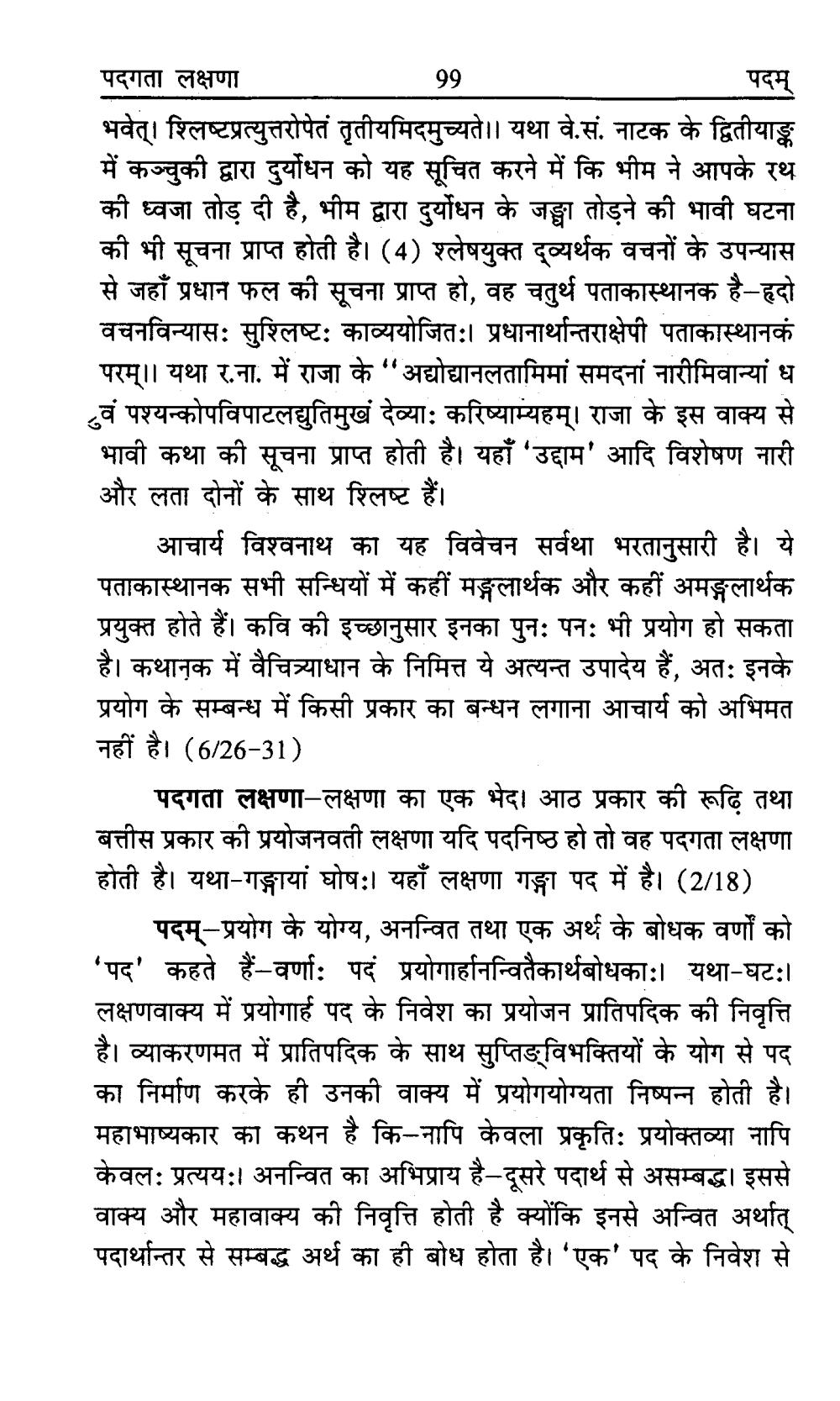________________
पदगता लक्षणा
99
पदम्
भवेत्। श्लिष्टप्रत्युत्तरोपेतं तृतीयमिदमुच्यते । । यथा वे.सं. नाटक के द्वितीयाङ्क में कञ्चुकी द्वारा दुर्योधन को यह सूचित करने में कि भीम ने आपके रथ की ध्वजा तोड़ दी है, भीम द्वारा दुर्योधन के जङ्घा तोड़ने की भावी घटना की भी सूचना प्राप्त होती है। (4) श्लेषयुक्त द्व्यर्थक वचनों के उपन्यास से जहाँ प्रधान फल की सूचना प्राप्त हो, वह चतुर्थ पताकास्थानक है - हृदो वचनविन्यासः सुश्लिष्टः काव्ययोजितः । प्रधानार्थान्तराक्षेपी पताकास्थानकं परम्।। यथा र.ना. में राजा के " अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां ध वं पश्यन्कोपविपाटलद्युतिमुखं देव्याः करिष्याम्यहम् । राजा के इस वाक्य से भावी कथा की सूचना प्राप्त होती है। यहाँ 'उद्दाम' आदि विशेषण नारी और लता दोनों के साथ श्लिष्ट हैं।
आचार्य विश्वनाथ का यह विवेचन सर्वथा भरतानुसारी है। ये पताकास्थानक सभी सन्धियों में कहीं मङ्गलार्थक और कहीं अमङ्गलार्थक प्रयुक्त होते हैं । कवि की इच्छानुसार इनका पुनः पनः भी प्रयोग हो सकता है । कथानक में वैचित्र्याधान के निमित्त ये अत्यन्त उपादेय हैं, अतः इनके प्रयोग के सम्बन्ध में किसी प्रकार का बन्धन लगाना आचार्य को अभिमत नहीं है। (6/26-31)
पदगता लक्षणा-लक्षणा का एक भेद । आठ प्रकार की रूढ़ि तथा बत्तीस प्रकार की प्रयोजनवती लक्षणा यदि पदनिष्ठ हो तो वह पदगता लक्षणा होती है। यथा- गङ्गायां घोष: । यहाँ लक्षणा गङ्गा पद में है। (2/18)
पदम् - प्रयोग के योग्य, अनन्वित तथा एक अर्थ के बोधक वर्णों को 'पद' कहते हैं - वर्णाः पदं प्रयोगार्हानन्वितैकार्थबोधकाः । यथा - घटः । लक्षणवाक्य में प्रयोगार्ह पद के निवेश का प्रयोजन प्रातिपदिक की निवृत्ति है | व्याकरणमत में प्रातिपदिक के साथ सुप्तिविभक्तियों के योग से पद का निर्माण करके ही उनकी वाक्य में प्रयोगयोग्यता निष्पन्न होती है। महाभाष्यकार का कथन है कि - नापि केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः। अनन्वित का अभिप्राय है- दूसरे पदार्थ से असम्बद्ध। इससे वाक्य और महावाक्य की निवृत्ति होती है क्योंकि इनसे अन्वित अर्थात् पदार्थान्तर से सम्बद्ध अर्थ का ही बोध होता है। 'एक' पद के निवेश से