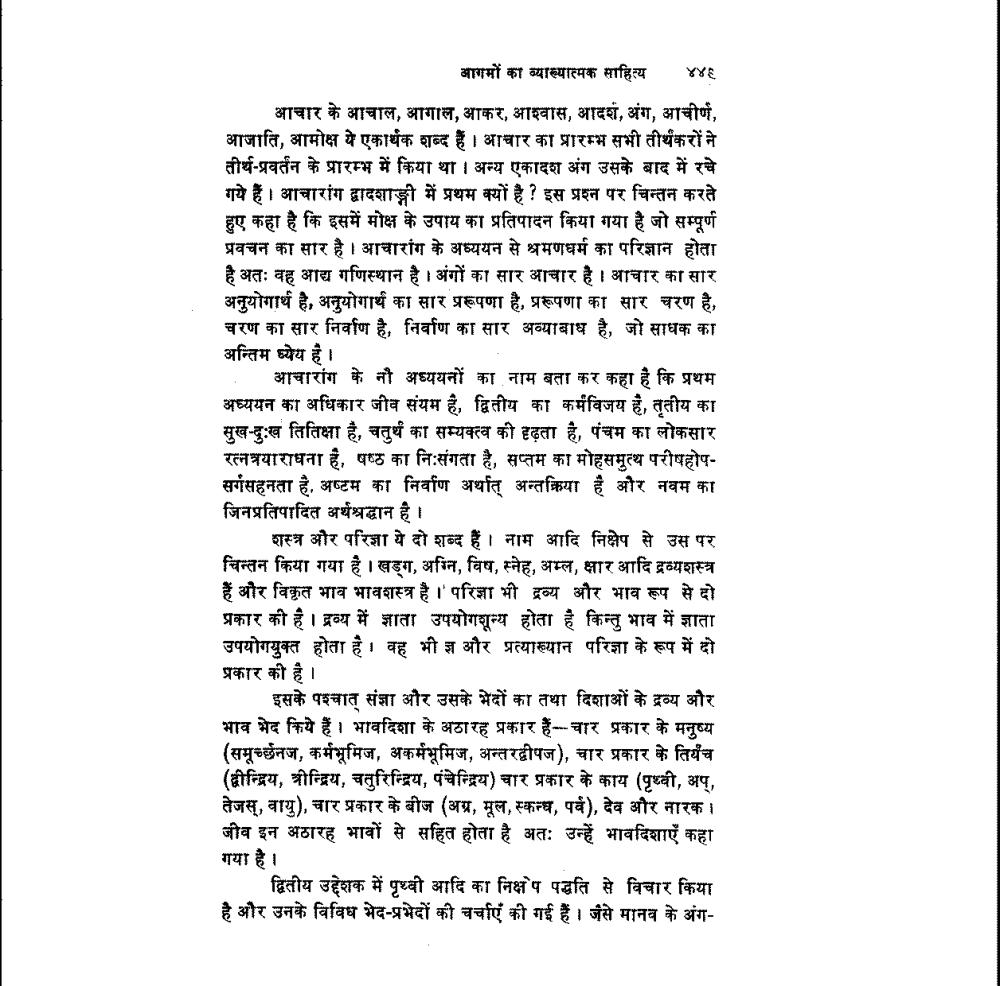________________
आगमों का व्याख्यात्मक साहित्य ४४६ आचार के आचाल, आगाल, आकर, आश्वास, आदर्श, अंग, आचीर्ण, आजाति, आमोक्ष ये एकार्थक शब्द हैं । आचार का प्रारम्भ सभी तीर्थंकरों ने तीर्थ-प्रवर्तन के प्रारम्भ में किया था । अन्य एकादश अंग उसके बाद में रचे गये हैं। आचारांग द्वादशाङ्गी में प्रथम क्यों है ? इस प्रश्न पर चिन्तन करते हए कहा है कि इसमें मोक्ष के उपाय का प्रतिपादन किया गया है जो सम्पूर्ण प्रवचन का सार है। आचारांग के अध्ययन से श्रमणधर्म का परिज्ञान होता है अतः वह आद्य गणिस्थान है। अंगों का सार आचार है । आचार का सार अनुयोगार्थ है, अनुयोगार्थ का सार प्ररूपणा है, प्ररूपणा का सार चरण है, चरण का सार निर्वाण है, निर्वाण का सार अव्याबाध है, जो साधक का अन्तिम ध्येय है।
आचारांग के नौ अध्ययनों का नाम बता कर कहा है कि प्रथम अध्ययन का अधिकार जीव संयम है, द्वितीय का कर्मविजय है, ततीय का सुख-दुःख तितिक्षा है, चतुर्थ का सम्यक्त्व की दृढ़ता है, पंचम का लोकसार रत्नत्रयाराधना है, षष्ठ का निःसंगता है, सप्तम का मोहसमुत्थ परीषहोपसर्गसहनता है, अष्टम का निर्वाण अर्थात् अन्तक्रिया है और नवम का जिनप्रतिपादित अर्थश्रद्धान है।
शस्त्र और परिज्ञा ये दो शब्द हैं। नाम आदि निक्षेप से उस पर चिन्तन किया गया है । खड्ग, अग्नि, विष, स्नेह, अम्ल, क्षार आदि द्रव्यशस्त्र हैं और विकृत भाव भावशस्त्र है। परिज्ञा भी द्रव्य और भाव रूप से दो प्रकार की है । द्रव्य में ज्ञाता उपयोगशून्य होता है किन्तु भाव में ज्ञाता उपयोगयुक्त होता है। वह भी ज्ञ और प्रत्याख्यान परिज्ञा के रूप में दो प्रकार की है।
इसके पश्चात् संज्ञा और उसके भेदों का तथा दिशाओं के द्रव्य और भाव भेद किये हैं। भावदिशा के अठारह प्रकार हैं-चार प्रकार के मनुष्य (समर्छनज, कर्मभूमिज, अकर्मभूमिज, अन्तरद्वीपज), चार प्रकार के तिर्यंच (द्वीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय) चार प्रकार के काय (पृथ्वी, अप, तेजस्, वायु), चार प्रकार के बीज (अग्र, मूल, स्कन्ध, पर्व), देव और नारक । जीव इन अठारह भावों से सहित होता है अतः उन्हें भावदिशाएँ कहा गया है।
द्वितीय उद्देशक में पृथ्वी आदि का निक्षेप पद्धति से विचार किया है और उनके विविध भेद-प्रभेदों की चर्चाएं की गई हैं। जैसे मानव के अंग