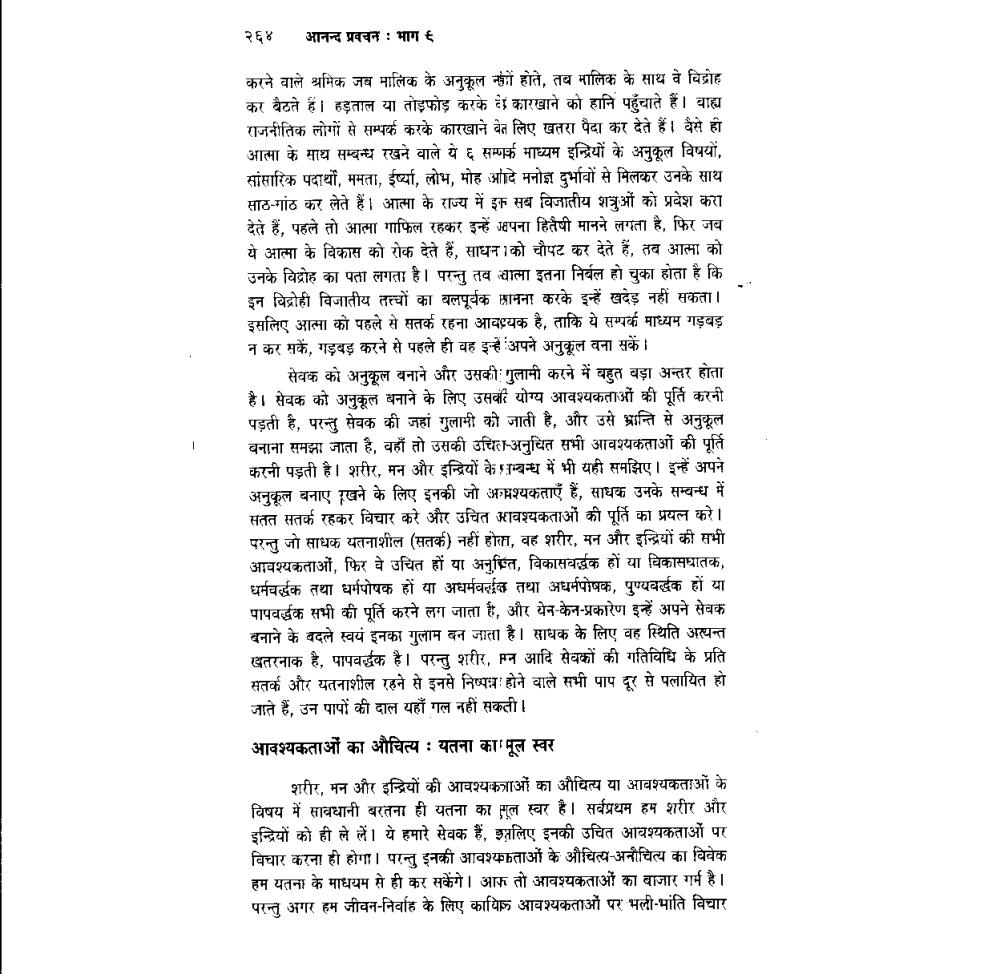________________
२६४
आनन्द प्रवचन : भाग ६
करने वाले श्रमिक जब मालिक के अनुकूल नकों होते, तब मालिक के साथ वे विद्रोह कर बैठते हैं। हड़ताल या तोड़फोड़ करके कारखाने को हानि पहुंचाते हैं। बाह्य राजनीतिक लोगों से सम्पर्क करके कारखाने बेत लिए खतरा पैदा कर देते हैं। वैसे ही आत्मा के साथ सम्बन्ध रखने वाले ये ६ सम्पर्क माध्यम इन्द्रियों के अनुकूल विषयों, सांसारिक पदार्थो, ममता, ईर्ष्या, लोभ, मोह आदे मनोज्ञ दुर्भावों से मिलकर उनके साथ साठ-गांठ कर लेते हैं। आत्मा के राज्य में इस सब विजातीय शत्रओं को प्रवेश करा देते हैं, पहले तो आमा गाफिल रहकर इन्हें अपना हितैषी मानने लगता है, फिर जब ये आत्मा के विकास को रोक देते हैं, साधनाको चौपट कर देते हैं. तब आत्मा को उनके विद्रोह का पता लगता है। परन्तु तव चात्मा इतना निर्बल हो चुका होता है कि इन विद्रोही विजातीय तत्त्वों का बलपूर्वक सामना करके इन्हें खदेड़ नहीं सकता। इसलिए आत्मा को पहले से सतर्क रहना आवश्यक है. ताकि ये सम्पर्क माध्यम गडबड न कर सकें, गड़बड़ करने से पहले ही वह इन्हें अपने अनकल बना सकें।
सेवक को अनुकूल बनाने और उसकी गुलामी करने में बहुत बड़ा अन्तर होता है। सेवक को अनुकूल बनाने के लिए उसकी योग्य आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है, परन्तु सेवक की जहां गुलामी को जाती है, और उसे भ्रान्ति से अनुकूल बनाना समझा जाता है, वहाँ तो उसकी उचित-अनुचित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। शरीर, मन और इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी यही समझिए। इन्हें अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए इनकी जो अघश्यकताएँ हैं, साधक उनके सम्बन्ध में सतत सतर्क रहकर विचार करे और उचित आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयल करे । परन्तु जो साधक यतनाशील (सतर्क) नहीं होता, वह शरीर, मन और इन्द्रियों की सभी आवश्यकताओं, फिर वे उचित हों या अनुस्ति, विकासबर्द्धक हों या विकासघातक, धर्मवर्द्धक तथा धर्मपोषक हों या अधर्मवर्द्धन तथा अधर्मपोषक, पुण्यवर्द्धक हों या पापवर्द्धक सभी की पूर्ति करने लग जाता है, और येन केन-प्रकारेण इन्हें अपने सेवक बनाने के बदले स्वयं इनका गुलाम बन जाता है। साधक के लिए वह स्थिति अत्यन्त खतरनाक है, पापवर्द्धक है। परन्तु शरीर, मन आदि सेवकों की गतिविधि के प्रति सतर्क और यतनाशील रहने से इनसे निष्पन्न होने वाले सभी पाप दूर से पलायित हो जाते हैं, उन पापों की दाल यहाँ गल नहीं सकती।
आवश्यकताओं का औचित्य : यतना का मूल स्वर
शरीर, मन और इन्द्रियों की आवश्यकताओं का औचित्य या आवश्यकताओं के विषय में सावधानी बरतना ही यतना का मूल स्वर है। सर्वप्रथम हम शरीर और इन्द्रियों को ही ले लें। ये हमारे सेवक हैं, इसलिए इनकी उचित आवश्यकताओं पर विचार करना ही होगा। परन्तु इनकी आवश्यकताओं के औचित्य-अनौचित्य का विवेक हम यतना के माधयम से ही कर सकेंगे। आफ तो आवश्यकताओं का बाजार गर्म है। परन्तु अगर हम जीवन-निर्वाह के लिए कायिक आवश्यकताओं पर भली-भांति विचार