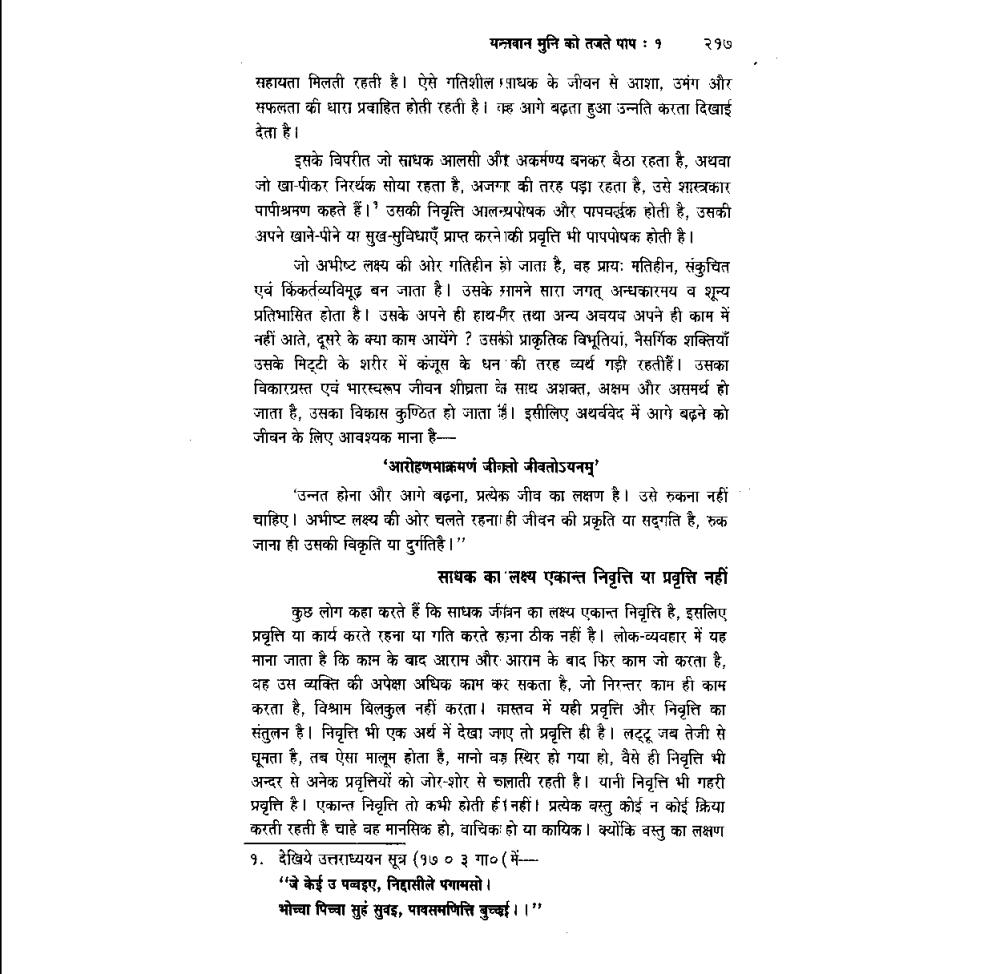________________
यानवान मुनि को तजते पाप : १
२१७
सहायता मिलती रहती है। ऐसे गतिशीलपाधक के जीवन से आशा, उमंग और सफलता की धारा प्रवाहित होती रहती है। यह आगे बढ़ता हुआ उन्नति करता दिखाई देता है।
इसके विपरीत जो साधक आलसी और अकर्मण्य बनकर बैठा रहता है, अथवा जो खा-पीकर निरर्थक सोया रहता है, अजगा की तरह पड़ा रहता है, उसे शास्त्रकार पापीश्रमण कहते हैं।' उसकी निवृत्ति आलन्थपोषक और पापवर्द्धक होती है, उसकी अपने खाने-पीने या सुख-सुविधाएँ प्राप्त करने की प्रवृत्ति भी पापपोषक होती है।
जो अभीष्ट लक्ष्य की ओर गतिहीन हो जाता है, वह प्रायः मतिहीन, संकुचित एवं किंकर्तव्यविमूढ़ बन जाता है। उसके मामने सारा जगत् अन्धकारमय व शून्य प्रतिभासित होता है। उसके अपने ही हाथ-गैर तथा अन्य अवयव अपने ही काम में नहीं आते, दूसरे के क्या काम आयेंगे ? उसको प्राकृतिक विभूतियां, नैसर्गिक शक्तियाँ उसके मिट्टी के शरीर में कंजूस के धन की तरह व्यर्थ गड़ी रहतीहैं। उसका विकारग्रस्त एवं भारस्वरूप जीवन शीघ्रता न साथ अशक्त, अक्षम और असमर्थ हो जाता है, उसका विकास कुण्ठित हो जाता है। इसीलिए अथर्ववेद में आगे बढ़ने को जीवन के लिए आवश्यक माना है--
___'आरोहणमाक्रमणं जीक्लो जीवतोऽयनम्' 'उन्नत होना और आगे बढ़ना, प्रत्येक जीव का लक्षण है। उसे रुकना नहीं । चाहिए। अभीष्ट लक्ष्य की ओर चलते रहना ही जीवन की प्रकृति या सद्गति है, रुक जाना ही उसकी विकृति या दुर्गतिहै।"
साधक का लक्ष्य एकान्त निवृत्ति या प्रवृत्ति नहीं कुछ लोग कहा करते हैं कि साधक जीवन का लक्ष्य एकान्त निवृत्ति है, इसलिए प्रवृत्ति या कार्य करते रहना या गति करते साना ठीक नहीं है। लोक-व्यवहार में यह माना जाता है कि काम के बाद आराम और आराम के बाद फिर काम जो करता है, वह उस व्यक्ति की अपेक्षा अधिक काम कर सकता है, जो निरन्तर काम ही काम करता है, विश्राम बिलकुल नहीं करता। सस्तव में यही प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन है। निवृत्ति भी एक अर्थ में देखा जाए तो प्रवृत्ति ही है। लटू जब तेजी से घूमता है, तब ऐसा मालूम होता है, मानो वा स्थिर हो गया हो, वैसे ही निवृत्ति भी अन्दर से अनेक प्रवृत्तियों को जोर-शोर से कालाती रहती है। यानी निवृत्ति भी गहरी प्रवृत्ति है। एकान्त निवृत्ति तो कभी होती ही नहीं। प्रत्येक वस्तु कोई न कोई क्रिया करती रहती है चाहे वह मानसिक हो, वाचिका हो या कायिक । क्योंकि वस्तु का लक्षण १. देखिये उत्तराध्ययन सूत्र (१७०३ गा० ( में----
"जे केई उ पवइए, निदासीले पगामसो। भोच्चा पिच्चा सुहं सुवइ, पावसमणित्ति बुचा।।"