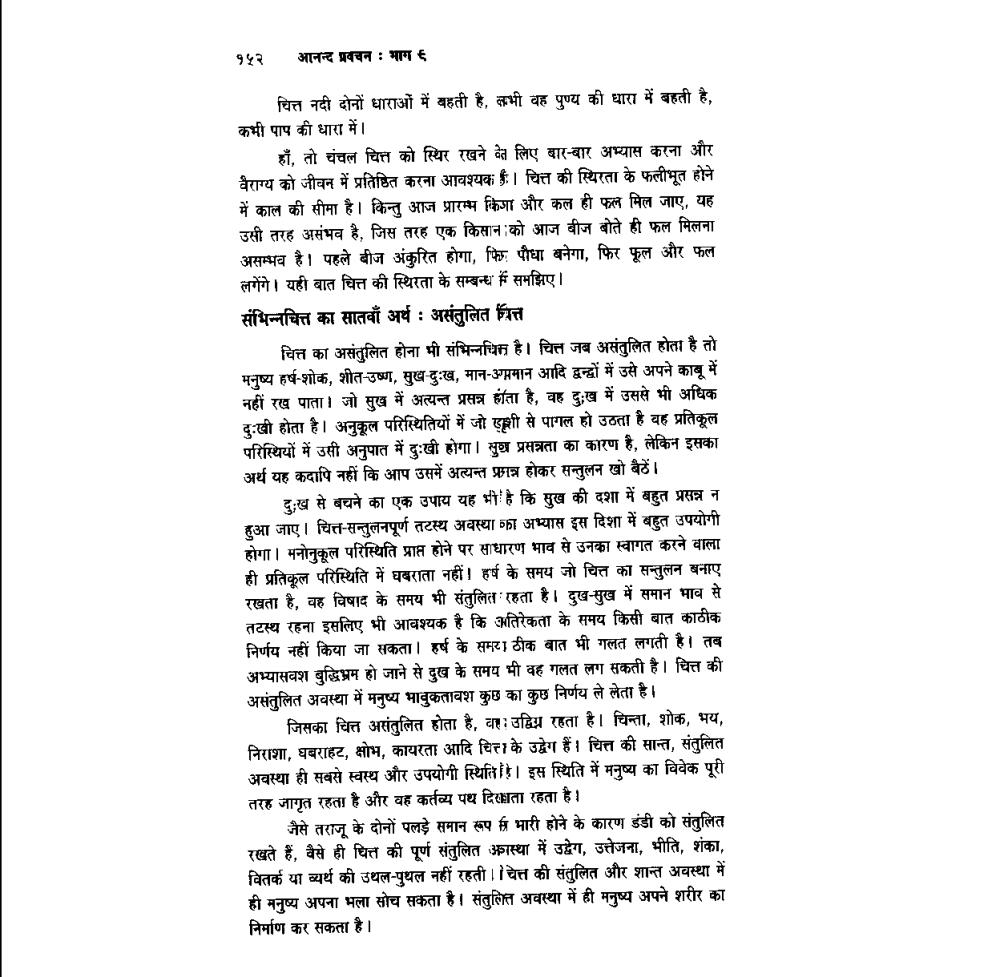________________
१५२
आनन्द प्रवचन : भाग ६
चित्त नदी दोनों धाराओं में बहती है, कभी वह पुण्य की धारा में बहती है, कभी पाप की धारा में।
हाँ, तो चंचल चित्त को स्थिर रखने वेत लिए बार-बार अभ्यास करना और वैराग्य को जीवन में प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। चित्त की स्थिरता के फलीभूत होने में काल की सीमा है। किन्तु आज प्रारम्भ किया और कल ही फल मिल जाए, यह उसी तरह असंभव है, जिस तरह एक किसान को आज बीज बोते ही फल मिलना असम्भव है। पहले बीज अंकुरित होगा, फि पौधा बनेगा, फिर फूल और फल लगेंगे। यही बात चित्त की स्थिरता के सम्बन्ध में समझिए। संभिन्नचित्त का सातवाँ अर्थ : असंतुलित वित्त
चित्त का असंतुलित होना भी संभिन्नधिक है। चित्त जब असंतुलित होता है तो मनुष्य हर्ष-शोक, शीत-उष्ण, सुख दुःख, मान-अपमान आदि द्वन्द्वों में उसे अपने काबू में नहीं रख पाता। जो सुख में अत्यन्त प्रसन्न होता है, वह दुःख में उससे भी अधिक दुःखी होता है। अनुकूल परिस्थितियों में जो खुशी से पागल हो उठता है वह प्रतिकूल परिस्थियों में उसी अनुपात में दुःखी होगा। सुश प्रसन्नता का कारण है, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि आप उसमें अत्यन्त फ्रान्न होकर सन्तुलन खो बैठें।
दु:ख से बचने का एक उपाय यह भी है कि सुख की दशा में बहुत प्रसन्न न हुआ जाए । चित्त-सन्तुलनपूर्ण तटस्थ अवस्था का अभ्यास इस दिशा में बहुत उपयोगी होगा। मनोनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर साधारण भाव से उनका स्वागत करने वाला ही प्रतिकूल परिस्थिति में घबराता नहीं। हर्ष के समय जो चित्त का सन्तुलन बनाए रखता है, वह विषाद के समय भी संतुलित रहता है। दुख-सुख में समान भाव से तटस्थ रहना इसलिए भी आवश्यक है कि अतिरेकता के समय किसी बात काठीक निर्णय नहीं किया जा सकता। हर्ष के समरा ठीक बात भी गलत लगती है। तब अभ्यासवश बुद्धिभ्रम हो जाने से दुख के समय भी वह गलत लग सकती है। चित्त की असंतुलित अवस्था में मनुष्य भावुकतावश कुछ का कुछ निर्णय ले लेता है।
जिसका चित्त असंतुलित होता है, वह उद्विग्न रहता है। चिन्ता, शोक, भय, निराशा, घबराहट, क्षोभ, कायरता आदि चित्त के उद्वेग हैं। चित्त की सान्त, संतुलित अवस्था ही सबसे स्वस्थ और उपयोगी स्थिति है। इस स्थिति में मनुष्य का विवेक पूरी तरह जागृत रहता है और वह कर्तव्य पथ दिखाता रहता है।
जैसे तराजू के दोनों पलड़े समान रूप में भारी होने के कारण डंडी को संतुलित रखते हैं, वैसे ही चित्त की पूर्ण संतुलित अास्था में उद्वेग, उत्तेजना, भीति, शंका, वितर्क या व्यर्थ की उथल-पुथल नहीं रहती। चित्त की संतुलित और शान्त अवस्था में ही मनुष्य अपना भला सोच सकता है। संतुलित अवस्था में ही मनुष्य अपने शरीर का निर्माण कर सकता है।