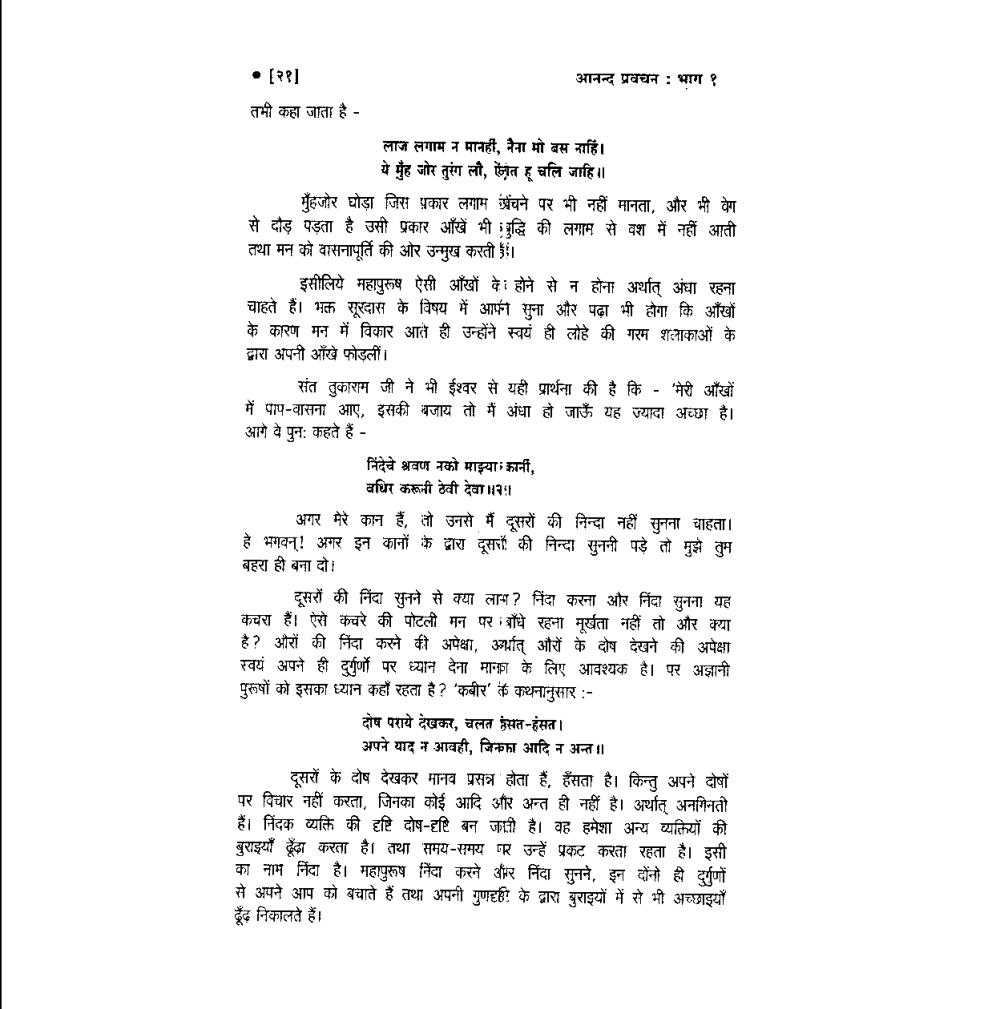________________
• [२१]
तभी कहा जाता है।
-
लाज लगाम न मानही, नैना मो बस नाहिं। ये मुँह जोर तुरंग लौ, ऐनत हू चलि जाहि ॥
आनन्द प्रवचन भाग १
मुँहजोर घोड़ा जिस प्रकार लगाम अँचने पर भी नहीं से दौड़ पड़ता है उसी प्रकार आँखें भी बुद्धि की लगाम से तथा मन को वासनापूर्ति की ओर उन्मुख करती हैं।
संत तुकाराम जी ने भी ईश्वर से में पाप वासना आए, इसकी आगे वे पुन: कहते हैं
इसीलिये महापुरूष ऐसी आँखों के होने से न होना अर्थात् अंधा रहना चाहते हैं। भक्त सूरदास के विषय में आफी सुना और पढ़ा भी होगा कि आँखों के कारण मन में विकार आते ही उन्होंने स्वयं ही लोहे की गरम शलाकाओं के द्वारा अपनी आँखे फोडलीं ।
यही प्रार्थना की है कि 'मेरी आँखों बजाय तो मैं अंधा हो जाऊँ यह ज्यादा अच्छा है।
निंदेचे श्रवण नको माझ्या कानी, बधिर करूनी ठेवी देवा ॥२॥
मानता, और भी वेग वश में नहीं आती
अगर मेरे कान तो उनसे मैं दूसरों की निन्दा नहीं सुनना चाहता । हे भगवन्! अगर इन कानों के द्वारा दूसरों की निन्दा सुननी पड़े तो मुझे तुम बहरा ही बना दो।
दूसरों की निंदा सुनने से क्या लाग ? निंदा करना और निंदा सुनना यह कचरा हैं। ऐसे कचरे की पोटली मन पर बाँधे रहना मूर्खता नहीं तो और क्या है ? औरों की निंदा करने की अपेक्षा, अर्थात् औरों के दोष देखने की अपेक्षा स्वयं अपने ही दुर्गुणों पर ध्यान देना मानकता के लिए आवश्यक है। पर अज्ञानी पुरुषों को इसका ध्यान कहाँ रहता है ? 'कबीर' के कथनानुसार :
दोष पराये देखकर चलत सत हंसत । अपने याद न आवही, जिनका आदि न अन्त।
दूसरों के दोष देखकर मानव प्रसन्न होता हैं, हँसता है।
किन्तु अपने दोषों पर विचार नहीं करता, जिनका कोई आदि और अन्त ही नहीं है। अर्थात् अनगिनती हैं। निंदक व्यक्ति की दृष्टि दोष दृष्टि बन जाती है। वह हमेशा अन्य व्यक्तियों की बुराइयाँ ढूँढ़ा करता है। तथा समय-समय पर उन्हें प्रकट करता रहता है। इसी का नाम निंदा है। महापुरूष निंदा करने और निंदा सुनने इन दोनो ही दुर्गुणों से अपने आप को बचाते हैं तथा अपनी गुणही के द्वारा बुराइयों में से भी अच्छाइयाँ ढूँढ़ निकालते हैं।